सार्थक संवाद ब्लॉग पर 16 अक्टूबर को एक लेख छपा। सुशोभित जी द्वारा लिखे इस लेख का शीर्षक है “श्रम के मूल्यांकन में विवेक की भूमिका”। यह लेख मैंने जब पढ़ा, तो मुझे यह ठीक नहीं लगा। मित्र आशुतोष जी के कहने पर मैंने अपनी आपत्ति को कमेंट्स सेक्शन में दर्ज़ कराया। बाद में उनका आग्रह था, कि केवल कमेंट्स से बात नहीं बनेगी, बल्कि मुझे अपने विचार एक व्यापक लेख के रूप में रखने चाहिए। मेरा यह लेख इसी संदर्भ में लिखा जा रहा है।
१.
इस लेख में एक मौलिक प्रश्न उठाया गया है- किसी भी श्रम का मूल्यांकन कैसे हो? इसके क्या आधार हों? उनकी यह चिंता आज के समाज की स्थिति को देख कर बन रही है। आज एक ऐसा वर्ग है, जो न के बराबर श्रम करता है लेकिन कई गुना वेतन पाता है। इस वर्ग को उक्त लेख में बुद्धिजीवी वर्ग कहा गया है तथा ‘बुद्धिजीवी’ एक ख़राब शब्द की तरह प्रस्तुत किया गया है। बुद्धिजीवियों के लिए निकम्मा, निठल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है और बुद्धिजीवियों की समस्त भागीदारी की समीक्षा “समाज में क्लेश बढ़ाना” कह कर की गई है।
इस वर्ग के विपरीत समाज में एक दूसरा वर्ग है – जैसे किसान, मज़दूर, कारीगर इत्यादि जो अत्यंत श्रम के बावजूद भी दीन – हीन स्थिति में जीने को मजबूर है। समाज में इस वर्ग का योगदान न केवल उपयोगी है, बल्कि अनिवार्य भी है – अगर किसान अन्न पैदा करना बंद कर दे, तो समाज खाएगा क्या?
उक्त लेख में एक से अधिक बार यह सवाल उठाया गया है कि बुद्धिजीवियों ने समाज / देश को ऐसा क्या दिया है, कि उनका ‘मेहनताना’ बाकी समाज के मुक़ाबले कई गुना है। न्यूनतम मज़दूरी श्रमिक वर्ग के लिए ही क्यों है – यह प्रश्न – जिसका सीधा सीधा असर है, कि श्रमिक न्यूनतम रेखा के आस-पास ही जीता है, एक वाजिब प्रश्न है। इसके विपरीत, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसका वेतन तो आसमान छूता है।
समाज में इस प्रकार की ग़ैर बराबरी ठीक नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता और स्थिरता के लिए ख़तरनाक है। इस बात को कहने के लिए उक्त लेख में जी ने महात्मा गांधी का सहारा लिया गया है जहॉं पर गांधी जी की बातों को और उनके जीवन को कई बार उद्धृत किया गया हैं।
२.
मेरे विचार से उपर्युक्त लेखक को अपनी यह बात कहने के लिए महात्मा गांधी को याद करने की आवश्यकता नहीं थी। यह ज़रूरी नहीं, कि हम अपनी बात कहने के लिए गांधी जी को परलोक से यहाँ बुलाएँ। ऐसी ज़बरदस्ती से हमें बचना चाहिए। वे अगर गांधी की बजाए मार्क्स को बुलाते, तो शायद ज़्यादा उचित होता।
मेरे जैसे व्यक्ति के लिये महात्मा गांधी उन गिने चुने लोगों में हैं, जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता का मूलयांकन भारतीय दृष्टि के धरातल पर खड़े हो कर किया है। ऐसा करना तब साहस की बात थी (और आज भी है)। उनकी किताब हिंद स्वराज (जिसको उक्त लेखक ने अपने लेख में उद्धृत किया है) शायद पश्चिम की समीक्षा करने का पहला प्रयास है। और उस किताब के 100 वर्ष बाद भी पश्चिम की समीक्षा के कुछ गिने चुने उदाहरण ही मिलते हैं। इस लिए मेरे जैसा व्यक्ति जब महात्मा गांधी के नाम को किसी लेख में देखता है, तो एक अपेक्षा रहती है, कि भारतीय दृष्टि के धरातल पर खड़े होने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी अपेक्षा होना सहज ही है। ऐसी अपेक्षा होना वाजिब है।
इसके विपरीत उल्लिखित लेख को पढ़कर मुझे लगा, कि वह पश्चिम की दृष्टि से लिखा गया लेख है और इस दृष्टि को लेखक जाने – अनजाने महात्मा गांधी पर आरोपित कर रहे हैं। उक्त लेख महात्मा गांधी पर तो नहीं है किन्तु लेख तो वर्तमान समाज में आर्थिक ग़ैर बराबरी पर है। बिना गांधी जी को बुलाए यह बात की जा सकती थी। लेख की मूल चिंता पर उससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता।
महात्मा गांधी भारत के समाज को समझते थे। और वे यूरोप को भी समझते थे। और इन दो सभ्यताओं में वे ठीक से भेद कर पाते थे। गांधी के लिए बड़ी समस्या थी “भारत का धर्म – भ्रष्ट हो जाना”1। और उनका समूचा प्रयास ‘धर्म – स्थापना’ के अर्थ में ही था। धर्म की स्थापना कैसे हो, इसके लिए क्या किया जाए, यह चिंता सदैव ही हमारा समाज करता आया है। मेरे विचार से पॉलिटिक्स का मूल प्रश्न यह ही है। महाभारत में विदुर जिन्हें नीति का विद्वान माना गया है – सदैव धर्म की रक्षा के संदर्भ में ही सुझाव देते हैं। हमारे इतिहास में धर्म – स्थापना के लिए विष्णु जी अवतरित होते रहते हैं – कभी राम बन कर, कभी कृष्ण के रूप में इत्यादि। धरमपाल जी ने एक सभा में हल्के से कहा था कि वे गांधी तो अवतार मानते थे।2 उनका गांधी को अवतार कहना शायद इसी अर्थ में है- गांधी की मूल चिंता धर्म -स्थापना के अर्थ में ही थी।
हमें पश्चिम और भारत के बीच के भेद के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। हमारी समीक्षाओं में, हमारे विवरणों में, हमारे उदाहरणों में और हमारे विमर्श में इस भेद के प्रति हमारा संचेतन दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। जिस तरह की हमारी पढ़ाई-लिखाई हुई है, जिस तरह के कथा-विमर्श (नैरटिव) से हम गुज़रे हैं, हमारे लिए पश्चिम और भारत में भेद कर पाना सहज नहीं होता। हमें मुश्किल होती है। कई बार हम पश्चिम की दृष्टि को ही घुमा-फ़िरा कर भारत पर और भारत के लोगों पर आरोपित करते हैं। ऐसा हम जाने-अनजाने अनेकों बार करते हैं। शायद रोज़ करते हैं। यह बात मैं अपने लिए (और अपने मित्रों के लिए) ही कर रहा हूँ।
३.
भारत के समाज में एक से अधिक करेन्सी (currency) रही हैं। धन एक करेन्सी है। इसके अलावा धान्य, गाय-बैल, भेड़-बकरी, सामान, सेवा इत्यादि भी currency रही हैं। पारम्परिक गाँव की अर्थव्यवस्था ऐसी थी, (जिसे हमें जजमानी व्यवस्था भी कह सकते हैं) कि जो परिवार जिस काम में लगा है, वह उसकी currency होती थी। किसान की currency अनाज था, कुम्हार-लोहार-चर्मकार इत्यादि की currency उनके उत्पाद थे, शिक्षक – चित्रकार – कथाकार इत्यादि की currency उनकी अपनी कला थी। भारत के गाँव में एक नहीं बल्कि अनेक करेन्सी चला करती थीं। इनके बीच आदान-प्रदान की एक सुगम व्यवस्था निर्मित थी।
उक्त लेख में लिखित चिंता उस व्यवस्था में पैदा होती है, जहाँ एक ही करेन्सी है। ऐसी व्यवस्था में यह प्रश्न खड़ा होता है कि अलग अलग श्रम को एक पैमाने पर कैसे बिठाया जाए। इस व्यवस्था में हमें किसान के श्रम को, कुम्हार के श्रम को, कथाकार के श्रम को, पंडित के श्रम को इत्यादि को एक स्केल पर बैठाना होता है। इसके लिए समाज की विविधता को ख़त्म करना लाज़मी हो जाता है। ऐसे में समाज स्वतः ही uniformity और standardization की तरफ़ बढ़ता है। और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए सत्ता का केंद्रीकरण करना पड़ता है।
भारत के समाज का एक बड़ा हिस्सा (मेरे अनुमान में एक-तिहाई जनसंख्या) भिक्षा वृत्ति का था। यह लोग कलाओं के पोषण-संरक्षण में अपना जीवन लगाते थे- कथावाचन, चित्रकारी, नृत्य, संगीत, नाट्य, कठपुतली इत्यादि। इनके अलावा चिकित्सा में लगे लोग भी इसी वृत्ति में आते थे। और फिर साधु-सन्यासी, पंडित-वेदमूर्ति इत्यादि भी होते थे। इन लोगों का भारत की सभ्यता में क्या योगदान रहा है? इस प्रश्न पर हमें विचार-विमर्श करना चाहिए। मेरे विचार से भारत “कृषि-प्रधान” सभ्यता नहीं रही है (जैसा पंडित नेहरू कह गए) और न ही भारत की सभ्यता ‘उद्योग-प्रधान’ थी। भारत एक ‘कथा-प्रधान’ (या कला-प्रधान) सभ्यता रही है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय यहाँ के भिक्षा-वृत्ति समाज को जाता है। हमारी सामाजिकता के निर्माण में भिक्षा वृत्ति का प्रयास प्रमुख रहा है। जिसे हम भारतीय समाज कहते हैं, उसकी संरचना भिक्षा वृत्ति के लोगों ने की है। आज भारत में सोसाएटी की कल्पना व्याप्त है- जिसकी मूल चिंता प्रॉपर्टी की वृद्धि और सुरक्षा है, समाज की कोई कल्पना ही नहीं है। समाज और सोसाएटी में हमें लगातार भेद बना कर चलना चाहिए।3
भिक्षा वृत्ति के ह्रास से भारत का समाज टूटा है। हम धर्म – अधर्म की चिंता छोड़ प्रॉपर्टी की चिंता में लग गए हैं – सभी के पास प्रॉपर्टी हो, सभी के पास बराबर प्रॉपर्टी हो। पिछले 150 वर्षों में भिक्षा-वृत्ति का ह्रास हुआ है – इसे मैं आधुनिक भारत की सबसे बड़ी त्रासदी मानता हूँ, यहाँ की ग़ुरबत से भी बड़ी त्रासदी।
४.
सुशोभित जी ने जो प्रश्न उठाया – किसी भी श्रम का मूल्यांकन कैसे किया जाए, यह एक मौलिक प्रश्न है। इस पर विचार-विमर्श होना चाहिए। सुशोभित जी की चिंता को मैं वाजिब ही मानता हूँ। इसके लिए भारतीय अर्थ-चिंतन को पकड़ना होगा। और शायद भारत में वृत्ति की अवधारणा को भी पकड़ना होगा – हमारे यहाँ तीन वृत्तियाँ मानी गई हैं, कर्म-वृत्ति, वैश्य-वृत्ति और भिक्षा-वृत्ति। अमरकण्टक के बाबा अग्रहार नागराज ने भी श्रम-मूल्य पर कुछ लिखा है। उसे भी देखना चाहिए।
इसके अलावा जो आर्थिक-बराबरी की उनकी चिंता है वो शायद मौलिक नहीं है। या फिर बुद्धिजीवियों की उनकी समीक्षा भी हल्की प्रतीत होती है। इस तरह की बात आधुनिक दृष्टि से आधुनिकता की समीक्षा जैसी लगती है। आधुनिक दृष्टि से आधुनिकता की समीक्षा पश्चिम में ख़ूब होती है। हम भी उसी चिंतन का हिस्सा बनने का प्रयास कर रहे हैं क्या? इसमें कुछ ग़लत नहीं है, लेकिन इसके प्रति सचेत तो होना ही चाहिए। वर्तमान में जो प्रचलित कथा-विमर्श है, वर्तमान में जो प्रचलित मूल्य हैं- जैसे freedom, equality, justice इत्यादि, हम इन्हें आधार बना कर अपने समाज का मूल्यांकन करते हैं। इसे हम ओब्जेक्टिव मूल्यांकन मानते हैं। मेरे विचार से यह एक त्रुटि है। हमारा मूल्यांकन हमारे ही आधारों से हो, यह ईष्ट है, जिसके लिए समाज में भारत के आधार क्या हो – इसके ऊपर भी संवाद व विमर्श होना चाहिए।
संदर्भ
- देखें आचार्य, नंदकिशोर “सभ्यता का विकल्प: गांधी-दृष्टि का पुनर्वलोकन” पृ.12 वागदेवी प्रकाशन, बीकानेर 1995
- देखें https://www.youtube.com/watch?v=wrA3dZ2EY7w
- देखें https://saarthaksamvaad.in/धर्म-और-हमारा-साधारण-समाज/
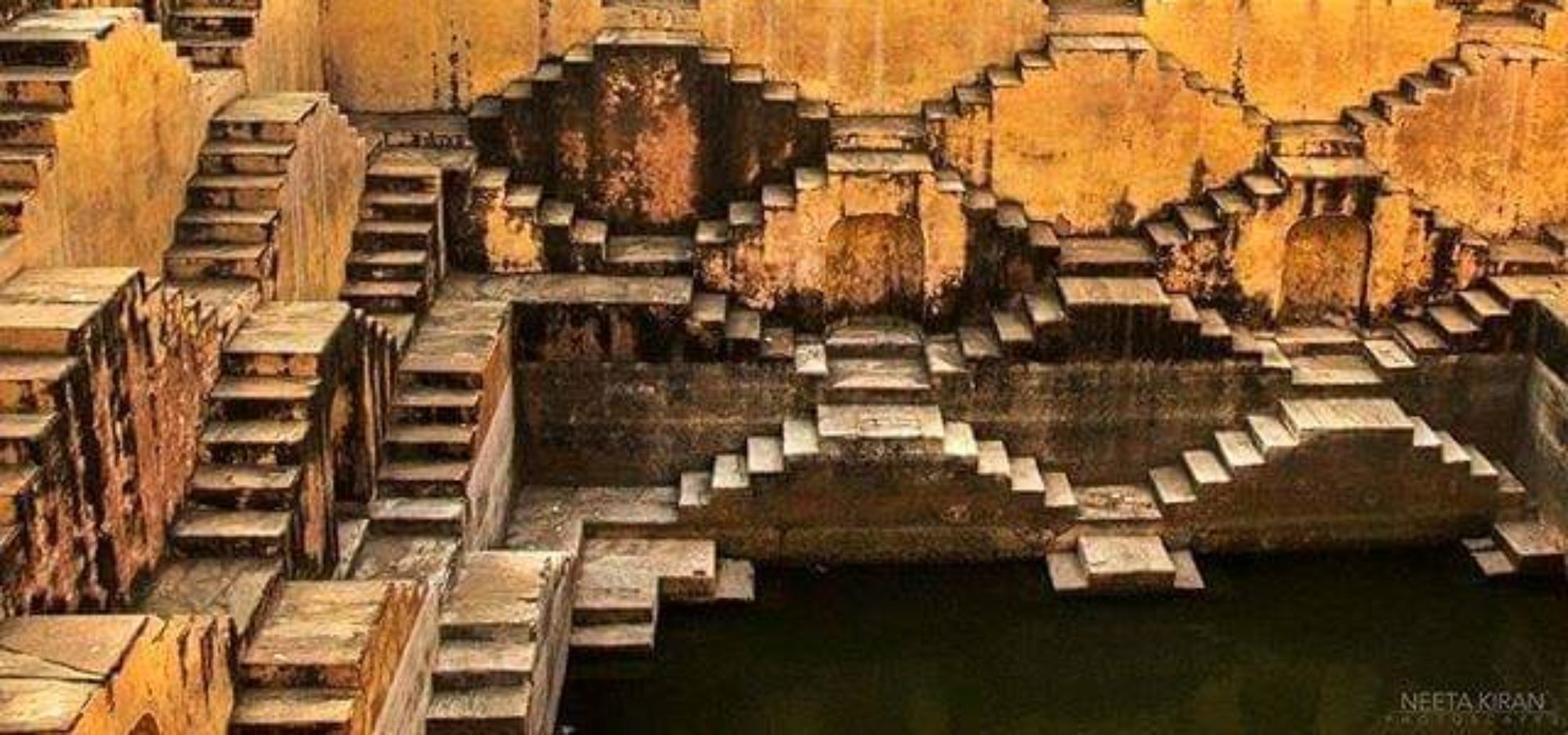

Leave a Reply