भारत में ही भारत के भारतीयों द्वारा विस्थापन की स्थिति में ७० वर्ष से नये बन रहे ‘आधुनिक’ भारत में क्या आपको अपनी आत्मछबि दिख रही है? अधिकतर भारतवासियों को अपनी छवि नहीं दिखती। इसी स्थिति को समझने के लिए हमें इस सवाल का सामना करना जरूरी है, कि हमारे आर्थिक, राजनैतिक, बौद्धिक – शैक्षिक – सांस्कृतिक और औद्योगिक जीवन में जिसे हम ‘अपना’, ‘भारतीय’ या भारत की प्रतिभा के प्रमाणरूप कह सकें – ऐसे किसी भी सिद्धांत, नियम, संस्था, मान्यता, तकनीक, व्यवहार, व्यवस्था इत्यादि का क्या स्थान है, उनकी क्या अहमियत है, क्या प्रतिष्ठा है?
यह सवाल राज्य और समाज बनाने वाले आधारभूत सभी तंत्रों के विषय में करना जरूरी है, ताकि हम अपनी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चेतना की स्थिति और गति को पहचान सके और राष्ट्र होने के अर्थ को समझकर राष्ट्र बने रह सके। गांधीजी की उस मूलभूत चेतावनी के संदर्भ में इस पर चिंतन – मनन करना जरूरी है, कि ”नकलचियों से राष्ट्र नहीं बनता।”
‘हमारा‘ अर्थात् भारतीय, राष्ट्रीय, होने का अर्थ:
किसी भी कृति, संस्था, तंत्र, विद्या, तकनीक, पद्धति इत्यादि का ‘हमारा अपना’ अर्थात् भारतीय यानि कि राष्ट्रीय होने का अर्थ क्या है? किसे कहेंगे, कि यह ‘हमारा’ है? किसी भी चीज का ‘अपनी’ होने का स्पष्ट – सा सबसे पहला प्रमाण है, कि उस पर हमारा अधिकार हो, वह हमारे नियंत्रण में हो, उसके साथ हमारा पारस्परिक सामंजस्य हो। अधिकार का अर्थ मालिकी अधिकार से मात्र नहीं है, जो बाहर से, बाज़ार से खरीदी हुई चीज पर भी होता है। अधिकार का अर्थ है, कि जिसके विषय में हम अधिकृत हो, प्रमाणभूत हो; जिस की संपूर्णता या संपूर्ण गति पर नियंत्रण हो; न कि उसकी किसी एक या आंशिक अवस्था पर नियंत्रण या अधिकार।
इसका एक तात्पर्य यह भी निकलता है, कि उसकी समस्त अवस्थाओं – विचार में, सिद्धांत में या कल्पना में उसकी अवधारणा बनने से लेकर उसकी उत्पत्ति, रूप – स्वरुप निर्धारण, विस्तार और क्षय; मूल्य, प्रतिष्ठा, उपयोग इत्यादि सभी अवस्थाओं के विषय में हम अधिकृत, प्रमाणभूत, अंतिम प्रमाण और अंतिम संदर्भ माने जाते हों।
जिसके संदर्भ में हम यह चर्चा कर रहे हैं, उन सबका हमारे लिये ‘अपना’ होने का एक और महत्वपूर्ण अर्थ है, कि हम उनके वसियतधारी वारिस ही केवल न हो, लेकिन उसमें बढ़ौतरी करके उसे हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को थमाते हो – एक अविरत, निरंतर, अनंत धारा की तरह। जो हमने इस निरंतर धारा में रहकर और होने के अधिकार के और जिम्मेदारी के साथ पाया होता है और जिसका हम आने वाली पिढ़ी को हस्तांतरण करते हैं। उसीसे राष्ट्र बनता है।
जिसकी वसियत में हमारा नाम ही न हो, वह हमारा नहीं हो सकता। जो हमारे पुरखों से प्राप्त न हो, जो हमारी अपनी ज्ञान परम्परा की पैदाइश न हो, जो हमारी खोज न हो, वह हमारे तात्कालिक, सुविधाजनक उपभोग की चीज हो सकती है, हमारी पहचान उससे नहीं हो सकती; वह हमारे स्वत्व का प्रमाण नहीं हो सकती, भले ही हमारे वर्तमान अस्तित्व में उसने जगह बना ली हो।
‘आधुनिक’ कही जाने वाली एक भी चीज के हम वसियतधारी अधिकृत वारिस नहीं है। उन्हें हमें न तो खोजा है, न अपने पुरुषार्थ से पाया है। उनकी वसियत में, एक से दूसरी पीढ़ी और अनंत काल तक उसके हस्तांतरण और संजोने के दायित्व की वसियत में हमारा नाम न तो है, न ही हो सकता है। या तो वे चीजें हम पर लादी गई हैं और हमने चूपचाप आज्ञाकारी विद्यार्थी, सेवक या भक्त की तरह उन्हें अपना लिया है; या खरीदा है, या वो हमें उधार या सशर्त, या प्रयोग के तौर पर (हमारी जानकारी में या धोखे से) मिला है।
उन चीजों से हमारा संबंध, हमारे अधिकार की सीमा और स्वरूप केवल उनके पुनरूत्पादन या नकल करने तथा उपयोग के अनुकूल मामूली ऊपरी ऊपरी तब्दीलियाँ करने तक ही सीमित है। चाहें तो भी इससे अधिक हमारा अधिकार हो भी नहीं सकता, क्योंकि उनमें से एककी भी कल्पना, अवधान, गर्भाधान तथा जन्म के लिये हम जिम्मेदार हैं ही नहीं। उन पर हमारी सत्ता इसलिए हो नहीं सकती, क्योंकि उनके विषय में हम न तो अंतिम प्रमाण हैं, न उनकी आत्मा के संचालक, या चरित्र और स्वभाव के निर्धारक तथा निर्णायक। उनमें से एक में भी भारत का बीज नहीं है।
उपयोग या व्यवहार में आने की तथा सार्वजनिक होने की अवस्था उन अनेक अवस्थाओं में से एक है, जहाँ उसके मूलभूत चरित्र और स्वभाव में परिवर्तन की कोई गुंजाईश नहीं रह जाती, उदाहरण के लिए ‘वेस्ट मिन्स्टर’ बहुदलीय संसद प्रणाली ले लें; या ‘लॉकोमोटीव’ – ट्रेन, कार इत्यादि; या आधुनिक खेती के तरीके ले लें; या कोई भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का साधन – सरंजाम ले लें। उपयोग में लाने पर उनके जाने और अधिकतर अनजाने परिणामों, प्रभाव और दुष्प्रभाव; उसकी जरूरतें, उसकी भूख और उसकी आदतें, सब उसके बीजधारण और जन्म से ही तय हो चुका होता है।
मनुष्य के पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक जीवन में इससे आने वाले बदलाव या दुष्प्रभाव जैसे – जैसे उनका उपयोग करते हैं, सामने आने लगते हैं – स्थान और समय से प्रभावित होकर, लेकिन यदि उसका उपभोग या उपयोग करने वाले ऐसा मान लें, कि वह टेक्नोलॉजी, तन्त्र, व्यवस्था या संस्था इत्यादि उनके नियंत्रण में है और उसके उपयोग से किस प्रकार, कौन – से और किस मात्रा में परिणाम लाये जाय – वह वे निर्धारित कर लेंगे, तो वह केवल भयानक, आत्मघाती, भ्रम और आधुनिक चीजों के विषय में घोर नासमझी है।
जब हमारे अधिकार की कोई भी टेक्नोलॉजी, संस्था विद्या और ज्ञान परंपरा – कोई भी मौलिक रूप से भारतीय चीज हमारे जीवन को सार्थक रूप से प्रेरित, संचालित और मार्गदर्शित नहीं कर रही है, तब सवाल तो यह पैदा होता है, कि क्या हम केवल जन्म से ही भारतीय रह गए; चरित्र और कर्म से नहीं?
यदि हम किसी भी शाश्वत और मौलिक रूप से भारतीय चीज के धारक, संवर्धक और वाहक नहीं हैं, तो हम ऐसा दैहिक ढाँचा हैं, जिसमें प्राण, बुद्धि और विचार किसी और के हैं। भारत की काया में किसी और के प्राण प्रवेश कर चूके हैं। उसका आत्मबोध यदि समाप्त नहीं हुआ है, तो बेहद क्षीण तो हो ही गया है।
गांधीजी के मार्गदर्शन और उनके प्रयोग की सार्थकता के बावजूद आज हमारे पढ़े लिखे, ‘विकसित’ लोगों के हाल तो यह हैं, कि उन्हें भारतीय संस्कृति से न तो कुछ लेना देना है; अधिकतर तो उनके मन में हीनभाव ही है। हमारा असली सांस्कृतिक रूप क्या है, इसे जानने की इनमें कोई दिलचस्पी, जिज्ञासा नहीं है, यदि वे जानने का प्रयास करते हैं, जानकारी लेते भी हैं, तो उनमें यह भाव पैदा नहीं हेाता, कि उन्होंने खुद को जाना है, खुद की ही खोज की है; खुद के ही सत्य का साक्षात्कार किया है। ‘भारत की खोज’ वे तीसरे पुरुष एकवचन के रिश्ते से करते हैं, मानो वे इसके अंश ही न हों।
संभ्रांत और पढ़े – लिखे वर्ग में उनकी भारतीय मौलिकता, बुद्धि और मन उनकी आत्म-चेतना के किसी अंधेरे कोने में दब गये हैं। उनकी भारतीयता उन्हें चूक गई है। हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी इस अवस्था के गंभीर पक्षों और नतीजों के प्रति आंखें मूंदे हुए है। अधिक से अधिक हम एक ऐसा भारत खड़ा कर रहे हैं, जो विक्षिप्त हो, न परम्परा में, न आधुनिकता में। उसके पुराने संस्कार ‘पुराने’ बनकर कहीं दबे पड़े हैं और केवल व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन में क्रिया – कर्म – कांड के रूप में सामने आते रहते हैं। जबकि हमारे सक्रिय सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक व्यवहार हम जिस मन और विचार से करते हैं, उनमें हमारे दबे पड़े संस्कार – मन – बुद्धि की कोई सार्थक निरंतरता नहीं है, न ही भूमिका है।
भारतीय मन – बुद्धि पर पाश्चात्य मन – बुद्धि हावी – प्रभावी है। वही हमें अपनी बोली में उसकी भाषा बुलवाता है, उसके नचाए हम नाचते हैं और उसीसे प्रेरित होकर हम सोचते हैं और समझते हैं, कि हमारे विचार – हमारे अपने हैं, मौलिक है, सही जगह से निकले हैं और सही जगह ले जायेंगे। यदि ऐसा न होता, तो हम इस लक्ष्य के किस पायदान पर हैं, अगले मुकाम कौन से हैं और कैसे हैं वह सब स्पष्ट होता।
किसी स्पर्धा या संवाद से नहीं, लेकिन आक्रमण से आयी सभ्यता के खाके में हम समा रहे हैं। हमारे निर्णय उनके मानदंडों के समर्थन में होते हैं। फिर हमारी राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद क्या है? भारतीय राष्ट्र की स्वचेतना, उसका आत्मबोध, उसकी आधारभूत मौलिकता के विस्थापित हो जाने के बाद किस आधार और अधिकार से हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाये रख सकते हैं? यही मूलभूत प्रश्न गांधीजी ने राजनैतिक आजादी के सम्बन्ध में रख दिया था।
भारत या हिन्दुस्तान जो भी कहें – हमारे राष्ट्र का अर्थ और अस्तित्व ही पारंपरिक होने में है। ‘आधुनिक भारत’ एक विरोधाभासी नाम और विरोधाभासी पहचान है; असल में तो पहचान है ही नहीं। यह मिटती हुई पहचान का सांकेतिक परिचय है, इन दो शब्दों में आश्वासन है – उन्हें, जिनका ‘प्रोजेक्ट’ भारत को पाश्चात्य सभ्यता का एजेंट और अंग बनाने का है।
यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है, कि ‘परंपरा’ शब्द का हम निहायत गलत अर्थ करते रहे हैं। लोकाचार, रीति –रिवाज, व्यवहार में चली आ रही कोई भी चीज ‘परंपरा’ नहीं कही जाती, जबकि हम हर कुरीति, कुप्रथा को भी ‘परंपरा’ कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ‘परम्परा’ का संक्षेप में अर्थ है: वह ज्ञान और विद्या जो ‘परम्’ या प्रामाणिक स्त्रोत से उत्पन्न है। यह परम् स्त्रोत परम् ज्ञान या परम् पुरुष हो सकते हैं। दूसरे, उसकी धारा निरंतर, अविच्छिन्न होनी चाहिए और तीसरी कसौटी यह है, कि तार्किक प्रमाणों से जिसे सिद्ध किया जा सके।
गांधीजी ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया है, कि जिसे सत्य, अहिंसा और तर्क (विवेक) के मापदण्ड पर खरा पाया जाय, वही परम्परा कही जानी चाहिए। इस सार्वभौमिक सार्वकालिक कसौटी के बाद ‘पाश्चात्य’ या ‘भारतीय’ होना कसौटी का मूलभूत और अंतिम आधार नहीं रह जाता। व्यवहार में उनके लिए और तब तक यह आधार हो सकता है, जब तक कि हम ‘परम्परा’ के अर्थ को इस प्रकार अपनी भाषा में आत्मसात नहीं कर पाते।
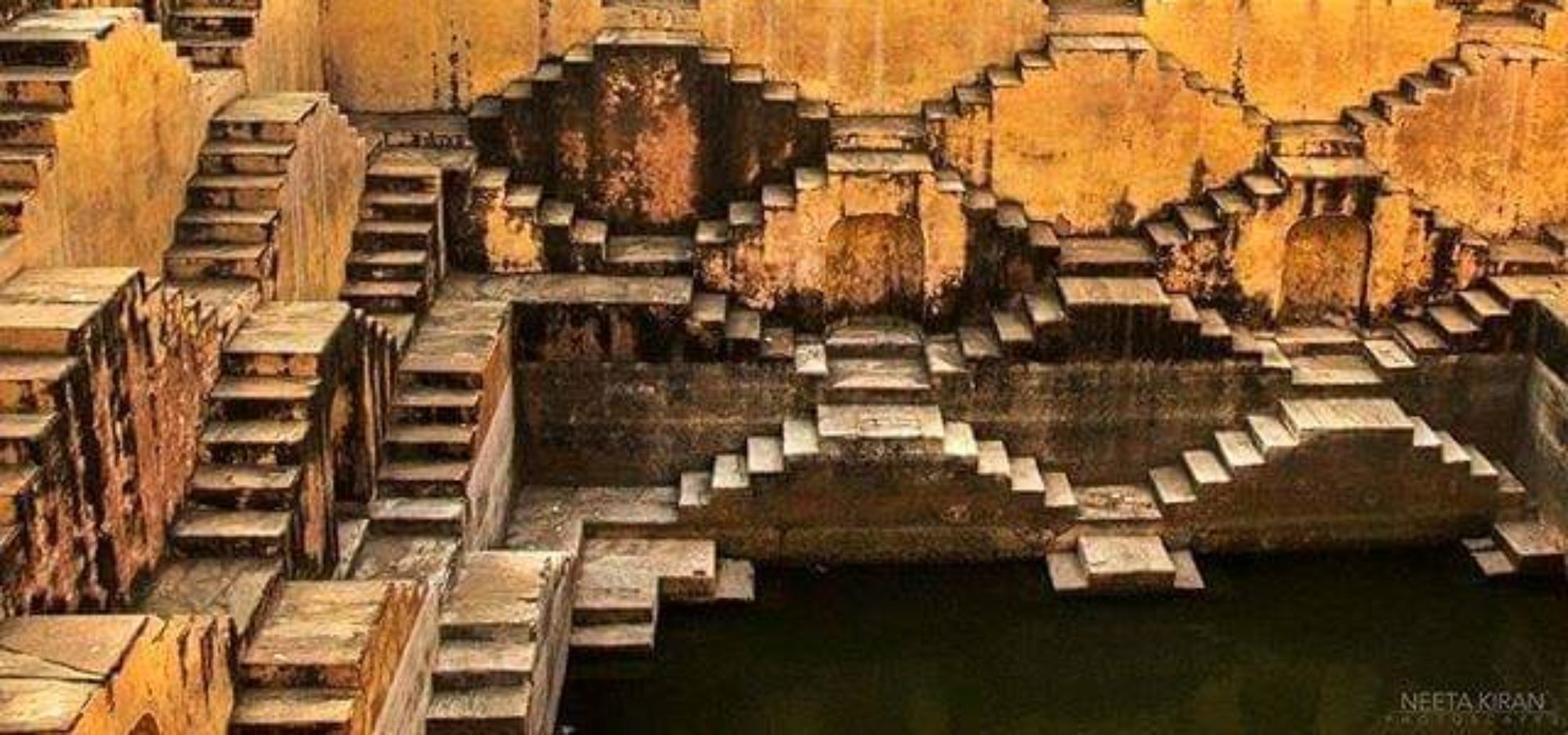

Leave a Reply