भाग १ पढ़ने के लिए यहाँ click करें।
भाषा केवल शब्द और व्याकरण नहीं है। भाषा के लिए शायद बेहतर शब्द बोली है: जो बोलना चाहते हैं, उससे भाषा बनती है। हमारी बोली में हमारी जीवन दृष्टि बोलती है, हमारे जीवन सिद्धांत बोलते हैं; हमारी विश्व दृष्टि बोलती है। क्या तमिल प्रजा जिसकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी बात अंग्रेज द्वारा अपनी जरूरतों के अनुसार विकसित भाषा में कह सकती है?
अपनी भौतिक जरूरतों के लिए अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, डच भाषा चल सकती है। प्रजा अगर जीवन केवल भौतिकता के स्तर पर ही जी रही है और अंतिम हेतु केवल अस्तित्व को टिकाये रखना है, तो अंग्रेजी उत्तम भाषा है। छोड़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टि यूरोपीय आधुनिक सभ्यता का मूल स्वभाव है और भाषा में संस्कृति – सभ्यता बोलती है।
आधुनिक जीवन किसी भी प्रकार हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में सनातन सिद्धांतो का प्रतिक या प्रमाण नहीं है। हम काम चलाऊ जीवन जीतें है। सयोंगों द्वारा निर्मित प्रासंगिकता और आकस्मिकता हमारे जीवन की राह तय करती रहती है। आधुनिकता की भूल भुलैया में खुशी से रमे हुए लोगों के लिये अंग्रेजी भाषा ही उपयुक्त है, क्योंकि किन्हीं सनातन जीवन सिद्धांतो और मूल्यों से ओत-प्रोत जीवनशैली और विचारशैली से वर्तमान अंग्रेजी भाषा का लेना देना नहीं है। जो इस भूल भुलैया में फँसे हैं, जिन्हें धर्म की दरकार है; जीवन में सनातन सिद्धांतो की दरकार है; जो अपने स्वत्व को, अपने आत्मबोध को खोये हुए नहीं हैं और खोना नहीं चाहते, जो अपने स्वत्व को जीवन में स्थापित देखना चाहते हैं; जिनके लिए अपने धर्मशास्त्र प्रमाणभूत हैं, आर्ष सत्य और आर्ष वाक्यों को जिन्होंने नकार नहीं दिया है, अपनी परम्परा का जिन्हें मूल्य है; उनके मन की बात अंग्रेजी कैसे कह सकती है?
यही कारण है, कि हमारे उच्च शिक्षित और प्रशासनिक अधिकारी समाज से कटे हुए हैं, असामाजिक हैं। यही स्थिति न्यायाधीशों और पूरी न्याय व्यवस्था की है। पत्रकारों और शिक्षा संस्थानों की है। कॉर्पोरेट जगत तो चलता ही इसी के बल पर है। अंग्रेजी भाषा भारत को अपनी सभ्यता से दखल कर पाश्चात्य सभ्यता का अंगभूत देश बनाने के लिए है। यह भारत के “समाज परिवर्तन”, “सेक्युलराइजेशन” की भाषा है। पश्चिम के उस प्रोजेक्ट की भाषा है, जो भारत को “पिछड़ेपन” और “जाहिलियत” से “सभ्य”, “विकसित” बनाने का है, यह उसके रूपांतरण, ‘कीड़े’ में से ‘मनुष्य’ बनाने के ‘मेटामॉरफोसिस’ की साधन रूप भाषा है (‘मेटामॉरफोसिस’ महान लेखक काफ्का की १९१२ में लिखी अद्भुत कहानी है, जो समर्थ समाज वैज्ञानिकों के लिए मनुष्य समाजों के किये जा रहे परिवर्तन को समझने का आधार बन गयी )।
लेकिन जिस सभ्यता की नींव आध्यात्मिकता में हो, उस प्रजा का स्वत्व भौतिकता की बैठक पर खड़ी भाषा में अभिव्यक्त नहीं हो सकता, केवल काम चलाऊ अनुवाद हो सकता है और वह भी अप्रमाणभूत। अंग्रेजी को अपनाकर क्या हम इस अद्वितीय सभ्यता की संस्कृति से आने वाली पीढ़ियों को वंचित कर देना चाहते हैं और पश्चिम की सभ्यता का गुलाम राष्ट्र बन जाना चाहते हैं? जो अंग्रेजी के गुलाम हो चूके हैं, उसमें रम गए हैं और जिन्हें सपने भी अंग्रेजी में आते हैं, उनकी बात छोड़िए, बाकी लोग जिनके ऊपर उसका बोझ है, जो उसमें फँसे हैं, वे कैसे उससे मुक्त हो जाए और अंग्रेजी केवल उतनी रहे, जितनी कि आंतरराष्ट्रीय व्यवहार के लिए जरूरी है, उसके उपाय सोचना आवश्यक है।
जिस दिन ऐसा हो गया, देश की दमित प्रतिभा खिल उठेगी। देश अपनी आजादी का अर्थ समझने और उसे अर्थवान बनाने लगेगा। सामान्य लोगों को जो यह लग रहा है, कि देश और उसका राज्य अंग्रेजी पढ़े लिखों का है, वह उन्हें अपना दिखने लगेगा। अपनी आत्मछवि जो उन्हें नए भारत में नहीं दिखती, वह दिखने लगेगी।
भाषा-समृद्धि सापेक्ष होती है
हम शायद यह मान के चल रहे हैं, कि अगर अपने भाषा परिवार के बाहर की किसी भी भाषा पर अगर प्रभुत्व हो, तो अपने स्वत्व, स्वभाव, संस्कृति को, अपने मन के प्रमाणभूत भाव और विचार को उतने ही या, अंग्रेजी के कुछ विशेष पक्षधरों के अनुसार, अधिक सार्थकता और सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। हकीकत तो दरअसल में यह है, कि सामान्य लोगों का अपनी भाषा पर जैसा अधिकार, प्रभुत्व होता है, वैसा प्रभुत्व अंग्रेजी पर अंग्रेजी के ऊँचे प्रोफेसर भी प्राप्त नहीं कर सकते। वीरले लोग ही ऐसा कर सकते हैं।
शायद हम एक और गलतफहमी में रहते हैं, कि सामान्य, ‘अनपढ़’ लोग भाषा में कमजोर होते हैं, कि उनका भाषा विन्यास बहुत ही संकुचित और संकीर्ण होता है। यह भारी गलत धारणा है। जितना अंग्रेजी के प्राध्यापक का प्रभुत्व और भाषा विन्यास अंग्रेजी का होता होगा, उससे कहीं अधिक इन ‘ग्राम्य’ लोगों का अपनी भाषा का भाषाविन्यास होता है।
प्रतीकों और मुहावरों से समृद्ध इन बोलियों को शब्दों के घटाटोप की जरूरत नहीं होती, लेकिन साथ ही प्रकृति और धर्म के साथ का उनका एकात्म गहन सम्बन्ध उनकी भाषा में झलकता है।
उदाहरणार्थ, वर्षा के बादलों की अलग अलग छटा और प्रकार के लिए उत्तर प्रदेश के किसान नब्बे शब्द, सौराष्ट्र की जनजाति चारण आपको चाल और स्वाभाव के हिसाब से घोड़ों के लिए पच्चीस अलग अलग गुणवाचक नाम बता देंगे। राजस्थान के रण में पता नहीं हवा के बारीक़ से बारीक़ अलग अलग रूख और उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश और गर्मी के लिए कितने ही शब्द होंगे! भक्ति के नव प्रकार क्या अंग्रेजी संस्कृति में हैं?
एक और बात। अगर किसी समुदाय का भाषाविन्यास मानो कि इतना नहीं भी है, तब भी यह सत्य है, कि कम शब्दों में वे ज्यादा बड़ा सत्य कह देने में समर्थ होते हैं, क्योंकि अनुभव अपनी बोली में स्वतः बोल उठता है, अप्रयास। उनके अपने कवि शायर दो पंक्तियों में वह बात कह देते हैं, जो कहने के लिए हमें आपको घंटा भर का भाषण देना पड़ता है! शायद इसलिए भी, कि ज्ञान और जीवन के बीच जितना कम भेद, इतना ही शब्दों की कम जरूरत पड़ती है।
अपने अनुभव को कहने में लोक भाषाओं के जाने माने अध्येता डॉ कपिल तिवारी ने बेहतरीन दृष्टांत दिया। एक आदिवासी किसान से आज की खेती पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उसने सहज ही कह दिया: “खेत में दवाई डालोगे, तो तुम्हें भी दवाई खानी पड़ेगी।” इस के सामने पर्यावरणवाद की लम्बी चौड़ी फीकी उबाऊ और आडम्बरपूर्ण बनावटी आयातीत भाषा कहाँ ठहरेगी? सत्य के जितना करीब, शब्द इतने ही कम होते जाते हैं। गीता कितना छोटा ग्रन्थ है; हिन्द – स्वराज केवल ८७ पृष्ठ की पुस्तिका है। एक में समस्त विश्व का, कालातीत सत्य कह दिया गया है, दूसरे में हमारे काल का सत्य कह दिया गया है।
क्रमश:
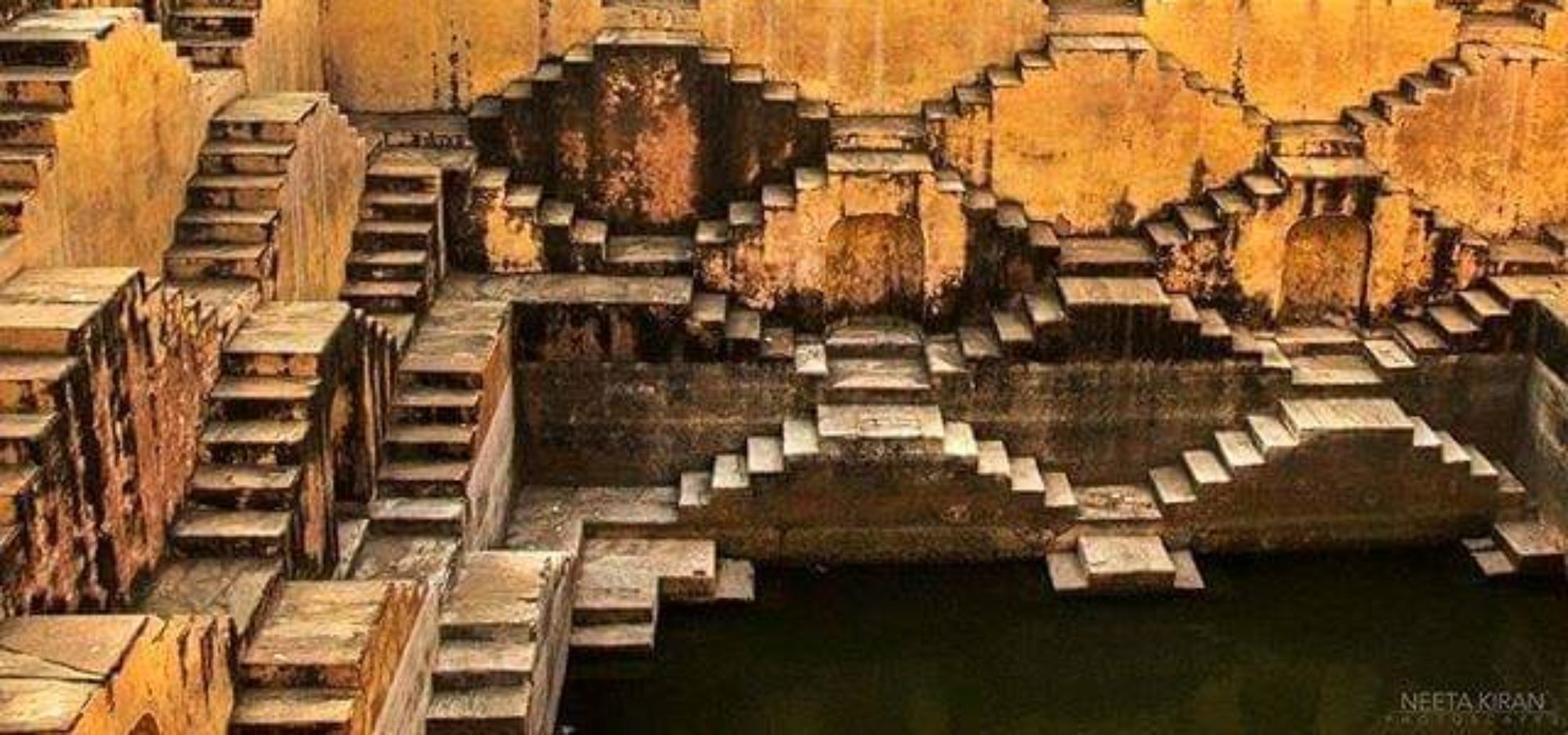

Leave a Reply