मानव जीवन तीन प्रकार के सम्बन्धों में विस्तृत है। या यह भी कह सकते हैं, कि बंधा हुआ है: मनुष्य का अन्य मनुष्यों से सम्बन्ध; मनुष्य का प्राकृतिक विश्व के साथ सम्बन्ध और मनुष्य का परम तत्त्व – ईश्वर के साथ सम्बन्ध। तीन रिश्ते सम्पूर्ण रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि तीसरा अगर जीवन में न हो, तो नैतिकता की प्रेरणा का कोई निरपेक्ष आधार नहीं रहता।
मनुष्य हिंसक रास्ता अपनाएगा, जैसे कम्युनिज्म ने किया है। राजनीति केवल प्रथम रिश्ते में ही आती है, बाकी दो में नहीं। किसान प्रकृति से अन्न पैदा करता है, उसके और प्रकृति के बीच कौन सी राजनीति है? प्रेम है, भक्ति है, कवित्त्व, साहित्यिक प्रतिभा, सौंदर्य बोध और कला है। ये गुण मनुष्य में कौन भरता है? उनका उपयोग राजनीति के लिए हो सकता है, लेकिन वे राजनीति से स्वायत्त सत्ता है। उनकी सत्ता राजनीति पर आधारित नहीं है। मनुष्य किसान, कारीगर, मजदूर या किसी और स्वरूप में जो भी पैदा करता है, उस क्रिया में राजनीति कहाँ आती है? वे ऐसी ही क्रियाएँ हैं, जैसे माता शिशु को जन्म देती है। वे सब स्वतः सिद्ध हैं। केवल जब उन उत्पादों का अन्य मनुष्य से विनिमय करने की बात आती है, तब राजनीति आती है। वहाँ भी राजनीति तब आती है, जब समाज की इकाइयाँ स्वावलम्बी न हो, पारस्परिकता आधारित सहकारी रिश्तो में न हो, कर्तव्य भाव से काम न किया जाता हो, स्वानुशासन न हो। राजनीति अनुशासन के लिए है, स्वानुशासित प्रजा में राजनीति का दायरा सिमित होता है, जहाँ राज्य समाज की एक इकाई होता है। आज की तरह नहीं, कि केवल राज्य ही राज्य हो, समाज कहीं नहीं। भारतीय परम्परा राज्य की नहीं है। अगर हमें नैतिक राज्य व्यवस्था की खेवना है, जोकि गांधी जी के नेतृत्व के आंदोलन का मुख्य हेतु था और सामान्य लोगों – हिन्दू, मुस्लिम सबके मन की बात थी, संस्कार और परम्परा की बात थी, तो मौजूदा पाश्चात्य प्रणाली के राज्य को एक अस्थायी व्यवस्था ही मानना पडेगा, न कि भारत की सनातन नियति। जो हार चुके हैं, पश्चिम को साष्टांग दण्डवत प्रणाम की मुद्रा धारण कर लिये हैं, उनके लिए तो यह बहुदलीय संसदीय प्रणाली सर्व गुण संपन्न है। इनका जमीर मर चुका है।
जो राजनीति को ही जीवन का सत्य समझते हैं, वे एक तिहाई जीवन को ही जीवन समझते हैं; उतना ही नहीं, वे पूर्ण सेक्युलर (मनुष्य सत्तावादी) हो गए हैं। मार्क्सवाद ने हमारी बुद्धि कितनी भ्रष्ट कर दी है, उसीका यह प्रमाण है, कि हम स्वाधीन चैतन्यपूर्ण मनुष्य और स्वाधीन चैतन्यपूर्ण समाज की बात भी नहीं कर सकते। राजनीति का स्थान समाज में केवल इतना ही होना उचित है, जैसे पंगु को या वृद्ध को लाठी का सहारा और राष्ट्र की सुरक्षा के एक पक्ष के सन्दर्भ में, क्योंकि सुरक्षा के अनेक आयाम हैं, जो राजनीति और राज्य से स्वतंत्र होते हैं। बाह्य और आंतरिक दुश्मनों से सुरक्षा राज्य का धर्म है और सैन्यशक्ति संसदीय राजनीति (दलीय) से स्वतंत्र ही होनी चाहिए।
राज्य हमेशा रहेगा, लेकिन राज्यसत्ता का अर्थ वही नहीं, जो आधुनिकता ने हमें घुट्टी की तरह पिला दिया है। जिसमें राज्य समाज को और समाज की समस्त इकाइयों की सत्ता को हड़प कर के सर्व सत्ताधीश बना हुआ है। जिनका स्वार्थ इस से जुड़ा है, वे सवाल खड़ा नहीं करना चाहते और जो सवाल करते हैं, उन्हें उलटा समझते हैं। यह कथन ही हम भूल गए, कि जो कम से कम शासन करता है, वही उत्तम राज्य होता है – स्वयं शासित समाज के प्रति प्रतिबद्ध, हालाँकि कम्युनिझम ने भी अपना अंतिम उद्देश्य राज्यसत्ता की समाप्ति बताया, लेकिन ऐसी अवस्था प्राप्त करना मनुष्य के अंदर की अच्छाई का परिणाम होता है और मार्क्सवाद में मनुष्य की अंदर की अच्छाई के लिए कोई प्रेरणा नहीं है। तानाशाही की, लाखों लोगों की कतल की प्रेरणा है। (और यह केवल गांधी जी और जय प्रकाश जी ही देख पाए, नेहरू तो कम्युनिज्म के अंध प्रेम में पड़ गए, यहाँ तक कि यह लिख दिया कि लेनिन अगर भारत में होते, तो उन्हें महान संत घोषित किया जाता!!!) अगर आप मार्क्सवादी हैं, तो सही है, कि जीवन सम्पूर्ण रूप से राज्य सत्ता और उसकी राजनीति का बंधक है, अगर मार्क्सवादी नहीं होने पर भी जो ऐसा मानते हैं, तो उसका अर्थ यह है, कि उन्हें पता तक नहीं है, कि उनका दिल दिमाग किसके कब्जे में है। मतलब वे बौद्धिक नैतिक रूप से निद्रावस्था में हैं। कुम्भकर्ण की तरह!
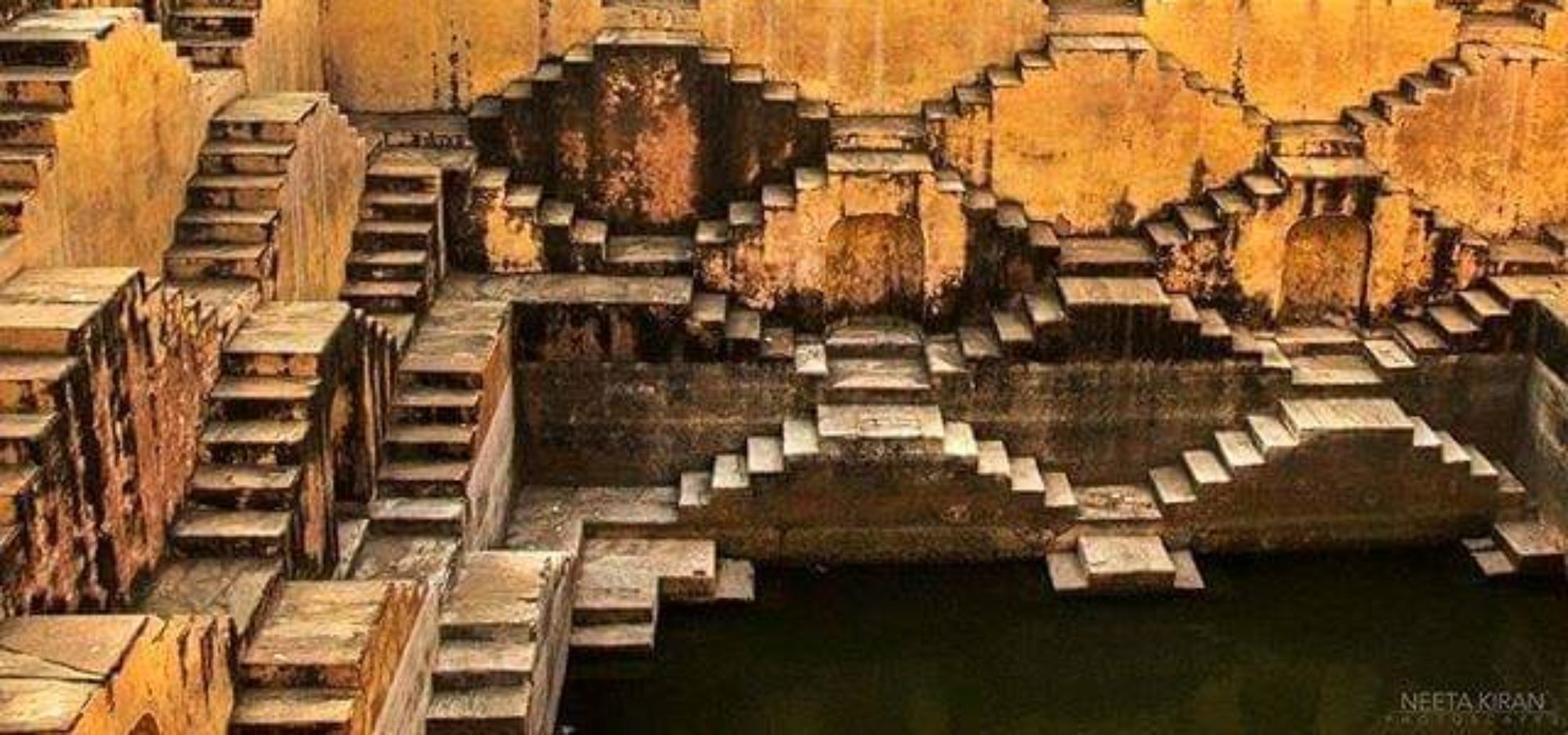

Leave a Reply