हिन्द स्वराज में महात्मा गांधी ने प्रश्न किया था, कि वकील मज़दूर से ज़्यादा रोज़ी क्यों मांगते हैं? उनकी ज़रूरतें मज़दूर से ज़्यादा क्यों हैं? उन्होंने मज़दूर से ज़्यादा देश का क्या भला किया है?
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिस पर हिन्द स्वराज लिखे जाने के 113 वर्षों बाद भी पर्याप्त मनन नहीं हो सका है। वहाँ पर महात्मा गांधी वकीलों के बहाने बुद्धिजीवी वर्ग की ओर संकेत कर रहे थे। इसमें आप वकील के साथ ही अफ़सर, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक, नीति-निर्माता, क़ानून-निर्माता, ठेकेदार और तमाम तरह के वित्तपोषक-हितग्राहियों को भी जोड़ सकते हैं। हर वो वर्ग, जो बुद्धिबल से रोज़ी कमाता है, वह श्रमबल से रोज़ी कमाने वाले की तुलना में अधिक धन कमाता है। गांधीजी का प्रश्न है, कि ऐसा क्यों?
इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह एक विचित्र स्थिति है, जिसमें आय का अनुपात आश्चर्यजनक रूप से विषम है। थोड़ा-बहुत अंतर होता तो कोई बात नहीं थी, किंतु आप देखेंगे कि बुद्धिजीवी के काम के घंटे श्रमजीवी की तुलना में कहीं कम होते हैं और उसका वेतन श्रमजीवी की तुलना में कई गुना अधिक होता है। गांधीजी पूछते हैं बुद्धिजीवियों में ऐसे कौन-से सुरख़ाब के पर लगे हैं, जो उनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, उनकी आमदनी ज़्यादा है, जबकि समाज में उनका रचनात्मक योगदान ना के बराबर है। वास्तव में अधिकतर बुद्धिजीवी तो उलटे समाज में वैमनस्य बढ़ाने का ही काम करते हैं। हिन्द स्वराज में हिन्दुस्तान की दशा शीर्षक से लिखे गए पाँच अध्याय इस परिप्रेक्ष्य में पठनीय हैं।
हिन्द स्वराज 1908 में लिखी गई थी। तब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। मज़े की बात है कि तब वो स्वयं वकालत करते थे। अलबत्ता उन्होंने अपने जीवन में शारीरिक श्रम को सदैव ही एक केंद्रीय स्थान दिया था, किंतु उन्हें अपनी आजीविका बुद्धिबल से प्राप्त होती थी। राजकोट में क़ानून की अर्ज़ियां लिखने से दक्षिण अफ्रीका में प्रतिवेदन और हलफ़नामा पेश करने तक उनका मुख्य कार्य दिमाग़ी-कसरत का ही था। कालान्तर में वे लेखन और पत्रकारिता की दिशा में भी प्रवृत्त हुए, अलबत्ता न्यासिता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके और स्वत्वाधिकार का विरोध करके उन्होंने बुद्धिबल से वित्तीय-लाभ कमाने की वृत्ति की अवहेलना ही की थी। आप देखिए, कि वकील होकर वो वकीलों के बारे में कह रहे हैं, कि उन्हें मज़दूरों से ज़्यादा वेतन लेने का अधिकार नहीं। ऐसी खरी और देशी बातें ही मुझको बारम्बार महात्मा गांधी की ओर खींचती हैं। उनका राजनैतिक-जीवन मुझे उतना नहीं लुभाता, जितना सामाजिक-चिंतन। उसमें बहुत मूल्य है और बड़ी दीर्घकालीन प्रासंगिकताएँ हैं, मानवीय-महत्त्व के टिकाऊ प्रश्न हैं।
बीते दिनों हमने देखा, कि एक प्रतिष्ठित लेखक ने साक्षात्कार देने के ऐवज़ में 25 हज़ार रुपयों की अनुचित माँग की और सम्पूर्ण लेखक-समुदाय ने एकमत से इसका समर्थन किया। मुझे कोई ऐसा लेखक नहीं दिखा, जिसने इसकी भर्त्सना की हो। इसके पीछे उचित-अनुचित का चिंतन था या अपनी बिरादरी के हित की चिंता थी? आज समाज की अनेक बुराइयों के मूल में यह भी है, कि मनुष्य अपनी बिरादरी के हितों को किसी क़ीमत पर ताक पर नहीं रखता और अपने तात्कालिक लाभ के लिए औचित्य के दीर्घकालिक-प्रश्नों को दरकिनार कर देता है। महात्मा गांधी ने वकील होकर वकीलों के अनुचित आचरण पर प्रश्न किया था, लेखकों ने लेखक होने के कारण अपनी बिरादरी के एक व्यक्ति के अनुचित आचरण का समर्थन किया। बहुत कम आज ऐसा दिखलाई देता है कि कोई व्यक्ति अपनी बिरादरी से सम्बंधित प्रश्नों पर, तात्कालिक हितों को नज़रंदाज़ करते हुए, नीर-क्षीर-विवेक की बात सामने रखता हो।
प्रश्न तो यह भी है, कि वेतनमानों का निर्धारण किसने किया? यह किसने निश्चय किया कि श्रमजीवी न्यूनतम वेतन पाएगा और बुद्धिजीवी ना केवल आवश्यकता से अधिक धन कमाएगा, बल्कि हर साल उसके वेतन में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी ही होती जाएगी? यहाँ पर बुद्धिबल और देहबल की तुलना करने का प्रयास नहीं है, क्योंकि दोनों का स्वरूप भिन्न होता है और यह सच है, कि बुद्धिबल के पीछे वर्षों की एकान्त-साधना निहित होती है। किंतु इतना अवश्य है कि समाज में आर्थिक-विषमताओं के मूल में जितना चिंतन पूँजीपति-श्रमिक के वर्गभेद पर किया गया है, उतना बुद्धिजीवी-श्रमजीवी के वर्गभेद पर नहीं किया गया है। इन दोनों के वेतन में आज आकाश-पाताल का भेद हो गया है। सुरसा के मुख की तरह बुद्धिजीवी की सुखभोग की लिप्सा बढ़ती ही जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो बहुत बुनियादी रूप से ग़लत है।
जबकि बुद्धिजीवी ने निठल्ला और निकम्मा होने के बाद समाज में कलुष बढ़ाने में ही अधिक योगदान दिया है- इसमें संदेह नहीं है। इंटरनेट-युग में तो यह कलुष सर्वव्यापी हो गया है। अगर आप फ़ेसबुक पर बुद्धिजीवियों का कार्य-व्यवहार देखें तो पाएंगे, कि नाहक़ के विवाद छेड़ने और प्रपंच रचने के अलावा इन्होंने कोई रचनात्मक योगदान नहीं दिया है। जितने घंटे बुद्धिजीवी फ़ेसबुक पर बिताता है, उसमें कटौती करके अगर उससे मेहनत करवाई जाए तो शायद मज़दूर को किताब लेकर बैठने का अवसर मिले।
आज गांधीजी की याद आती है। गांधीजी होते तो इन निकम्मे बुद्धिजीवियों को काम पर लगा देते। इनसे चरखा चलवाते, आश्रम में झाडू लगवाते। इनके व्यक्तित्व में थोड़ी दीनता आती, ये विनम्र और तलस्पर्शी बनते और समाज में व्याप्त अश्लील-आर्थिक-विषमता में इसी बहाने थोड़ी कमी आती।
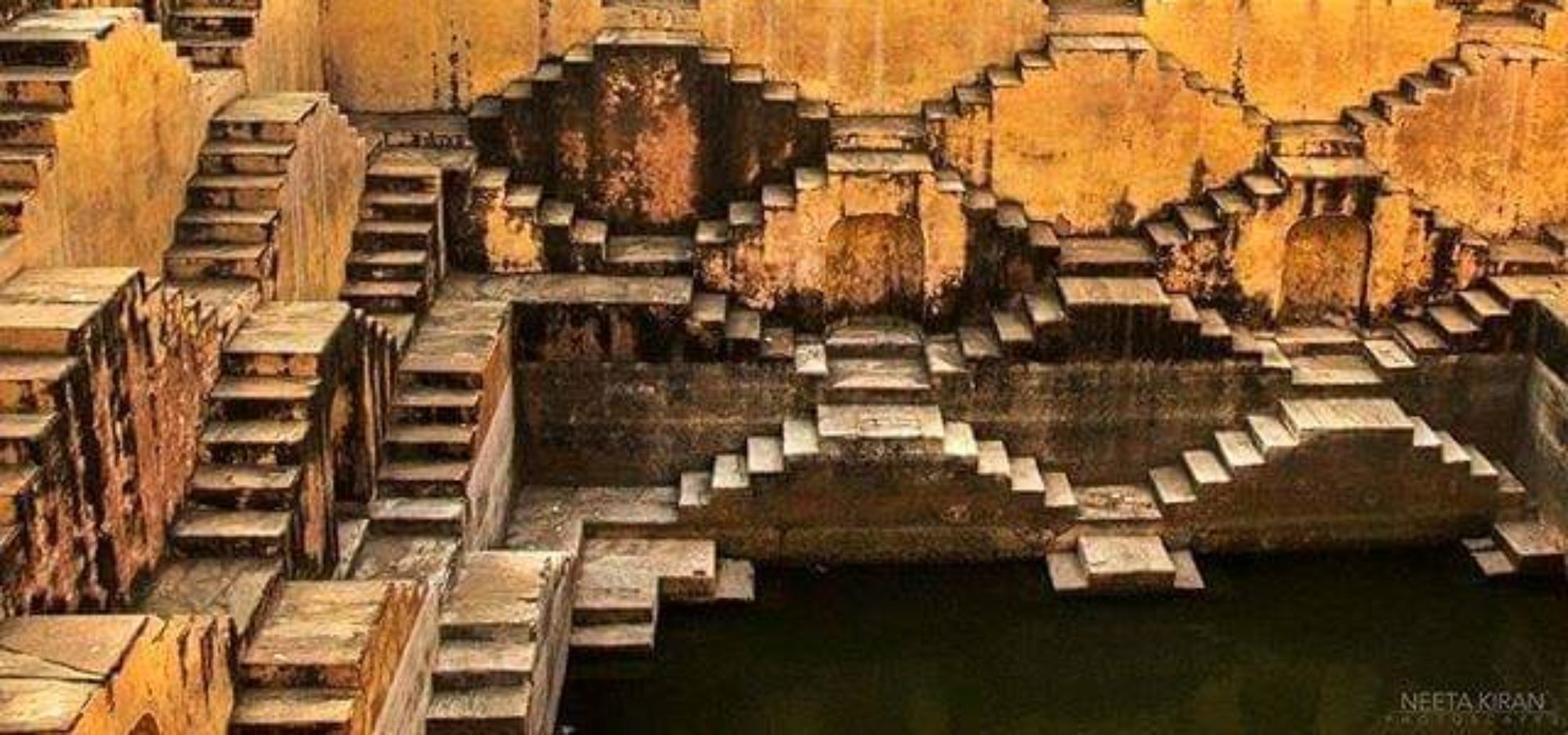

Leave a Reply