नीलमनगर से मेरा अन्न जल उठ चूका था। कई दिनों से अन्तर्मन उदास रह रहा था। काम में मन नहीं लग रहा था। आराम काटने को दौड़ता था, विलास विषाद को और भी गहरा बना रहा था और सौन्दर्य मन को व्यथित करता था। बेचैनी की सीमा नहीं थी। लगातार ऐसा लग रहा था, कि अब यहाँ से छुटकारा पाना चाहिए। वृत्तियों के इस कबन्ध में ज़िन्दगी अधिक गुज़ारनी पड़ी तो आत्मा को सदा के लिए वहीं भटकना पड़ेगा। सुरक्षा और सुविधाओं ने आरामतलबी का आसव पिला-पिला कर पुरुषार्थ को अपाहिज बना दिया था। जीवन की विशुद्धि का आकर्षण होता था, पर अशुद्धियों को लाँघ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। शान्ति निकेतन से लौट कर यह नौकरी स्वीकार की थी, तब मन में निश्चय किया था कि आचार-व्यवहार में कुछ मर्यादा तक ही समझौता करूंगा। इस मर्यादा के बल पर पाँच-सात वर्ष बिता कर कुछ अर्थसंचय कर लूंगा, लेकिन इन स्वनिर्मित मर्यादाओं का भंग तो आरम्भ के चार छह महीनों में ही हो गया; या तो यों कहिए कि करना पड़ा। अतएव बाद के दिनों में धनसंचय तो हुआ, पर अन्तरात्मा का अधिकाधिक कर्जदार होता चला गया। चार वर्ष बाद तो परिस्थिति इतनी असह्य हो उठी, कि उसने मुझे आकुल-व्याकुल कर दिया।
एक तरफ विलास, ऐश्वर्य, ऐशो-इशरत, आराम और अर्थप्राप्ति के पंच महाबलों ने मिल कर जीवन को सत्त्वहीन बनाना शुरू कर दिया, तो दूसरी ओर अन्तरात्मा सात्विकता के दीपक को आदर्शों की मलमल का झौना अन्तराय खड़ा करके बुझने से बचाने का भगीरथ प्रयत्न किये जा रही थी। इस कशमकश की, इस बेचैनी की जानकारी मेरे प्राणों को थी, पर वह उसे पसन्द आने वाली बात नहीं थी। अन्तःकरण इस दोहरी ज़िन्दगी से खिन्न होता था, पर उसके अस्तित्व से मानो जान-बूझ कर बेखबर रहने का प्रयत्न करता था। इस प्रकार जीवन के कुरुक्षेत्र में महाभारत की भेरी बजने लगी। कभी ऐसा लगता, कि जीवन में ऐसा मौक़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिन सुखों के लिए लोग तरसते हैं, जिनके ख़्वाब देखते हैं, वे मुझे अनायास मिल रहे थे; पर विलास की इस मोहिनी से आसक्त प्राण कभी-कभी आत्मा के क्रन्दन से विह्वल भी हो उठता था। इन्द्रियों के सुखों से संचालित मन ऐश्वर्य के वशीभूत होकर कभी तो आत्मा को आश्वासन देता और कभी उसके साथ असहयोग घोषित कर बैठता। दूसरी ओर मन में यह आवाज़ भी प्रबल होती जा रही थी कि भीख माँग कर गुज़ारा करना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं पर जीवन के इस नरक रूपी शिकंजे से छूटना ही चाहिए।
एक बार जब उलझन बहुत बढ़ गयी, तो गांधी जी को दिल्ली तार करके मिलने का समय माँगा। बापू ने तार से ही उत्तर देकर तुरन्त आ जाने की सूचना दी। नीलमनगर बहुत छोटा-सा क़स्बा है। अत्यन्त पिछड़ी हुई सामन्ती रियासत, १९३९ का घटनापूर्ण वर्ष। गांधी जी का तार देख कर उस छोटे से तारघर में मानो भूचाल आ गया। ख़ुफ़िया पुलिस के अफ़सरों को सूचना दी गयी। उन्होंने महाराजा से कहा। तार मुझे मिला, उससे पहले उसकी प्रतिलिपि महाराज को मिल चुकी थी। में दिल्ली जाने के लिए उनकी अनुमति लेने गया, तब उन्होंने अत्यन्त गम्भीर चेहरे से बापू के तार का ज़िक्र किया। मुझे याद दिलाया, कि में उनका निजी सचिव हूँ। अतः वाइसरॉय या दिल्ली सरकार का राजनीतिक विभाग यह मान सकता था, कि ख़ुद महाराजा भी इन गतिविधियों से सम्बन्धित होंगे। तार ऑफ़िस से यह सूचना पॉलिटिकल एजेण्ट को अवश्य मिली होगी और यह समाचार दिल्ली पहुंचने में देर नहीं लगेगी, कि हमारा गांधी जी से गुप्त सम्पर्क है और कोई षड्यन्त्र चल रहा है। उन्हें पहले मालूम होता, तो वे मुझे तार हरगिज़ नहीं करने देते। ऐसे ही चुपचाप चला गया होता, तो यह सारा बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता…इत्यादि।
महाराजा साहब सचमुच ही चिन्तित हो उठे थे। मैंने बहुत समझाया कि तार के शब्द बिल्कुल स्पष्ट है। उनमें कोई गूढ़ संकेत नहीं है। मैंने अपने वैयक्तिक काम के लिए बापू से समय माँगा था। फिर भी मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि तार-ऑफ़िस जाकर ऐसी व्यवस्था कर दूँगा, कि पॉलिटिकल एजेण्ट को कुछ मालूम न हो। महाराजा साहब ने एहतियातन यह राय भी दी कि मैं सतना-इलाहाबाद के बजाय झाँसी होकर दिल्ली जाऊँ, रास्ते में नवगाँव उतर कर पॉलिटिकल एजेण्ट से मिल लूँ और इस बात की ख़ातिरजमा कर लूँ, कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ भी मालूम नहीं हुआ।
मैंने तार बाबू को महल में बुलाया। सौ रुपये का नोट उसकी जेब में डाला और ज़बान बन्द रखने को कहा। इस प्रकार तार की पूरी बात ही दब गयी। दूसरे दिन मैं झाँसी के लिए रवाना हुआ। रास्ते में नवगाँव उतर कर पॉलिटिकल एजेण्ट से मिला। उन्होंने जिस प्रसन्नता और निष्कपटता से बात की, उससे स्पष्ट मालूम हुआ, कि तार के सम्बन्ध में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी। दोपहर का भोजन उनके साथ करके में दिल्ली चल दिया।
बापू उन दिनों पुरानी दिल्ली की हरिजन कॉलोनी में देवदास के यहाँ रहते थे। शाम को प्रार्थना के समय हज़ारों लोगों का समुदाय जुटता था। मैं और भाई यशवन्त पंड्या प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए निकले। प्रार्थना के बाद वहीं बापू से मिल लेंगे, ऐसी योजना थी। उस समय बात न हो सकी, तो बाद का समय निश्चित कर लेंगे, पर हम कुछ देर से पहुँचे। प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। अतः स्वयं सेवकों ने हमारी गाड़ी पहली चौकी पर ही रोक दी। प्रार्थना समाप्त होने तक हमें रुकना पड़ा और बाद में भीड़ की ऐसी रेल आई, कि हम आगे बढ़ ही न सके, परन्तु पंड्या दिल्ली के जानकार थे। उन्होंने स्वयंसेवक के कान में न मालूम क्या मन्त्र कहा, कि हमारी मोटर को अन्दर जाने की इज़ाज़त मिल गयी।
देवदास भाई के घर पहुँचे, तब बापू अपने कमरे में जा चुके थे। मैंने परची भेजी। उन्होंने तुरन्त बुला लिया। पंड्या मोटर में ही बैठे रहे। उस दिन सोमवार था। बापू का मौन था। वात्सल्य भरे स्मित से उन्होंने मेरा स्वागत किया। मेरे हाथों में कोरे काग़ज़ों का एक पुलिन्दा थमा दिया। फिर लिख कर मुझे बताया कि उनका मौन होने के कारण वे मेरी बातों का उत्तर लिख कर देंगे। और मैं भी अपने प्रश्न लिख कर ही पूछूं। कोई चालीस-पैंतालीस मिनट तक यह क्रम चलता रहा। आख़िरी परची में उनका आदेश प्राप्त हुआ- “जीवन के इस दलदल में तुम इतने गहरे उतर गये हो, कि तुरन्त बाहर नहीं निकले, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। फिर तो ज्यों-ज्यों निकलने का प्रयत्न करोगे, त्यों-त्यों गहरे धँसते जाओगे। अतः ईश्वर पर श्रद्धा रख कर यह नौकरी तुरन्त छोड़ दो। यह तुम जैसे लोगों का काम नहीं है।”
मैं चरण-स्पर्श करके उठ खड़ा हुआ। बापू घूमने जाने की तैयारी करने लगे। मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, पर मन हिचकोले खा रहा था। नीलमनगर से निकलते समय जिस मानसिक महाभारत की आगाही हुई थी वह युद्ध अब छिड़ चूका था। एक ओर सुख विलास की वृत्तियाँ किसी वारांगना के से आकर्षण से प्राणों को परवश बना रही थी, दूसरी ओर अन्तरात्मा अनाविल अभीप्सा की बुझती हुई चिनगारियों पर जमी हुई प्रसाद की राख को फूंक मार कर उड़ाने का प्रयत्न कर रही थी।
मेरे पीछे-पीछे बापू भी उतरे। किसी के कन्धे पर एक हाथ था, दूसरे हाथ में लकड़ी। साँझ हो चुकी थी, पर रात का अन्धकार सघन नहीं हुआ था। उस अस्पष्ट प्रकाश में बापू के पुनर्दर्शन हुए। उनके चरणों में मानो अन्तःकरण पर अपने पदचिह्न आगे बढ़ गये, पर मुझे उचित दिशा दिखलाते गये।
दूसरे ही दिन नीलमनगर जाकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और में मुक्त होकर चल निकला।
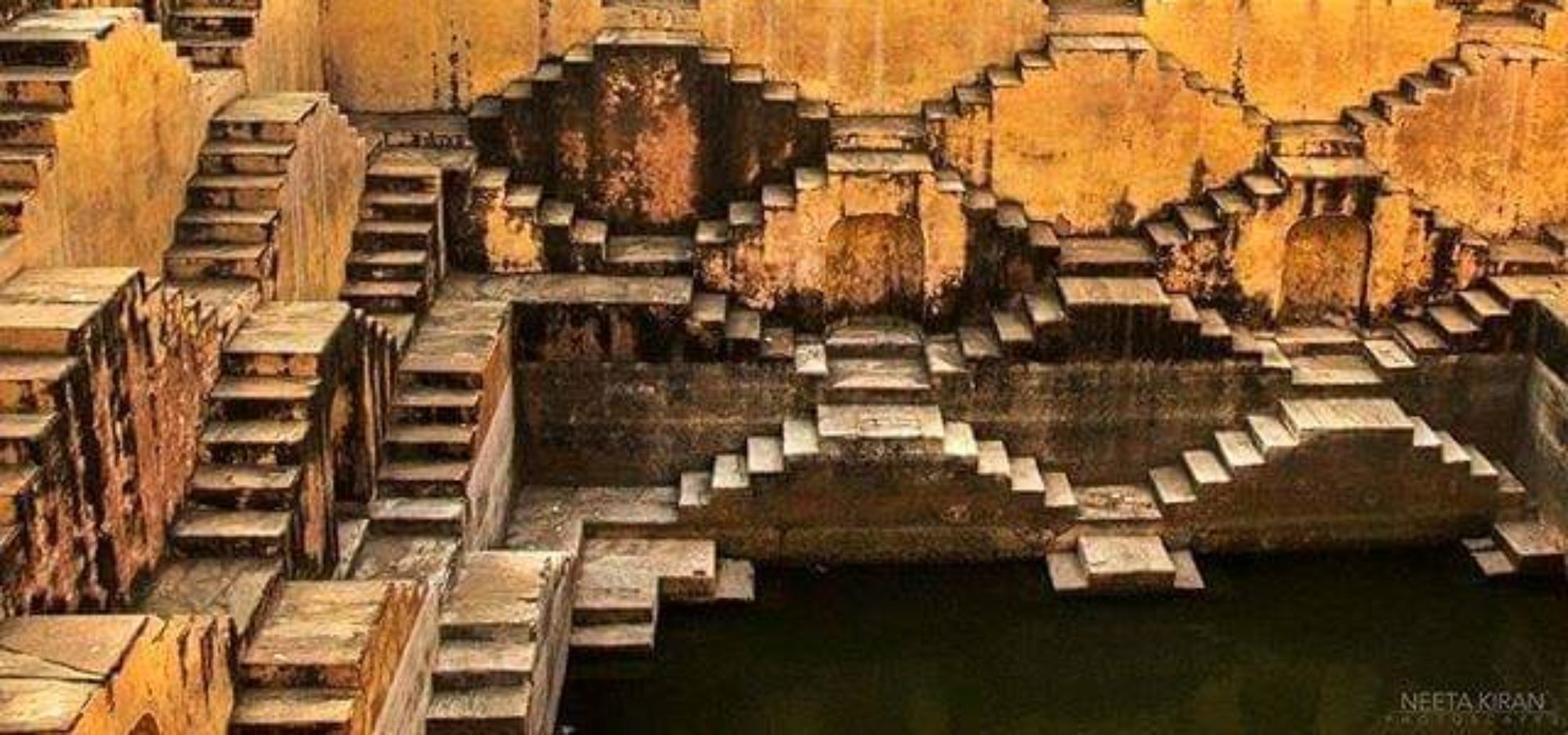

Leave a Reply