गतांक से चालू। भाग १ यहाँ पढ़ें।
(२) शाम ढल चुकी थी। कृष्णपक्ष की रात का अँधेरा उतर आया था। बिजली के खम्भों की रोशनी से वह दबने को तैयार नहीं था। ठण्ड कह रही थी, कि दिल्ली में मेरा राज है, काँग्रेस का नहीं। शायद नौ बजे होंगे। पूरे शाहजहाँ रोड पर मेरे सिवा और कोई दिखायी नहीं दे रहा था। किसी प्रकार की सवारी का नामो निशान नहीं था। बस के लिए कुछ देर रुका पर दिल्ली की बस सर्विस। राम का नाम। में आकाश की ओर देखता हुआ चलने लगा। सप्लाई ऑफ़िस के सामने से गुज़रा। दिन में जहाँ भीड़ का अन्त नहीं रहता है वहाँ इस समय चिड़िया भी नहीं थी। मुझे पूरा शाहजहाँ रोड पार करके कर्ज़न रोड पहुंचना था। सोचा कि इण्डिया गेट पर कुछ चहल-पहल होगी। शायद कोई सवारी भी मिल जाए। रफ़्तार कुछ तेज कर दी।
धोलपुर हाउस के पास एक पेड़ के नीचे अँधेरे में दो आकृतियाँ दिखायी दी। पास जाकर देखा तो एक स्त्री और एक पुरुष। पास ही साइकिल रखी थी। स्त्री की गोद में बच्चा था। पुरुष जवान था। साइकिल में कुछ जोड़- तोड़ कर रहा था। मैंने पास जाकर पूछा, कि “मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या?” जवान ने लाचारी से कहा “बाबूजी, साइकिल पंचर हो गयी है। हम पति-पत्नी मज़दूरी करने गये थे। वहाँ इसको बच्चा हो गया। मैं इसे साइकिल पर बैठा कर घर ले जा रहा था, कि साला पंचर हो गया। भाग्य की बलिहारी है।”
उतने में घोड़े की टाप सुनायी दी। मैंने कहा, “शायद ताँगा आ रहा है। ऐसा कर, में तेरी पत्नी को ताँगे में पहुंचा दूँगा। तू साइकिल लेकर पैदल आ जा।”
“बाबूजी! हम ग़रीब आदमी हैं। ताँगे के पैसे कहाँ से देंगे? पुरानी साइकिल खरीदी थी, तभी का तेरह रुपये का कर्ज बाक़ी है, जो अब तक नहीं चुका।” उसने दीन हताश वाणी में कहा।
मैंने कहा, “घबराओ मत। ताँगे के पैसे मैं दे दूंगा।”
इतने में ताँगा आ गया। ताँगे वाला कोई ग़ज़ल गाकर वातावरण की शून्यता को भरने का प्रयत्न कर रहा था। किराया तय करके उस स्त्री को पीछे बिठाया। में ताँगे वाले के साथ आगे बैठा। ताँगा चल दिया। चार- छह मोड़ लेकर ताँगा एक बंगले के पिछवाड़े में जहाँ अक्सरों के नौकरों की कोठरियों होती है, वहाँ जाकर रुका। मैंने उस स्त्री को उतार कर कहा, “अब कोई हर्ज न हो तो मैं चलूँ।” उस सद्यप्रसूता के हाथ में मैंने पाँच रुपये का नोट देने की कोशिश की। “नहीं बाबूजी, रुपये नहीं लूँगी। आप कुछ देर रुक जाइए। मेरा घर वाला आ जाए, फिर जाइए।” उसने ताँगे वाले से भी रुकने के लिए कहा।
बालक को बरामदे में लिटा कर उसने कोठरी का ताला खोला। अन्दर जाकर लालटेन लायी। दियासलाई ढूँढ़ कर उसे जलाने की कोशिश की, पर लालटेन में तेल नहीं था। फिर ढूंढ़-ढांढ़ कर मोमबत्ती का एक टुकड़ा लायी और उसे जलाया। मैं खड़ा रहा। उसने भीतर से एक मूंज की टूटी-फूटी खाट निकाली। उस पर मैली कुचैली दरी बिछायी और मुझसे बैठने को कहा।
“नहीं, में यहीं ठीक हूँ। यह बंगला किसका है? उस तरफ़ वह सड़क कौन सी है?”
“यह संगत बाबू का बंगला है, बाबूजी और वह बारहखम्भा रोड है।” स्त्री ने जवाब दिया। मोमबत्ती के प्रकाश में वह बालक का मुँह ठीक से देखने की कोशिश कर रही थी।
में चौंक पड़ा। यह तो मेरे आज के मेज़बान अफ़सर के ही बँगले का पिछवाड़ा निकला! मेरा मन चीत्कार कर उठा। आगे के दरवाज़े पर जगमगाते प्रकाश में दम्भ का साम्राज्य। पिछले दरवाज़े पर गहन अन्धकार में दरिद्रनारायण की ऐसी मजबूरी। इसे क्या कहें कुदरत का खेल? या अपना-अपना भाग्य?
इतने में साइकिल लिये वह आदमी आ पहुँचा, गद्गद कण्ठ से उसने मेरा उपकार माना। स्त्री को डाँटा, “अरी कैसी है तू? बाबूजी को बैठाया भी नहीं।” मैंने जवाब दिया, कि “मैंने ही खड़े रहना चाहा था।”
“देखो देखो, इसका मुँह तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है।” स्त्री ने चहक कर कहा। पुरुष ने बच्चे को ध्यान से देखा। “चल झूठी कहीं की। बिल्कुल तुझ पर गया है।” फिर मुझे दिखा कर बोला, “बाबूजी! यह हमारा पहला ही बच्चा है। लड़का है।”
“सुनो, थोड़ा सा गुड़ ले आओ। बाबू जी का मुँह मीठा कराओ। उनके आशीर्वाद से हमारा यह राजा बड़ा हो जाएगा।” स्त्री की आवाज़ से माता के वात्सल्य की माधुरी टपक रही थी। चेहरे पर त्रिभुवन का राज्य मिलने की खुमारी थी।
मैंने वह पाँच का नोट बालक की मुट्ठी में पकड़ा दिया। पुरुष ने आश्चर्य से कहा, “यह क्यों बाबूजी?” मैंने कहा, “भाई! मैं भी तो बच्चे का ताऊ लगता हूँ। मुँह देख कर खाली हाथ कैसे लौटूँ?”
मैं बरामदे की सीढ़ियाँ उतर रहा था। पति-पत्नी दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। अन्धकार में एकता का मूर्तिमन्त स्वरूप दिखायी दे रहे थे। ताँगे में बैठते हुए मैंने गुड़ की डली मुँह में डाल ली। वाणी मूक थी, पर मन प्रफुल्ल था। साँस में ज़िन्दगी की ख़ुशबू बसी हुई थी। सोचा, जब तक पृथ्वी पर अमीरी को चुनौती देने वाली ऐसी ग़रीबी मौजूद है, तब तक डर की कोई बात नहीं। इस भूमि का पुण्य अब तक चुक नहीं गया।
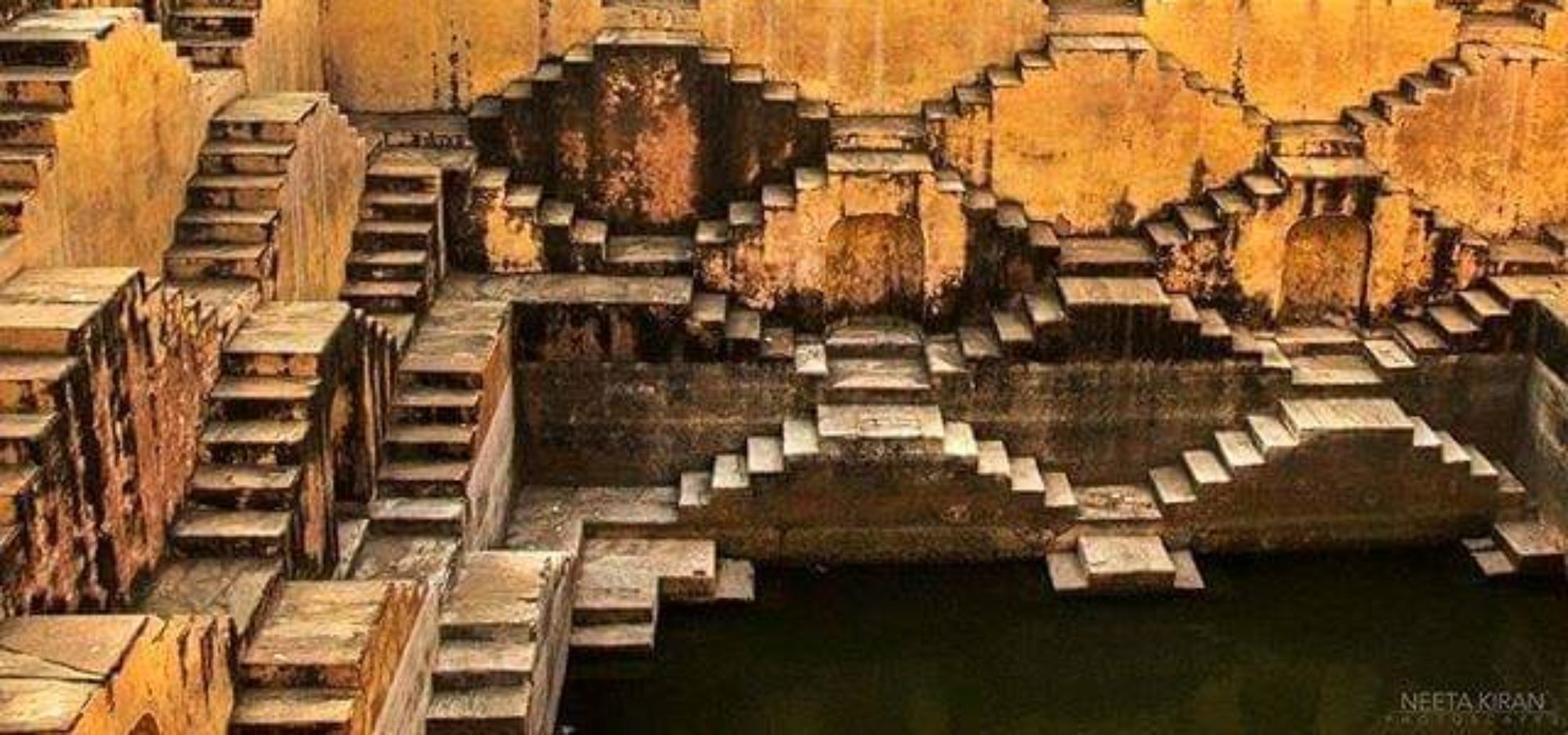

Leave a Reply