राष्ट्रीय नवरचना, ‘विकास’ और ‘प्रगति’ की राह पर चल पड़ने पर सभ्यता और संस्कृति के सवाल खड़े होने न केवल स्वाभाविक है; अगर खड़े न हो तो समझना चाहिए, कि कुछ भारी गड़बड़ है। आजादी का आंदोलन जब उस दौर में पहुंच गया, जहाँ आजादी आने के बाद देश की नवरचना के विषय में गंभीरता से निर्णयात्मक रूप से सोचना जरूरी हो गया, तब यही सवाल गांधीजी ने जवाहरलालजी और कांग्रेस के सामने रखे थे। गांधीजी को पूरी तरह से नकार देते हुए राष्ट्रीय ‘विकास’ और ‘प्रगति’ की जिस दृष्टि को अपना लिया गया, उसी पर पिछले सात दशक से देश का शासन चलता रहा है, ‘विकास’ होता रहा है , ‘प्रगति’ के रास्ते हम चलते रहे हैं।
एक सवाल: हमारे पास अपना कहने लायक क्या है, उनकी क्या अहमियत है, क्या प्रतिष्ठा है?
एक सवाल पूछना चाहिए, कि आप जरा यह तो बतायें, कि आप हमें ले कहाँ जा रहे थे और उस मंजिल के रास्ते पर कौन से मुकाम, कौन से स्टेशन पर आज हम पहुचाये गये हैं और आगे के मुकाम कौन से हैं, कैसे हैं ? इस सवाल के कुछ गहरे मायने हैं, लेकिन इसके पहले एक बेहद सीधे-सादे निर्दोष सवाल की जाँच करना करना जरूरी है. अगर सवाल के जवाब ने सवाल को निरर्थक बता दिया, तो मंजिल का सवाल भी निरर्थक हो जाएगा। यह सवाल खुद से भी है, सबसे है। सवाल यह है: आज हमें कोई पूछे, कि एक राष्ट्र होने की हैसियत से, एक सभ्यता होने की हैसियत से हमारे पास अपना कहने लायक क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे?
हमारा हिन्दुस्तानी, भारतीय होने का विशेष प्रमाण और परिचय क्या है? पहचान देने वाला प्रमाण वह होता है जो अस्मिता – स्वत्व – और अस्तित्व के बीच एकवाक्यता, एकसूत्रता स्थापित करता हो। जिसकी जीवन में – राष्ट्रीय जीवन घडने में मान्यता, प्रतिष्ठा हों; उसका दिनो दिन बढ़ता हुआ मूल्य हो। कहने के लिये तो बहुत कुछ है; राष्ट्र कहलाने लायक सबकुछ है। लेकिन उनकी हैसियत, उनका अधिकार, रूतबा , उनका मूल्य अपने ही लोगों के बीच में, राष्ट्रीय जीवन व्यवहार में; वर्तमान में और भविष्य को घडने में क्या है? क्या हमारे आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृति और शैक्षिक, सामाजिक जीवन को चलाने वाली व्यवस्था उन पर आधारित है? क्या हमारा भौतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, जीवन उनसे प्रेरित और ओतप्रोत है?
हमारे व्यक्तिगत, समूहगत और राष्ट्रीय लक्ष्य को बनाने और पाने के लिए, हमारे प्रयास – पुरूषार्थ में, उनका क्या स्थान है? क्या हमारे विचार, हमारी भाषा और अभिव्यक्ति, हमारी भावना उनसे ओत प्रोत है, उनसे पलती और बढ़ती है? हम जो है और जो बनना चाहते हैं – हमारी असलियत, अस्तित्व और आदर्श में उनकी क्या भूमिका, क्या स्थान है? जो हम हैं और जो स्वाधीकारपूर्वक हमारा है, जो हमें विशेष सभ्यता और एक विशिष्ट संस्कृति होने की पहचान देता है उनमें और हम जो भी बन रहे हैं, ‘विकसित’ होकर, ‘प्रगति’ की राह पर चल कर जो बन रहे हैं, उन दो के बीच क्या कोई निरंतरता है? सामंजस्य है? क्या रिश्ता है उनके बीच?
एक ही सीधे सादे प्रश्न के यह सब विविध आयाम हैं और एक का भी जवाब ‘हाँ’ में नहीं दिया जा सकता – न तार्किक रूप से, न तथ्यात्मक रूप से।
भारत की एक भी चीज, एक भी कृति न तो अपने सही स्थान पर है, न उसकी सत्ता है, न प्रतिष्ठा। इस प्रश्न की पडताल करना जरूरी है। एक उदाहरण के साथ अपने मूल सवाल को खोल कर देख सकते हैं।
न हमारे पास अपनी भाषा है, न अपनी संस्थाएँ, न राजनैतिक, न आर्थिक, न औद्योगिक, न व्यापारिक , न शैक्षिक-सांस्कृतिक- बौद्धिक तंत्र न व्यवस्था। न विचार प्रणाली, न अपना विज्ञान, न टेक्नोलॉजी, न उत्पादन का तरीका न वितरण और न उपभोग की व्यवस्था, न नीति और न तो तरीका। हमारी भाषा(ओं) के तो ये हाल हैं, कि परायी जीवनशैली, जीवन दर्शन और जीवन व्यवस्था का कारोबार और वर्चस्व हमारे बीच जमाने के लिए हमने अपनी भाषा, अपनी वाणी को, अपनी बोली और शब्द रूपों को चित्र – विचित्र, अधकचरे, काम चलाऊ और गांधीजी के शब्दों में ‘नीति की जगह अनीति सीखाने’ वाले विचारों, विचारशैलियों तथा शास्त्रों को ढोने का वाहन मात्र बना दिया है और ऐसा करने को भारतीय भाषाओं की तरफदारी और सेवा भी माना जाता है। इच्छनीय है, कि हमारा काम भारतीय भाषाओं के माध्यम से हो; उन्हें भी यह ऊमदा अवसर मिले, न कि केवल अंग्रेजी को।
अगर जीवन मूल्यों, जीवन दृष्टि, जीवन के आदर्शों की भाषा छूट गई, तो जीवन की अवस्था को, लगातार अनियंत्रित, अप्रत्याशित, अकल्पनीय रूप से बदलती अवस्था को – किस भाषा से समझोगे? उदाहरण अनेक लिए जा सकते हैं। सिद्ध यही होगा, कि भारत के लोगों की प्रतिभा के प्रमाण रूप कोई एक भी चीज अपने अधिकृत स्वाभाविक स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं है। ‘भारत’ में भारत विस्थापित है, या यूँ कहें, कि इंडिया में भारत विस्थापित, दमित है । विस्थापित भारत को प्रतिस्थापित किये बिना विश्व के प्रति अपना दायित्व भारत कैसे निभा सकता है?! खुद को भुला हुआ दूसरों को क्या मार्ग दिखायेगा?
हम उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, जिनकी व्यक्ति से राष्ट्र तक और व्यक्तिगत से राष्ट्रीय जीवन व्यवस्था बनाने में प्राथमिक भूमिका होती है। कितना ही प्रयास करें, एक चीज भारतीय नहीं मिलेगी, जो अपने मौलिक स्थान पर और अवस्था में हो, अपने अधिकार और अपनी स्वायत्त सत्ता के साथ हो और जिसका उपयोग, जिसकी सेवा और परवरिश उसके अपने संपूर्ण दायरों में, सांगोपांग रूप से होती हो।
अधिक से अधिक अगर कोई चीज मिल भी गई, तो उसका स्थान और मान्यता या तो प्रयोगात्मक; सहायक के रूप में; प्रसाधन रूप; कुतूहल के रूप; या आंशिक लाभ या लोभ की पूर्ति के लिए होगा; या कभी-कभी अपनी पुरानी ‘धरोहर’ के बीज या नमूने को जिंदा रखने की जिम्मेदारी के अहसास के रूप में होगा; या नुमाईश के लिए। उदाहरणार्थ, पारंपरिक पद्धति की खेती, गाय का दूध, या पंचायत व्यवस्था, योग, कुछ औषधि-पद्धतियां और ‘नुस्खे’, संगीत एवं नृत्यकला, खान-पान और पहनावा इत्यादि। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक कर्मकाण्डों और लोकाचारों का वहन करके हम परंपरा के वहन का दंभ भरते हैं – यह समझे बिना – कि ये केवल उनकी आंतरिक अर्थहीनता के संकेत मात्र बन कर रह गये है।
कुछ भी हमारे जीवन में, हम में, मौलिक है ही नहीं, जो है – वह एक नकली पहचान है, जिसे हमने ओढ़ रखा है। हम यह भी देखेंगे, कि नकली पहचान को ओढ़े रखना स्वार्थ का तकाजा भी हो गया है। इसे हम स्वीकार करेंगे तो ही हम इससे मुक्त हो सकते हैं।
अंग्रेजी शिक्षा ने हमें सिखा दिया, कि प्रगतिशील होने का अर्थ आधुनिकतावादी होना है और आधुनिकतावादी होने का अर्थ पश्चिम के नेतृत्व और नियंत्रण वाले औद्योगिक और टेक्नोलोजिकल समाज बनना है और ऐसा आधुनिक बनने के लिए जो कुछ अपना था और है, अपनी परंपरा के पिछडे़पन की निशानी समझकर उनसे छूटकारा पाना ही उन्नत और विकसित होना है। हमने बिना जाँच – पड़ताल के, बिना किसी प्रकार के शास्त्रार्थ या उनके और भारतीय के बीच तुलनात्मक अध्ययन के, किसी विवाद या संवाद किए बिना ही ‘आधुनिकता’ की श्रेष्ठता, सार्वभौमिकता, सत्ता स्वीकार कर ली।
केवल एक गांधीजी थे जिन्होंने तल स्पर्शी शास्त्रार्थ, संवाद, विरोध और जबरदस्त संघर्ष किया, लेकिन उनके इस पक्ष को उन्हीं के उन अनुयायियों ने देश निकाला दे दिया, जो आजादी आते ही सत्ता में आये। केवल विजेता होने के यूरोपीय प्रजा के सामर्थ्य से प्रभावित हमारे इस अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग ने शिष्यवत होकर उनके सीखाये सारे पाठ सीख लिये, आधुनिकता – पाश्चात्य सभ्यता को सांगोपांग ऐसा स्वीकार कर लिया, मानो ये मानवमात्र की नियति हो। मानो भारत की कोई पहचान, कोई सभ्यता ही न हो। सभ्यता की अपनी स्वाधीन दृष्टि होती है, नियति होती है। दूसरों से लेन – देन होनी ही चाहिए, लेकिन ‘लेन’ ही ‘लेन’ नहीं। हमारे तो इन हवाओं में पैर ही ऊखड गए।
कभी हमने सोचा कि अंग्रेजी साम्राज्य से जीतने का सामर्थ्य हममे कहाँ से आया? लड़ते तो पहले भी रहे, लेकिन संघर्ष पूरी प्रजा का तब बना और मनोबल की अद्भूत शक्ति तब आई, जब गांधीजी ने राजनैतिक आजादी के आंदोलन को आत्म – जागृति का, ‘स्व’ की पहचान का, भारत की स्व – चेतना अर्थात् स्वराज – चेतना की जागृति का आंदोलन बना दिया। हर देशवासी को, गरीब से गरीब व्यक्ति को भरोसा बन गया, कि यह राज्य, यह समाज, यह व्यवस्थातंत्र मेरे हैं; जिसमें उसे अपनी छवि दिखे। उसके संचित ज्ञान, हुनर, जीवनदृष्टि और उसे चलाने के साधन-संस्थाओं-शात्रों की अहमियत हो। उनमें आये दोष को सुधारा जाए, न कि उन्हें निकम्मा बना दिया जाए। वहाँ से भारत खड़ा हो – अपनी धरोहर अपनी अस्मिता की घर – वापसी के लिए। इसके अर्थ को समझने के लिए आगे चलकर हम ऐसा उदाहरण भी देखेंगे। इस दृष्टि से सोचना इस लिए जरूरी है कि हम समझ सकें, कि भारत का सामर्थ्य किसमें है और किस प्रकार वह अपनी अस्मिता पाकर विश्व के लिए मार्गदर्शक बन सकता है।
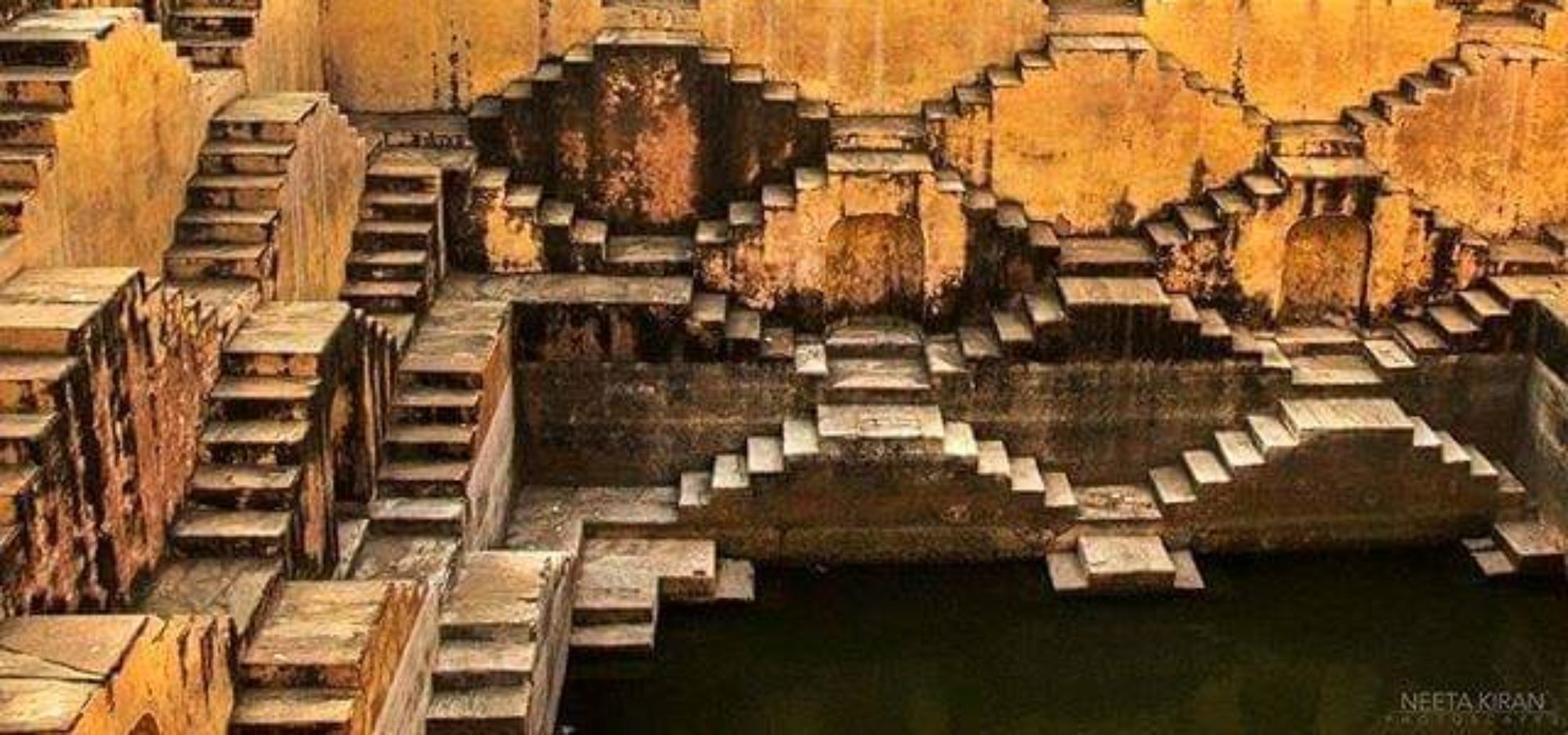

Leave a Reply