धर्मपाल जी का समग्र लेखन छपने के बाद उसमें से प्रत्येक अध्येता अपनी रुचियों के अनुसार गुज़रता है। मैं भी कुछ हिस्सों से गुज़रा। स्वभावतः भारत की वे छवियाँ टूट गयीं, जो बरसों से मन में आधुनिक शिक्षा के कारण बनी हुई थीं, लेकिन इन छवियों के टूटने के कारण विशिष्ट थे।
‘हमारा पहले का भारत बहुत शानदार था’ – ऐसे वाक्य बचपन से सुनता आया था। फ़िल्मी गानों में – संतों के प्रवचनों में और कुछ राजनैतिक रुझानों वाले नेताओं के मुख से भी, परन्तु उन वाक्यों के पीछे जब कुरेदता, कि वे सब उस ‘महानता’ का आधार कहाँ से पाते हैं, तो सन्दर्भ हज़ारों बरस पहले के पौराणिक-ऐतिहासिक स्रोतों से आते। मस्लन प्राचीन भारत के वायुयान अथवा महरौली का लौह स्तम्भ या विशालकाय मंदिर किले आदि। समाज व्यवस्था का प्रश्न आने पर गांधीजी द्वारा कहे गए ‘रामराज्य’ की बात चलती, कि पहले तो सब रामराज्य था और सभी जगह न्याय होता था।
आयु बढ़ने के साथ – साथ वैकल्पिक तस्वीरें भी उभरने लगीं। मस्लन निर्गुण भक्ति काव्य में जातिभेद की तीव्र आलोचना ने थोड़ा विचलित किया। विचलित इसलिए किया कि आलोचना करने वाले बाहरी लोग नहीं थे। वे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक भी नहीं थे, वे मध्य-पूर्व से आये मुस्लिम आक्रमणकारी भी नहीं थे, वे हमारे बीच से ही आये संत थे। दलित चिंतन के उभार के साथ आयी आत्मकथाओं को पढ़ने से कुछ नए आयाम खुले। ओमप्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा – जूठन अथवा दया पवार की अछूत या फ़िर प्रोफेसर तुलसीराम की लिखी मुर्दहिया।
ये सब आत्मकथाएँ थीं। नितांत निजी अनुभव। हम किताब के संदर्भों को तो शायद नज़रअंदाज़ कर भी दें, लेकिन आत्मकथा में दर्ज अनुभव को कैसे उपेक्षित करें। अतः इन सबसे एक मिली जुली उलझी तस्वीर बनी, चूँकि भारत को लेकर ये सब अलग अलग ‘सत्य’ थे। ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि इनमें से कोई एक ‘असत्य’ था, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि ये सभी सत्य एक दूसरे के साथ सहज बैठ नहीं सकते थे।
ऐसे में धर्मपाल जी का आकर्षण उनकी निष्पत्तियाँ – निष्कर्षों के कारण पैदा नहीं हुआ। ब्रिटिश – पूर्व भारतीय समाज को लेकर एक प्रशंसा तथा गौरव का भाव हमारी आम बोलचाल में रहा ही है।
गांधीजी से लेकर अन्यान्य दूसरे विचारक प्राचीन भारत के गौरव पर सर्वदा बल देते रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस ब्रिटिश-पूर्व समाज की स्थिति पर कभी कोई ठोस सिलसिलेवार शोध प्रस्तुत नहीं किया था; यूँ कहें, कि बातें ही बातें थीं पर अंतर्वस्तु गायब रही। थोड़ा सुधारकर सुन्दर कोमल शब्दों में कहना चाहें, तो यूँ कह लें, कि सारे निष्कर्ष ‘intuitive’ थे। इन ‘intutitve’ निष्कर्षों के साथ दिक्कत ये होती है, कि आप या तो इन्हें मान सकते हैं या फ़िर निरस्त कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ कोई आलोचनात्मक रिश्ता कायम नहीं कर सकते। ह्रदय झंकृत हुआ तो मान लिया – नहीं हुआ तो निरस्त कर दिया। ‘ह्रदय की आवाज़’ पर आधारित ये सब बातें ‘poetic truth’ अर्थात ‘काव्य-सत्य’ जैसी थीं।
ऐसे में धर्मपाल जी ने जो दस्तावेज़ों का अध्ययन करके ठोस सामग्री प्रस्तुत की, वो ‘आधार’ बिल्कुल नूतन था। दूसरी तरह से कहें, तो उन्होंने ब्रिटिश-पूर्व भारत को लेकर अध्ययन की पद्धति बदल डाली। अतः धर्मपाल जी मौलिकता निष्कर्ष की बनिस्बत ‘पद्धति’ यानी ‘methodology’ के अनुसंधान में अधिक है। पिछले दिनों उनकी रचना ‘भारतीय चित्त, मानस और काल’ पर चर्चाओं को सुनते हुए ये बात अधिक स्पष्ट हुई। ‘भारतीय चित्त, मानस और काल’ की कितनी ही अन्तर्दृष्टियाँ हमारे यहाँ के आधुनिक संतों, विचारकों तथा अध्येताओं के यहाँ भी आयी हैं, परन्तु मेरी रूचि धर्मपाल के कहे में अधिक इसलिए है, कि उनके यहाँ से जो अंतर्दृष्टि आ रही है वह बहुत परिश्रम से तैयार ठोस भूमि से आ रही है।
‘मुझे ऐसा लगता है’ – से आरम्भ होने वाली बातचीतों से भरे इस संसार में मुझे उन व्यक्तियों की तलाश रही, जो लम्बे अध्ययन-मनन के बाद ये कह पाएँ, कि ‘मैंने ऐसा पाया है’! जब हम इस समाज को समझने निकलते हैं तो – ‘मुझे ऐसा या वैसा लगता है’ – महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकता। समाज साझा है – भाषा साझी है – संस्कृति साझी है। अतः एक व्यक्ति को कैसा लगता है – ये अध्ययन का आधार केवल निजी रहस्यात्मक अनुभूति तक ही रह सकता है। रात्रि को आने वाले स्वप्न निजी होते हैं। प्रेमिका के साथ उद्यान के पेड़ों के पीछे की गयी मधुर बातें निजी होती हैं। लम्बे समय के बाद मिले मित्र के साथ साझे किये गए सुख दुःख भी निजी ही होते हैं, परन्तु सामाजिक सत्य निजी उपक्रम नहीं हो सकता।
धर्मपाल का यही अवदान है, कि उन्होंने भारतीय सामाजिक सत्य को हवाई वक्तव्यों से बाहर निकालकर एक ठोस अनुसंधान की भूमि पर प्रतिष्ठित किया। अतः उनका ‘method’ हम सबके लिए एक नया प्रस्थान था। ये दूसरी बात है, कि धर्मपाल के चिन्तन परिकर में कुछेक अपवादों को छोड़कर उनके ‘method’ की बनिस्बत उनकी ‘निष्पत्तियाँ’ ही अधिक प्रचलित प्रतीत होती हैं, हालाँकि उसका सीधा कारण यही है, कि भारतीय लोकमानस ‘वाचिक-मौखिक’ परम्परा की ओर उन्मुख रहा है और उसे ‘textual research’ में सीधे रस अनुभव नहीं होता। अलबत्ता भारतीय पांडित्य परम्परा में हज़ारों बरस तक ‘textual research’ की भी एक स्वतंत्र धारा रही है।
धर्मपाल अथवा हममें से कोई दूसरे व्यक्ति भी क्यों न हों, हमारी एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि होती है। उस पृष्ठभूमि से ये तय होता है, कि मैं किस दिशा में चलूंगा। मेरे मित्र, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे साथ संवाद करने वाले अध्येता – इन सबका एक प्रभाव मुझ पर पड़ता है। उन प्रभावों की सूची कभी पूरी तरह तो नहीं बनाई जा सकती, चूँकि वे सभी प्रभाव दर्ज करना लगभग नामुमकिन सी बात है। वे प्रभाव केवल प्रत्यक्ष ही नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष भी होते हैं, जो अवचेतन में चले जाते होंगे।
फ़िर भी धर्मपाल के संबंध में एक धुंधली झलक मुझे ‘धर्मपाल कुछ यादें’ से मिली। मैं कभी धर्मपाल जी से मिला नहीं। अतः उनके मित्रों-परिचितों के संस्मरण बहुत काम के प्रतीत हुए। पूरे विस्तार के लिए तो उस पुस्तक को ही देखना चाहिए, लेकिन मेरे मन में जो मोटा मोटी बातें उभरीं, वे अलग अलग तरह ही हैं। किताब खोलते ही पहला आलेख नवज्योति सिंह का है। इस आलेख के अंत में एक बात कही गयी, जो सम्भवतः धर्मपाल जी के चिंतन-circle से बात के दौरान उपजे द्वंद्वों की भी व्याख्या है। वह ये कि ‘Indian Analytical Tradition’ की ओर उनका स्वाभाविक झुकाव नहीं रहा। [मूल अंग्रेजी – He was not temperamentally inclined towards it]
अब ये एक विचित्र बात है। इसलिए भी, कि धर्मपाल जिस तरह से ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दस्तावेज़ों का अध्ययन कर रहे थे – उस तरह से उनके समय में और कोई नहीं कर रहा था। सिंह साहिब ये भी संकेत करते हैं, कि धर्मपाल ने पाश्चात्य ‘analytical enterprise’ का भारतीय समाज की तस्वीर को बदलकर देखने के लिए बखूबी प्रयोग किया। अब मेरे सामने गुत्थी ये है, कि जब धर्मपाल पश्चिम की analytic [विश्लेषणात्मक] प्रक्रियाओं का सहजता से प्रयोग कर रहे थे, तो स्वयं भारत की analytic परम्पराओं का उन्होंने विस्तारपूर्वक उल्लेख कैसे नहीं किया।
इसे समझने के लिए पुनः ‘भारतीय चित्त, मानस और काल’ की ओर लौटता हूँ। वे भारतीय पुराणों, महाभारत, रामायण आदि में गहनता से उतरते हैं, परन्तु भारत में न्याय-वैशेषिक और तर्कशास्त्र की जो धारा रही है, उसको लेकर धर्मपाल क्या सोचते थे! बौद्धों और नैयायिकों में सदियों तक गंभीर शास्त्रार्थ हुए। स्वयं मीमांसकों और वेदान्तियों में भी यह चला। जब हम वैशेषिक की भाषा देखते हैं, ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य-टीकाएँ देखते हैं, या फ़िर जैन न्याय के ग्रंथों को उलटते पुलटते हैं अथवा बौद्ध दार्शनिकों के कार्य को सामने पाते हैं, तो एक गंभीर तार्किक धारा हमारे सामने प्रकट होती है।
पंडित बलदेव उपाध्याय जी की ‘काशी की पांडित्य परम्परा’ या फ़िर गोपीनाथ कविराज की ‘काशी की सारस्वत साधना’ भी उसी ओर संकेत करती है। हमारे समय के जनार्दन गनेरी, बिमल कृष्ण मतिलाल और उससे भी पहले कृष्णचन्द्र भट्टाचार्य सरीखे दार्शनिकों ने उस भारतीय तर्क-दर्शन-परम्परा पर बहुत विस्तार से काम किया है। अतः मन में ये सवाल उठता है, कि धर्मपाल जब भारतीय चित्त की बात करते हैं, तो उसमें ये सब हिस्सा कहाँ होता है !
धर्मपाल उसे पर्याप्त स्थान क्यों नहीं देते। इसका एक जवाब तो ये हो सकता है, कि खुद भारतीय जनमानस ने भी अपनी ही तर्क दर्शन परम्परा को पर्याप्त स्थान कभी नहीं दिया। पंडितों के दार्शनिक मसले आमजन के दैनंदिन विमर्श का हिस्सा कभी नहीं रहे। बल्कि इसके उलट लोक में प्रचलित मुहावरे ‘पांडित्य’ पर व्यंग्य ही कसते थे। उच्चकोटि के संतों ने भी ‘पोथीज्ञान’ को हेय माना, वो बहुत हद तक उचित भी था, चूँकि आत्मा के अनुसंधान के विषय में तर्क-पद्धति पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता था। इस पूरे मसले का हालाँकि इतना ही पहलू नहीं है। धर्मपाल के चिंतन में ये ‘omission’ सांयोगिक नहीं है। इसके पीछे स्वयं भारतीय जीवन में आये बदलाव भी हैं।
यास्क के वक़्त में हज़ारों बरस पहले तर्क को ऋषि कहा गया। निरुक्त के अनुसार जब मनुष्यों द्वारा पूछा गया, कि ऋषि-परम्परा के बाद हमारा मार्गदर्शक कौन होगा, तो उत्तर आया, कि तर्क ही ऋषि होगा। लेकिन भारत में ये स्थिति बहुत लम्बे समय तक नहीं रही। महाभारतकाल के आते आते सामाजिक स्थिति डावाँडोल हो गयी। तब ग्रंथों ने तर्क को ‘अप्रतिष्ठित’ कह दिया, यानी तर्क के आधार पर कोई एक कुछ कहता है और कोई दूसरा कुछ कहता है। अतः हम तर्क को आधार न मानकर महापुरुषों के आचरण को आधार मानेंगे। अतः मेरे अपने विचार से नवज्योति जी धर्मपाल के संबंध में जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, वो दरअसल भारतीय परम्परा के भीतर की एक अनसुलझी गुत्थी है।
हम तर्क को ठीक से आगे ले जाने की बजाय उसपर से यकीन खो बैठे। ऐसा नहीं है, कि वो सब पंडितों में लुप्त हो गया। वो पंडितों में तो जारी रहा लेकिन जनमानस से हट गया। शायद यही इस बात का भी संकेत हो कि जब ब्रिटिश शासन प्रणाली के साथ वैज्ञानिक चिंतन पद्धति आयी, तो हमारा नया नवेला पढ़ा-लिखा वर्ग एकदम सम्मोहित हो गया, चूँकि उनका अभ्यास पौराणिक वाचिक धारा का था। नए बदलते आधुनिक औद्योगिक युग में वो भाषा चल नहीं सकती थी। इसलिए उन्नीसवीं शताब्दी के भारतीय विचारक अंग्रेजी विज्ञान से नहीं, बल्कि ‘पश्चिमी वैज्ञानिक चिंतन के method’ से मोहाविष्ट हो गए। मेरे अपने विचार से पश्चिम का विज्ञान उतना हमें आकृष्ट नहीं करता, जितना उनकी ‘विज्ञान की चिंतन पद्धति’ !
इसका बीज अपनी ही तर्क परम्परा से हमारा टूट गया नाता रहा होगा। धर्मपाल के लेखन में ये सारी उथल-पुथल बीज रूप से ढँकी हुई हैं। नवज्योति सिंह के शब्दों में धर्मपाल जिस ‘Substantial India’ की संकल्पना की ओर मुड़े, वो मुझे संयोग नहीं लगता। उनकी चिंतन परम्परा के उत्तराधिकारियों में भी उसी ‘Substantial India’ की खोज जारी है। यही वजह है कि खुद धर्मपाल के अनुसंधान के निष्कर्ष उन सबमें प्रचलित हैं – उसकी अनुसंधान पद्धति उतनी नहीं। इसके साथ साथ श्रीगुरुजी के चिंतन से नए प्रस्थान उभरे, जिनमें महत्त्वपूर्ण सत्र भी थे और कुछ नए प्रश्न भी!
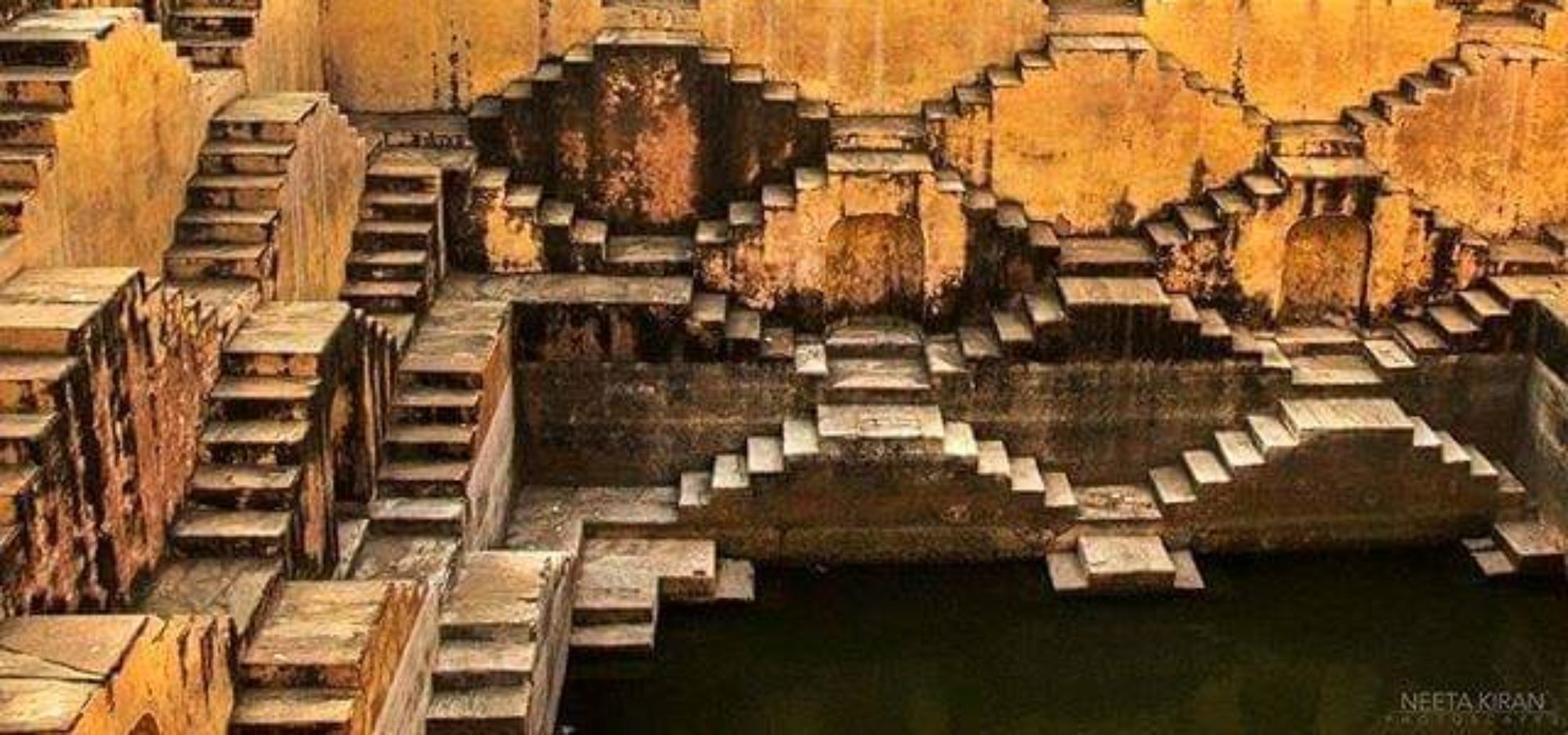


Leave a Reply