समाज की पारंपरिक कल्पना
हैना आरेंडट के मुताबिक़ ग्रीक सभ्यता में जो पोलिस (सार्वजनिक संवाद स्थली) की कल्पना थी, वह आधुनिक सोसाइटी से बिलकुल ही भिन्न थी। उस सभ्यता में, जहाँ घर – परिवार (household) आहार की सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता करते थे, वहीं पोलिस की चिंता उन मुद्दों पर थी जो जीवन की क्षितिज पर हैं – जैसे मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, अमरत्व की संभावना किस रूप में हैं, जन्म क्या होता है इत्यादि। पोलिस की चिंता जीवन – यापन के मुद्दों पर नहीं थी, या फिर उन मुद्दों तक सीमित नहीं थी। आरेंडट कहती हैं, आधुनिकता की शुरुआत पब्लिक और प्राइवेट के बीच जो महत्त्वपूर्ण अंतर था, उसके धूमिल होने से होती है। आधुनिकता में पोलिस / पोलिटिकल और परिवार / प्राइवेट के बीच राक्षस रूपी सोशियल खड़ा हो गया, जिसने धीरे – धीरे पब्लिक और प्राइवेट दोनों का भक्षण कर लिया।
ऐसा ही कुछ भारतीय सभ्यता में भी देखने को मिलता है। शायद समाज शब्द का प्रयोग पहली बार भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हुआ; नाट्य को देखने जो दर्शक इकट्ठा हुए उन्हें सामाजिक कहा गया है।5
नाट्य को सभी कलाओं की जननी समझा जाता है और कलाओं का प्रयोजन आम जन – मानस में धर्म के प्रति सद् इच्छा को जागृत करने का रहा है। यह बात नाट्यशास्त्र की भूमिका में एक कथा के द्वारा स्पष्ट की गई है – कृत युग (सत युग) से त्रेता युग का बदलाव मानव व्यवहार में आयी एक त्रुटि से समझा गया। मानव जन धर्म – अधर्म की चिंता छोड़ सुख-दुःख की चिंता में लग गए हैं। इस त्रुटि के निवारण हेतु, समस्त देवता गण ब्रह्माजी से एक पंचम – वेद की रचना करने को कहते हैं जो एक तरफ़ तो चारों वेदों का सार हो और दूसरी तरफ़ “सर्ववार्णिक” (सभी वर्णों के लिए) हो। ऐसे में नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति होती है, जिसे पंचम वेद भी कहा गया है। ब्रह्माजी इस “सर्ववार्णिक पंचम वेद” को भरत मुनि को सौंपते हैं और साथ ही उन्हें 100 पुत्र और 1 पुत्री देते हैं, जो आगे चल कर नट कहलाये।
यहाँ दो महत्त्वपूर्ण बातें ध्यान देने की हैं। पहली, नाट्य (कला) का प्रयोजन मानव जन का ध्यान सुख – दुःख की चिंता से ऊपर उठा कर धर्म – अधर्म की चिंता में स्थापित करना और दूसरी, कला को सभी के लिए उपलब्ध होने का प्रावधान।
जो दर्शकगण नाट्य को देखने के लिए और नाट्य में उठाए गए धर्म – संकट पर विचार – विमर्श के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनको नाट्यशास्त्र में सामाजिक कहा गया है। दूसरे शब्दों में, जब मानव धर्म – अधर्म पर विचार – विमर्श करने के लिए एक दूसरे के साथ आता है तब समाज का निर्माण होता है। इसके बाद, जब मानव जन साथ मिलकर धर्म की स्थापना के अर्थ में कार्य करते हैं, तब समाजिकता आगे बढ़ती है। बाकी सब कुछ – आहार की सुरक्षा, साधनों की संपन्नता, शादी – ब्याह (संतान उत्पत्ति) और रिश्तेदारी के मुद्दे इत्यादि सभी धर्म स्थापना की मौलिक चिंता के संदर्भ में ही समझे गए हैं। यह हमारी समाज की सभ्यतागत कल्पना है।
समाज और पोलिस की सभ्यतागत कल्पना आधुनिक यूरोप की उस कल्पना से बिलकुल भिन्न है, जहाँ यह माना गया कि जब मानव ख़ानाबदोश (hunter-gatherer) स्थिति से ऊपर उठ कृषि करने लगा तब उसे एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की आवश्यकता लगी। जमावड़े की ऐसी कल्पना पशुओं के जमावड़े से प्रेरित लगती है। इस कल्पना में आहार की सुरक्षा को मानव की मूल चिंता माना गया है।
एक ओर तो साथ आने की कल्पना में आहार की चिंता है, तो दूसरी ओर धर्म – स्थापना की चिंता है। यह तो स्पष्ट है कि ये दोनों कल्पनाएँ भिन्न स्रोतों से उपजी हैं। अगर हम अपने समाज को देखना चाहते हैं, तो इस भेद को समझना उपयोगी रहेगा। सोसाइटी की समझ से न पोलिस समझ आता है और न समाज।
साधारणिकरण और सामाजिकता
सामाजिक होने के लिए यह ज़रूरी है कि धर्म – अधर्म की चिंता में हम विलीन हों। प्रदर्शित नाट्य में जो धर्म – संकट प्रस्तुत किए गए हों, उनकी चिंता में हम विलीन हों। उन धर्म-संकटों का जो निवारण नाट्य में सुझाया गया है, उनमें हम विलीन हों। ऐसा गहरा और लम्बा विलीन होना आसान नहीं हैं। दैनिक जीवन में अनेकों व्यवधान मौजूद रहते हैं, जो हमें धर्म – अधर्म के मुद्दे पर विलीन रहने से रोकते हैं। जैसे, अगर घर में खाने पीने की कमी हो, या घर की छत टपक रही हो, तब ऐसे में सीता को लेकर राम के धर्म संकट पर या लक्ष्मण रेखा के विषय में चिंता करना संभव नहीं होगा।
नाट्य सफल तभी होता है जब दर्शक धर्म – अधर्म की चिंता में विलीन हो सके। इसके लिए यह ज़रूरी है, कि आम जन – मानस का जीवन – यापन सहज हो और भविष्य के प्रति उसमें निश्चिन्तता का भाव हो। जटिल जीवन शैली उसे जीवन – यापन में ही उलझा कर रखेगी। दो वक़्त की रोटी कमाने में या फिर घर को म्यूजियम की तरह सजाने में ही पूरा जीवन निकल जाए तो नाट्य के लिए समय ही नहीं बचेगा। वहीं दूसरी ओर अगर भविष्य की चिंता लगातार सताएगी तो धर्म – अधर्म की चिंता कहाँ से हो पाएगी। कोई भी व्यक्ति केवल और केवल तभी नाट्य में रुचि लेगा और उठाए गए धर्म – संकट पर विचार – विमर्श करने को तैयार होगा, जब उसका सहज जीवन हो और भविष्य के प्रति आश्वस्त हो।
ऐसी स्थिति को नाट्यशास्त्र में साधारणिकरण की स्थिति कहा गया है। यह स्थिति नाट्य में विलीन होने की स्थिति का कारण बनती है और इस स्थिति को सामाजिक होने के लिए अनिवार्य माना गया है। ऐसा माना गया है कि साधारणिकरण की स्थिति में दर्शक और कलाकार के बीच सह-हृदय होता है। मनमोहन घोष ने साधारणिकरण को immersion शब्द दिया है।
नवज्योति सिंह साधारणिकरण की स्थिति को मानव की नग्नता से जोड़ते थे – bare human being। एक ऐसी स्थिति जब व्यक्ति अपने सभी विशेषण त्याग दे (थोड़े समय के लिए); जैसे पुरुष – महिला का विशेषण, राजा – रंक का विशेषण, कुम्हार – किसान – लोहार – बढ़ई – चर्मकार – पंडित जैसे विशेषण इत्यादि इत्यादि। जो भी दर्शक की गद्दी पर बैठा है वह मानसिक सामाजिक रूप से नग्न अवस्था में होना चाहिए। ऐसा होने पर ही वह धर्म – अधर्म पर शुद्ध रूप से चिंतन करने की स्थिति में हो सकता है और ऐसे दर्शकों के जमावड़े को समाज कह सकते हैं।
केवल कथावाचक (कलाकार) ही है, जो अपने विशेषण नहीं त्यागता। वह नाट्य में immerse नहीं होता। कथावाचक हर क्षण कथा और वास्तविकता में भेद देख रहा होता है। कथावाचक की ज़िम्मेदारी है, पहले दर्शक को नाट्य में विलीन कर देना और फिर समाप्ति पर दर्शक को वापिस उसकी वास्तविकता में ले आना।
धर्म – अधर्म पर गहरी चिंता के लिए समाज में सामाजिक मानसिक नग्न अवस्था (साधारण) होना ज़रूरी है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए जो कार्य होना है, उसके लिए तो सभी को वापिस अपने अपने विशेषण ओढ़ने होंगे; कुम्हार को पुनः कुम्हार होना होगा, लोहार को लोहार, राजा को राजा इत्यादि। इसलिए मेरे विचार से समाज का एक पैर “नाट्य लोक” में होता है (जिसे परलोक कह सकते हैं)6 और दूसरा पैर इह – लोक (कर्म लोक)7 में होता है। परलोक चिंतन का लोक है। यहाँ मानव का दूसरा जन्म होता है – सामाजिक मानव8 और कर्म – लोक कर्म करने का लोक है। समाज दोनों ही लोक में वास करता है।
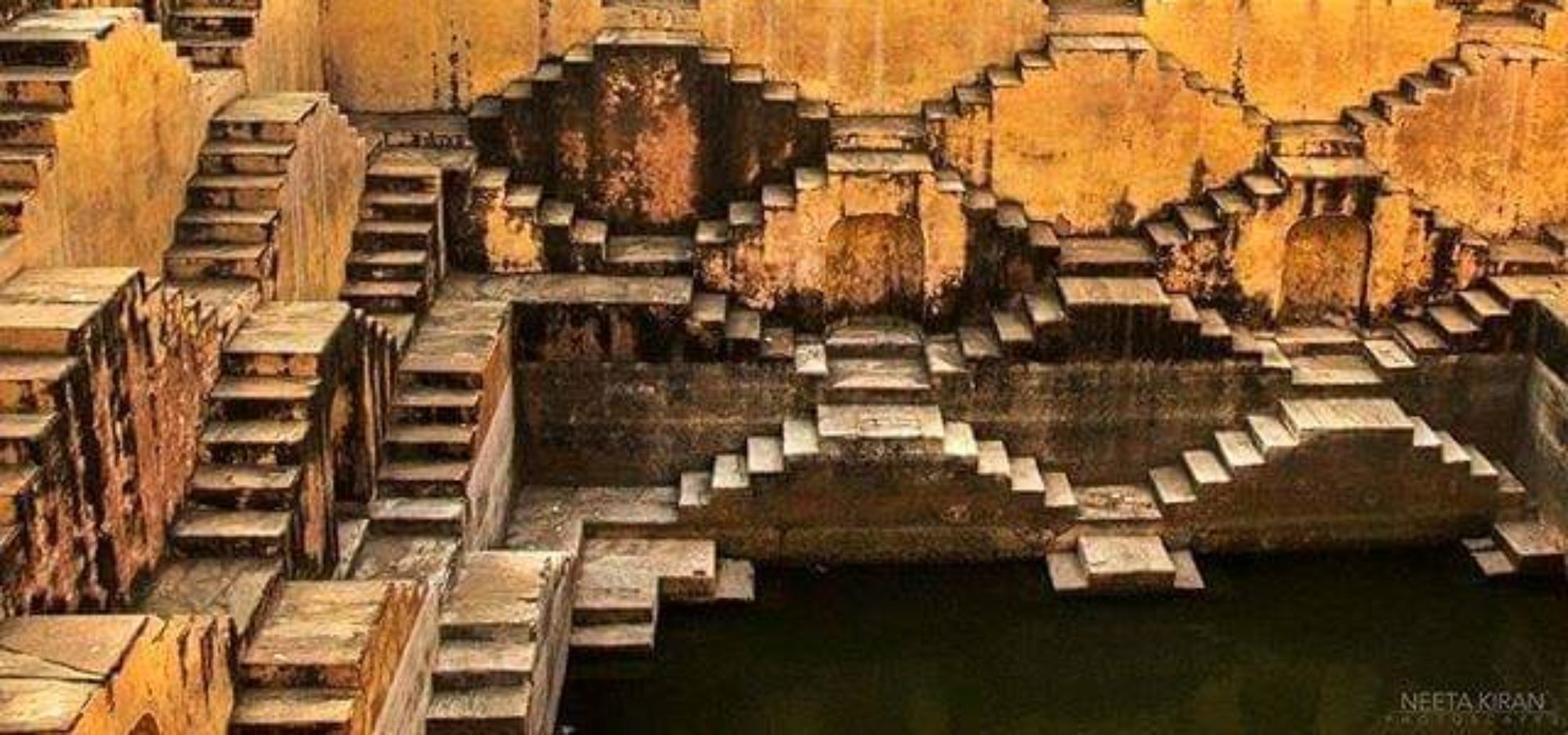


Leave a Reply