पिछले २०० – २५० वर्षों से मनुष्य को बहिर्मुखी बना दिया गया है, हमारी अपने ऊपर दृष्टि रही ही नहीं है, यदि कभी पड़ती भी है, तो भी केवल self consciousness के स्तर तक ही और वह भी केवल तुलना के माध्यम से। अपने भीतर क्या घटित हो रहा है, उसके उपर किसीका ध्यान ही नहीं है। यदि किसीको गुस्सा आता है या ईर्ष्या होती है या भय लग रहा है, तो उस व्यक्ति का इसके उपर ध्यान भी नहीं जाता कि उसके भीतर ये मनोभाव पैदा हो रहे हैं और स्वतंत्रता की इच्छा स्व में है, यह अनुभूति भी नहीं होती। स्वतंत्रता का विस्तृत अर्थ चाहे किसीको ना पता हो, लेकिन इतना तो ध्यान देने से कोई भी सोच सकता है कि मेरे उपर किसीका दबाव ना हो।
स्वतंत्रता की यह इच्छा प्रत्येक व्यक्ति में रहती ही है, यदि उसके उपर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाय। ठीक उसी प्रकार भय, ईर्ष्या, क्रोध भी प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है ही। यह सबको देखना अति आवश्यक है और यदि व्यक्ति स्वयं इन्हें देख नहीं पाता, तो शिक्षा के द्वारा उसे दिखाया जाय, देखना तो स्वयं ही है, बस देखने की प्रक्रिया में बाह्य सहायता हो सकती है, जोकि ध्यानाकर्षण करने भर से हो जाएगा।
आधुनिक शिक्षा ने भेदों को बड़ी स्पष्टता के साथ उजागर किया है, किसीको गोरा तो किसीको काला, किसीको ब्राह्मण, तो किसीको दलित तो किसीको आदिवासी तो किसीको कुछ, लेकिन सबके भीतर जो समानता है, उसकी ओर कोई ध्यानाकर्षण नहीं होता है, यह सब कहीं किसी पुस्तक में लिख देने से कुछ नहीं होगा, उसे पढ़ा देने से भी कुछ नहीं होगा, उसे रटा देने से भी कुछ नहीं होगा, ध्यानाकर्षण की प्रक्रिया ही मूलत: पढ़ाने – रटाने – लिखने – पढ़ने से भिन्न है और यह प्रयास आधुनिक शिक्षा में है ही नहीं।
‘स्वतंत्रता’ की दिशा में बढ़ना है, तो पहले ‘स्वत्व’ को पहचानना होगा। स्वत्व का अर्थ है: मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ का बोध और ये केवल आदतों के स्तर के बोध की बात नहीं है कि मुझे ये पसंद है और वो नहीं पसंद है, या मुझे ऐसा खाना पसंद है या जल्दी या देर से उठना पसंद है, आपकी मनोवृत्तियों को पहचानने को यह बोध कहा जाएगा।
यह बोध होते ही आपको स्वतंत्रता की चाह दिखने लगेगी, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि भी दिखने लगेंगे और इन सबके बीच के द्वंद्व भी दिखने लगेंगे और साथ ही साथ में यह भी प्रतीत होगा कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर के जैसे मानसिक विकारों को आधुनिक अर्थतंत्र समाजतंत्र व राजतंत्र के द्वारा बढ़ावा देकर बाजारतंत्र को खड़ा किया जाता है। आपकी छवि (image) बनाने की बात की जाती है, आपके व्यक्तिस्वातंत्र्य की बात की जाती है, सफलता के भी मापदंड बाहर से ही निश्चित किए जाते हैं और आप उन परिमाणों के अनुसार सफल होने की दौड़ में दौड़ पड़ते हैं, ना आप आगा सोचते हैं ना पीछा। आपकी छवि बनाने की बात को आपकी freedom के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि image ही तो आपको बांधकर रखती है, इस बंधन से मुक्त होने के लिए तो image बनाने या बिगाड़ने के चक्कर से मुक्ति पानी पड़ेगी, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनना पड़ेगा।
यह एक ऐसी प्रतिकूल व्यवस्था है, जिसमें स्वतंत्रता का हनन होता है (क्योंकि आप स्व को भी देख नहीं पाते), विकारों को भड़काया जाता है और freedom जैसी भ्रामक स्थितियों को स्वतंत्रता के नाम पर समाज में चलाया जाता है।
ध्यान देने से आज समझ में आता है कि आज एक की freedom और दूसरे की freedom के बीच में संघर्ष है, एक के free होने के लिए दूसरे का गुलाम बनना आवश्यक है। स्वतंत्रता तो उसे ही कहेंगे, जिसमें एक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता के लिए बाधक नहीं, उल्टा सहायक सिद्ध हो, तभी तो सहअस्तित्त्व बन पाएगा और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो प्रत्येक को स्वतंत्र होकर साथ में जीने के लिए सहायक सिद्ध हो और यह स्वतंत्रता तथा ये सहजता हर कोई साधारण मनुष्य को प्राप्त हो, ना केवल किसी व्यक्ति विशेष को।
ये व्यवस्थाएँ धर्मानुकूल होने से ही प्रत्येक व्यक्ति को सहजता व स्वतंत्रता से जीने में सहायक सिद्ध हो सकती है। धर्म का अर्थ यहाँ religion नहीं है, किन्तु जो व्यवस्था अस्तित्त्व में विद्यमान है, प्रकृति में विद्यमान है, उसीके आधार से धर्म को भी समझा जा सकता है।
जब व्यवस्था की बात होती है, तो कर्तव्यों की भी बात होती है, किन्तु ये कर्तव्य थोपे हुए कर्तव्य नहीं है, सहज कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों से कोई बोझ का भाव नहीं उत्पन्न होता, जैसे अपने बालक के लिए कुछ करना किसी भी माता का कर्तव्य है और यह उसे बोझ नहीं लगता, उसके आनंद का कारण बनता है, वैसे ही संपूर्ण समाज (मनुष्य, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, जीव जन्तु सब) के साथ आपका जो जुड़ाव है, उसीके आधार से कर्तव्य भी निश्चित हैं, उनके वहन में भी कोई बोझ की अनुभूति नहीं होती।
इसके विपरीत आजकी व्यवस्था में लगभग लगभग हर कर्तव्य एक बोझ सा बना प्रतीत होता है, जो सब ज़िम्मेदारी निभाता है, उसकी परेशानियों का कोई अंत ही नहीं है, जबकि पतली गली से निकल जाने वाले, जिम्मेदारियों से पल्ला झाड लेने वाले लोग मजे करते हैं, यही अवस्था बेईमानी को भी बढ़ावा देती है। यह व्यवस्थागत दोष है।
हर व्यक्ति के लिए सहजता व स्वतंत्रता के साथ जीने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रथम चरण तो ध्यानाकर्षण ही हो सकता है, कि हम कहाँ पर फँसे हुए हैं, व्यवस्थाओं में क्या दोष है इत्यादि। जैसे जैसे यह ध्यानाकर्षण होते जाएगा, वैसे वैसे हम आधुनिकता की दौड़ से मानसिक रूप से मुक्त भी होते जाएंगे। इसे एक उदाहरण से समझा जाए।
भारत में अङ्ग्रेज़ी आज एक भाषा ना रहकर गुरुताग्रंथि की द्योतक बन गई है, अङ्ग्रेज़ी में बोलने वाले व्यक्ति की बात सुनने से अधिक वृत्ति उससे अभिभूत होने की होती है और अमूमन बोलने वाले की भी चेष्टा सामने वाले को कुछ बताने या उससे बात करने से अधिक उसे प्रभावित करने की देखी जा सकती है। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति जागृति से देखता है, वह सचेत रूप से इस प्रभावित करने की चेष्टा से बचेगा और अङ्ग्रेज़ी का प्रयोग केवल भाषा के रूप में करेगा। यदि ऐसा होता है, तो वह अङ्ग्रेज़ी का उपयोग करते हुए भी उसके जाल में फँसने से बच जाता है।
साधारण मनुष्य अनिश्चितता को स्वीकार करता है, सब जानने का दावा नहीं करता है, वह जानता है कि कुछ है, जिसे वह नहीं जानता है और कुछ है जिसे वह जानता है। संभव है कि वह कुछ जानता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वह उसे जानता है और वह यह भी जानता है कि कुछ होगा जिसका उसको बोध नहीं होने का भी बोध नहीं है। इन चारों अवस्थाओं का अस्तित्त्व अनिश्चितता और अज्ञात के साथ जुड़ा हुआ है और इसी अनुभूति के साथ साथ ही आस्था भी विकसित होने लगती है। यह सभी के लिए संभव है, बस थोड़े से आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है।
आत्मनिरीक्षण के लिए आवश्यक है कि जीवन की गति थोड़ी सी धीमी हो। यह गति का धीमा होना या तो अपने आप हो सकता है, या तो कोई झटके की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। किसीके परिवारजन का देहांत होता है, तो आँखें खुल जाती हैं, किसीको बड़ी चोट लगती है, तो आँखें खुल जाती हैं, किसीको जीवन में बड़ी असफलता मिलती है, तो आँखें खुल जाती हैं, किसीको कोई धोखा देता है, तो आँखें खुल जाती है।
बहुतों के लिए कोरोना का संकट भी आँखें खोल देने वाला हो सकता है। घर में सुकून से बैठने का समय मिला है, उससे भी बहुत कुछ हो सकता है। कमसेकम इतनी आशा तो रखी जा सकती है। संभव है कि इस काल में डिजिटल नियंत्रण, अनिवार्य टीकाकरण जैसे आसुरी उपायों के उपर भी काम चल रहा हो, लेकिन कुछ ठीक होने की आशा तो रखी ही जा सकती है।
मजबूत आशा विश्वास से ही जनित हो सकती है और यह विश्वास आस्था से जुड़ा हुआ है। आशा की उत्पत्ति इस आस्था से भी हो सकती है, जब आप समझते हैं कि यही जीवन सबकुछ नहीं है, यह तो आपकी अनंत यात्रा का एक क्षणिक पड़ाव है और आप इस जीवन के बाद भी फिर से किसी और स्वरूप में आएंगे।
यह आशा – यह आस्था साधारण के भीतर बहुत मजबूत है, क्योंकि यह उन्हें विरासत में मिली है, कुछ ऐसे जैसे एक शिशु अपने घर में मातृभाषा सीखता है, उसे सीखने के ना कोई नियम होते हैं, ना कोई पद्धति और ना ही कोई तर्क, केवल उस वातावरण में बसने की और उसे अवशोषित होने देने की बात रहती है, जबकि हमारे जैसे पढे लिखे लोग जब स्वयं के भीतर आस्था विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो यह कुछ ऐसा प्रयास है, जिसमें एक बच्चा स्कूल में कोई भाषा सीख रहा हो। उसमें विशेष प्रयास करने पड़ते हैं।
आधुनिक व्यक्ति के शरीर और मन सदैव गतिशील रहते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं। यही अनावश्यक गतिशीलता हड़बड़ाहट, थकान और भय को जन्म देती है। स्थिरता के अभाव में वह बड़ी सरलता से किसी से भी प्रभावित होने लगता है और यहीं से वह भय एवम् भ्रम से ग्रसित होने लगता है।
सुनिए पवन गुप्त जी की वाणी में Deconstructing Modernity शृंखला का नवम चरण: Stepping out of the Modern Paradigm – Swatantrata।
For more videos, click on https://saarthaksamvaad.in/videos/
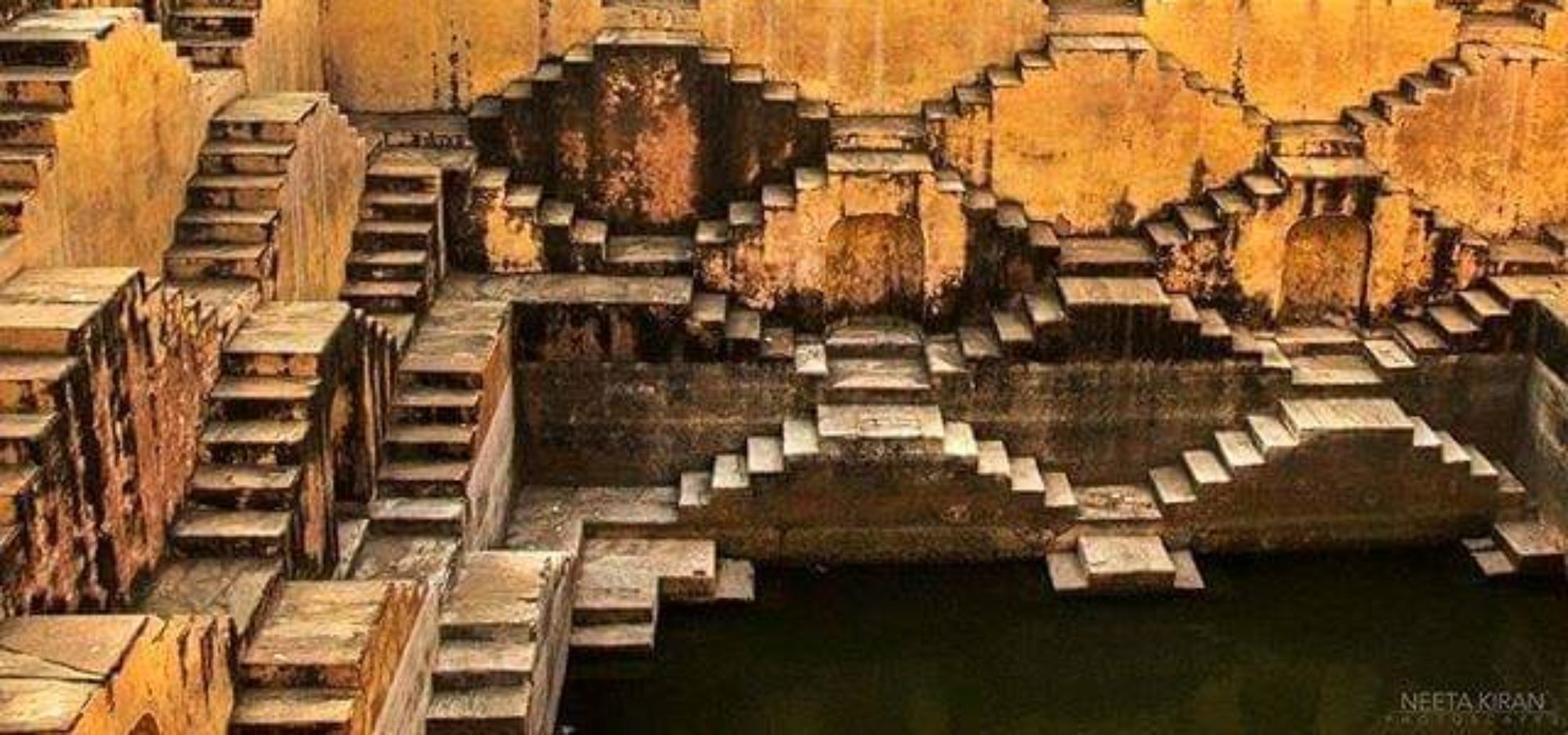

Leave a Reply