जिस तरह का प्रोत्साहन एवं सहयोग-तंत्र कृषि क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है, लगभग उतना ही, बल्कि उससे भी विशाल प्रोत्साहन एवं विस्तृत सहयोग-तंत्र देश में बड़े उद्योगों एवं समाज में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। कृषि क्षेत्र में स्थापित एक स्वतंत्र कृषि मंत्रालय की ही तरह, उद्योग क्षेत्र में समन्वय के लिए भी एक स्वतंत्र उद्योग मंत्रालय सरकार के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य कर रहा है।
इस पूरे व्यवस्था-तंत्र के माध्यम से समाज में बड़े उद्योगों को स्थापित करने, उनके व्यवस्थित संचालन एवं समाज में औद्योगीकरण को लगातार बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कार्य होता रहा है, पंरतु इस व्यवस्था में भी कारीगर, कारीगरी क्षेत्र और उससे संबंधित संपूर्ण कार्य, हमारे मूलभूत उद्योग होने के बावजू़द भी कहीं छूट गए है। कृषि और बड़े उद्योग, दोनों की तुलना में लगभग नहीं के बराबर का ध्यान, ऊर्जा, समय, खर्च और प्रयास कारीगरी के क्षेत्र की ओर किया जा रहा है।
कृषि क्षेत्र में वर्तमान तरह की निर्भरता बढ़ने से पहले, समाज के कारीगरी क्षेत्र में तरह-तरह का सामर्थ्य जहां-तहां सहज ही भरा पड़ा था। हम उद्योग-प्रधान देश होने के नाते न केवल कारीगरी एवं औद्योगिक कौशल के मामले में अग्रणी थे, बल्कि उससे भी बढ़िया हमारा व्यापारिक कौशल एवं कमाए हुए धन के बंटवारे की व्यवस्थाएँ थीं। गाँवों में विभिन्न सामानों की बिक्री और बिक्री के बाद धन के बंटवारे को लेकर कुछ स्वतंत्र व्यवस्थाएँ, कुछ पक्के नियम थे, जिनका लोग बहुत ही कड़ाई से पालन किया करते थे। यह हमारी इन व्यवस्थाओं के कारण ही था कि दूर देशों के व्यापार से प्राप्त हुई चांदी, सुदूर गाँवों के आदिवासियों इलाकों तक भी बराबर से पहुंचती रही है।
इन नियमों में सबसे पहला नियम था कि गाँव के (लोगों से कमाए) पैसों से (गाँव के) बाहर की कोई चीज नहीं खरीदी जाती थी। (गाँव के) बाहर की कोई चीज खरीदनी है, तो (गाँव के) बाहर से ही पैसा कमाना होता था। गाँव के कारीगर लोग, गाँव के लोगों का काम तो करते ही थे। मगर, उसके बाद भी इनके पास बहुत समय बचा रह जाता था। अपने खाली समय में, बरसातों आदि में ये लोग बहुत सुंदर-सुंदर चीजें बनाते थे। ये चीजें या तो कुछ जात्राओं में बिकती थीं, या फिर बाहर के देशों में व्यापार के लिए चली जाती थीं। साल की तीन जात्राएँ करके ये लोग कम से कम एक तोला सोना खरीद कर आते थे। सोना बाहर की चीज थी। गाँव के बाहर की जात्राओं से कमा कर, वहीं से सोना खरीद कर लाते थे। गाँव में चीजें बेचकर सोना नहीं खरीदा जाता था। आजकल तो इसके ठीक उल्टे गाँव के पैसे से दुनिया भर की बाहर की चीजें गाँव में घुस रही हैं। गाँव का पूरा पैसा बाहर (के बाजा़रों) की चीजें खरीदने में लग रहा है। गाँव की पूरी समृद्धि इसी रास्ते गाँवों से बाहर जा रही है।
इसी प्रकार, समाज में वैश्य वर्ग कोई अलग समाज या कोई अलग जाति नहीं थी। हर कारीगर वर्ग में से एक छोटा सा समूह होता था जो कि अपनी और अपने समाज के अन्य लोगों की बहुत सारी चीजों को गांव और देश से बाहर बेचने के लिए निकलता था। जुलाहों में से एक समूह, चर्मकारों में से एक समूह, बढ़इयों में से एक समूह, इस तरह हर जाति का एक-एक समूह निकलता था और ये सारे लोग मिलकर बाहर के व्यापार के लिए जाते थे।
गुरूजी बताते हैं कि हमारे यहां व्यापार दो तरीके से चला है। एक तो पानी के द्वारा – जहाज, नाव आदि के माध्यम से। और दूसरा सड़कों के द्वारा – सार्थवाह के माध्यम से। पुराणों आदि से लेकर ढेरों किस्सों, कहानियों में वैश्यों द्वारा पानी के द्वारा व्यापार के ढेरों जिक्र आते हैं कि फलाना वैश्य पानी के जहाज से फलानी दिशा में व्यापार करने गया था और दूसरा आता है, सार्थवाह। हमारे यहां एक चंद्रगुप्त वेदालंकार नामक एक विद्वान हुए हैं। बहुत छोटी उम्र में ही गुजर गए थे। मगर, उस छोटी सी उम्र में ही उनकी एक बहुत ही जबरदस्त किताब देखने में आई थी – वृहत्तर भारत। उसमें भारत के रास्तों का एक बहुत बड़ा अध्ययन सरीखा था। देश के विभिन्न रास्तों का बहुत ही विस्तार से वर्णन था कि व्यापार के लिए हम कौन-कौन से रास्ते इस्तेमाल करते थे, तीर्थों के लिए हम कौन से रास्ते इस्तेमाल करते थे आदि। उस पुस्तक में सार्थवाहों की पूरी पद्धति का भी बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है कि उनके एक-एक समूह में किस-किस तरह के कितने-कितने लोग होते थे। इनके साथ में इनकी कौन-कौन सी सुविधाएँ और कैसी-कैसी व्यवस्थाएँ चलती थीं। सार्थवाहों के साथ में बकायदा उनकी सेना चलती थी। उनकी पाठशालाएँ इत्यादि भी साथ में ही चलती थी। उनके वैद्य एवं अन्य चिकित्सीय सहायता तो साथ में चलती ही थी। एक-एक सार्थवाह में हजारों लोग एक साथ चलते थे। इतने सारे लोगों के राशन-पानी की, पानी की, दैनिक शौच इत्यादि की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। लोगों को लंबी दूरी के एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे तमिलनाडु से तक्षशिला आदि जाना होता था, तो वे किसी सार्थवाह में अपना नाम लिखा देते थे। नियत समय में जब सार्थवाह उस जगह से गुजरता था, तो वह उनके साथ हो जाते थे। काशी जाना है, या कहीं और की यात्रा करना है, तो किसी सार्थवाह के साथ ही निकल जाते थे, चूंकि उनकी पूरी व्यवस्था उनके साथ में चलती थी, इसीलिए किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती थी।
इन दोनों तरीकों के व्यापारों में, ये लोग विदेशों में जाकर, अपना सामान आदि बेच कर बदले में चांदी आदि लाते थे। उसको अपने-अपने समाजों में लाकर, जिसका जितना हिसाब हुआ, उस हिसाब से बाँट देते थे। कुछ समय बाद फिर से सभी लोगों का सामान लेकर निकल पड़ते थे। कई शताब्दियों से, कई पीढ़ियों से इसी तरह की पद्धति चलने से, इसी तरह जाने-आने से उन सारे लोगों की जातियाँ अलग-अलग होते हुए भी उनकी दिनचर्या एक जैसी हो गई थी। उठना-सोना, खाना-पीना और भी बाकी सारा काम लगभग एक जैसा ही हो गया था। अंग्रेजों के आने के बाद से जब इनका व्यापार और व्यापार का यह ढंग टूटा, तो ये सारे लोग अपनी दुकानें लगाकर बैठने लग गए। यही समाज वैश्य वर्ग कहलाया। यही सारे लोग वैश्य कहलाए। इसीलिए वैश्य एक वर्ण था, न कि एक जाति। उसमें बहुत तरह के लोग, बहुत सी जातियों (ज्ञातियों) के लोग नजर आते हैं। इसी तरह क्षत्रिय वर्ण का भी है। हमारे यहां ‘क्षात्र’ न तो अपने आप में कोई जाति रही है, और न ही यह किसी की ‘वृत्ति’ रही है। हर जाति का एक समूह अपने आप को क्षत्रिय मानता था। इस समय जो क्षत्रिय हैं, वह हर जाति में से निकला हुआ एक समूह था। चर्मकारों में से समगार निकले थे, जुलाहों में से रंगारे थे, ब्राह्मणों में से भूमिहार थे। इसी तरह हर जाति का एक समूह था। ठीक इसी तरह से वैश्य वर्ण भी था, जिसमें हर जाति का एक समूह था।
इस तरह से हमारा पूरा व्यापार चलता था और व्यापार के बदले में बाहर से चांदी आदि आती थी। और यह सब कुछ हजारों साल से ऐसे ही चलता रहा था। यह नहीं कि दस-बीस साल या पचास-सौ सालों से ही ऐसे चल रहा है। गुरूजी बताते हैं कि आदिलाबाद का लोहा यूनान तक जाता था। आदिलाबाद के लोहे को दमष्क बोलते थे। वहां जो दमष्क शहर है, वह इसी लोहे के नाम पड़ा है, ऐसा कहा जाता है। आदिलाबाद का लोहा तलवारों के लिए बहुत मशहूर था।
वे बताते हैं कि उनका अपना एक अध्ययन रहा है कि आखिर आदिलाबाद के इलाके में आदिवासियों के पास इतनी चांदी आई कहां से, क्योंकि उस इलाके के आदिवासियों के पास थोड़ी-बहुत चांदी नहीं है, बहुत चांदी है। वे बताते हैं कि एक बार आदिलाबाद में वहां के एक आदिवासी क्रांतिकारी – कोमराम भीम पर फिल्म बन रही थी। उस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर गुरूजी ही थे। उस फिल्म के लिए उन्होंने वहां के बहुत से इलाकों में घूमकर वहां के गहनों आदि की बहुत सी जानकारियां इकट्ठी की थीं। उस दौरान वे कई सुनारों से भी मिले। उन सब से मिलने पर उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही हुआ करता था कि पिछले दस सालों में उन्होंने लगभग कितनी चांदी गला ली होगी। और उन सभी के उत्तर आश्चर्यजनक हुआ करते थे। दस सालों के अंदर उनमें से लगभग सभी ने 6-6, 8-8, 10-10 क्विंटल चांदी के गहने गला डाले थे। पूछने पर पता चला कि पता नहीं क्यों, मगर लोग अपनी चांदी बेचते जा रहे हैं।
उस समय तो खैर ये आदिवारी लोग अपनी चांदी बेच रहे थे। मगर, प्रथम दृष्टया, उन्होंने यह चांदी कमाई कैसे थी! उनके पास आखिर इतनी चांदी आई कहां से थी! गुरूजी बताते हैं कि और जानकारियां लेने पर इस सबकी बइुत सुन्दर व्यवस्थाएँ वहां दिखाई दीं। बड़ी आसानी से यह पता लगा कि आदिवासी समाज आजकल की तरह तथाकथित मुख्यधारा से इतना कटा हुआ नहीं था। आदिलाबाद कस्बे के सारे सूखे पशु इन आदिवासियों के पास जंगल में ही रहा करते थे। आदिलाबाद बस्ती में केवल दूध देने वाले पशु ही लोग अपने पास गांव में रखते थे। बाकी सारे पशु जंगलों में आदिवासियों के पास छोड़ दिए जाते थे। उसके लिए बकायदा उनको अनाज दिया जाता था। हजारों पशु उनके पास होते थे। पशुओं के मर जाने पर उसकी खाल वे लोग ही तैयार करते थे। खाल उनकी हुआ करती थी। पशु के मर जाने के बाद उसके चमड़ा, सींग, आदि अन्य सारी चीजें भी वे लोग ही रखते थे। इन सारी चीजों पर उनका ही अधिकार हुआ करता था। बस्ती के चर्मकारों को चमड़ा की जरूरत होने पर, वे उनके पास जाकर, बदले में चांदी आदि देकर अपनी जरूरत का चमड़ा लाते थे। इसी तरह, बंगलगिरि समाज के लोग हैं, जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं। वे लोग भी साल में दो-तीन बार उनके पास जाकर, बदले में चांदी आदि देकर, सींग लाते थे, जिससे चूड़ियां तैयार होती थीं। इसके अलावा, जंगलों में एक विशेष तरह का घास भी होता था। आदिवासी लोग उस घास की कटाई करके अपने पास रखते थे। बस्ती में उस घास से निकले तेल का व्यापार करने वाले व्यापारियों का एक समूह था। वे लोग जंगलों में जाते थे, बदले में चांदी देकर उनसे घास लेते और वहीं उसका तेल निकलवाते थे। आदिवासी लोग वहीं जंगलों में भट्टियां लगाकर उसका तेल निकालते थे। उसके लिए भी उन लोगों को चांदी मिलती थी। इसके अलावा, ये लोग बहुत तरह की जड़ी-बूटियां तैयार करते थे। इस तरह से सारा कुछ चलता रहता था, जिससे उनके पास बहुत सी चांदी इकट्ठी होती रहती थी। इन सारी पद्धतियों के टूटने के बाद से ये लोग कंगाल होना चालू हो गए। नतीजतन, उनको अपनी चांदी बेचने की भी नौबत पड़ने लगी। नहीं तो, इसके पहले ये लोग समाज से इतने कटे हुए नहीं थे। रहते जरूर जंगलों में थे, मगर समाज के साथ जुड़े हुए ही थे।
व्यापार के इन्हीं तौर-तरीकों के प्रतीक के तौर पर हमारे यहां अभी भी दशहरे के अवसर पर ’सीमोल्लंघन’ की परंपरा निभाई जाती है, चूंकि, गाँव के भीतर व्यापार का निषेध हुआ करता है, इसीलिए लोग गांव की ’सीमा का उल्लंघन’ करके गाँव के बाहर जाते हैं, और गाँव की सीमा से बाहर से ‘सोने’ और ‘चांदी’ के स्वरूप में ‘शमी’ की पत्तियाँ और ‘जवारी’ लेकर आते हैं। यह ‘सोना’ और ‘चांदी’ भी स्वयं के उपयोग के लिए या स्वयं के घरों में ले जाकर के रखने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसे आपस में गले मिलकर लोगों में बांटा जाता है। ठीक उसी तरह जैसे बाहर से वैश्य वर्ण के लोगों के द्वारा कमाकर लाई गई धन-संपदा को वे लोग अपने-अपने कारीगरी बंधुओं में बांट दिया करते थे। इस तरह के बंटवारे का समय भी ज्यादातर दशहरे के आसपास हुआ करता था।
यह हमारे देश की उद्योग-प्रधान प्रकृति, व्यापार की पद्धतियां और व्यापार-लाभ के बंटवारे की हमारी अपने तरह की व्यवस्थाऐं ही थीं, जिसके कारण हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया और व्यापार का लाभ कुछ ही हाथों में न सिमट कर सभी लोगों तक बराबरी से पहुंचा था।
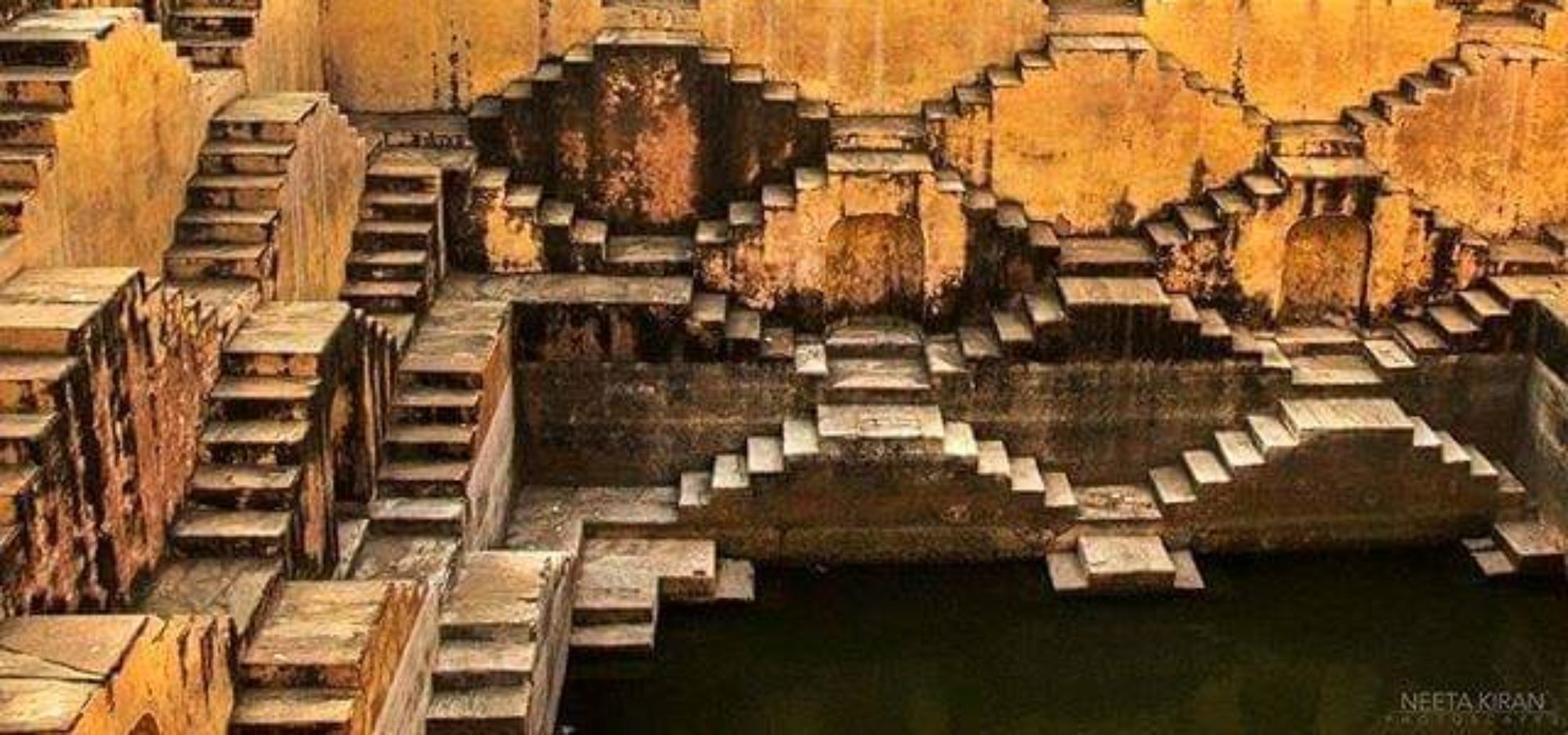


Leave a Reply