अभी कुछ दिन पहले ही नवगठित मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की प्रथम बैठक एक कार्यशाला के रूप में सम्पन्न हुई। बैठक और कार्यशाला का मुख्य विषय ‘पारम्परिक एवं देशज ज्ञान-विज्ञान का चिन्हीकरण और दस्तावेजीकरण’ था। श्री आशीष कुमार गुप्ता जी के विचार बैठक में प्रस्तुत लोगों को विशेष रूप से पसंद आए। बैठक के मुख्य अतिथि और कार्यशाला के मुख्य रिसोर्स पर्सन के रूप में पधारे IIM अहमदाबाद के श्री अनिल गुप्ता जी ने इन विचारों को लिपिबद्ध करके शीघ्र ही प्रस्तुत करने का वचन ही ले लिया। इस संदर्भ में ये विचार यहाँ भी प्रस्तुत हैं।
जिस तरह से ‘कला’ और ‘सामाजिकता’ एक कसौटी रही है, उसी तरह से ‘आर्थिक समानता’ एक अन्य महत्वपूर्ण कसौटी रही है। क्या हमने कभी सोचा है, कि ‘विज्ञान’ तो ठीक है, पर उस विज्ञान को अपनाकर बने उद्योगों और उन उद्योगों से बने उत्पादों के व्यापार की पद्धतियाँ क्या रही होगी? आज यह ज्ञात तथ्य है, कि 18 वीं सदी के शुरुआत तक भारत की विश्व व्यापार में 25-30% की भागीदारी थी। उसकी तुलना में, आज यह भागीदारी मात्र 1 से 1.5% के आसपास ही है। आजकी इस निम्नतम स्तर की भागीदारी के समय देश में टाटा, बिरला, अंबानी आदि जैसे हजारों व्यापार और उद्योग-घरानों का अस्तित्व हमारे पास है। उसी अनुपात में यदि हम तुलना करें, तो विश्व-व्यापार में 25-30% की भागीदारी की स्थिति में देश में इस तरह के घरानों की संख्या कितनी होनी चाहिए? पर क्यों हम टाटा, बिरला आदि से पहले के किसी उद्योग या व्यापारी घराने का नाम नहीं जानते हैं? क्योंकि ऐसे घराने अस्तित्व में ही नहीं थे; क्योंकि हमारे यहाँ अर्थ के, समृद्धि के उचित बँटवारे की उत्तम व्यवस्थाएँ उपलब्ध थीं; क्योंकि हमारी व्यवस्थाओं की उच्चता-मापन की एक मात्र कसौटी ‘विज्ञान’ और ‘धनार्जन’ नहीं थी; क्योंकि उत्पादन और उत्पादन की तथाकथित अधिक आधुनिक, अधिक वैज्ञानिक पद्धतियों और उसके माध्यम से अधिक से अधिक उत्पादन करने और धनार्जन करने से ज्यादा महत्त्वपूर्ण कसौटी ‘धन के उचित और समान बँटवारे’ की पद्धतियाँ थीं। समाज ने तथाकथित कई अधिक ‘वैज्ञानिक’ विकल्पों को नकारने में भलाई समझी, जोकि समाज में आर्थिक असमानता का कारण बन सकते थे। यही कारण है, कि इतने विशाल-विशाल, भव्य मंदिर और किले बना सकने वाले सामाज ने, समाज में लोहारों, बढ़ई, बंसकारों आदि वाली ‘छोटी टेक्नोलॉजी’ को ही प्रश्रय दिया, न कि maas-production वाली बड़े-बड़े कारखानों वाली टेक्नोलॉजी को, क्योंकि शायद ये भी समाज में आर्थिक असमानता ही लातीं, जैसा कि आजकल ला ही रही हैं।
वर्तमान के ‘वैज्ञानिक’ दृष्टिकोण मात्र रखने की एक और समस्या यह भी है, कि आजका तथाकथित ‘आधुनिक विज्ञान’ अपने आप में अधूरा ही है। अभी कुछ वर्षों पूर्व तक हम जिन चीजों को अवैज्ञानिक मानते रहे हैं, विज्ञान के नित नूतन आविष्कारों, खोजों के कारण आज उनकी वैज्ञानिकता समझ में आ रही है। वर्तमान की वैज्ञानिक खोज, आगे होने वाली खोजों की तुलना में तो अधूरी ही हैं। पर हमने भूतकाल के कई रीति-रिवाजों को उस समय के अनुसार अवैज्ञानिक साबित करके, उन्हें अंध-विश्वास घोषित करके, उन पूरी व्यवस्थाओं को समाज से एकदम बाहर ही कर दिया है। वही सारी प्रथाएँ, वर्तमान के विज्ञान के अनुसार वैज्ञानिक नजर आती हैं, जिसके कारण, हम सब उनको पुनर्जीवित करने में लगे हैं। कुछ वर्षों पूर्व ही हमने माँ के पहले दूध, जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, को अवैज्ञानिक और अंध-विश्वास से भरा मान लिया था। फिर, कुछ वर्षों बाद, उसे पुनः वैज्ञानिक साबित करके, उस पर करोड़ों रुपये खर्च करके उसको समाज में पुनर्स्थापित करने में लगे हैं। इसी तरह से, हमारे समाज में नवजात बच्चों की नाल को बहुत ही सुरक्षित करके रखने का प्रावधान पीढ़ियों से था। नाल के सूखकर गिर जाने के उपरान्त, उसे हल्दी में डूबे एक कपड़े में बहुत सुरक्षित ढंग से रखकर, फिर उसको एक बहुत छोटे से मटके में रखकर, उसमें उस बच्चे का नाम लिखकर या कोई निशानी लगाकर, घर के पिछवाड़े में सावधानी से गाड़कर रख दिया जाता था। ताकि, बच्चे को कुछ असाध्य बीमारी हो जाने पर उसी नाल से दवाइयाँ, आदि बनाकर दि जा सके। बंजारों के जैसी घुमक्कड़ जातियों में नाल के एक छोटे से टुकड़े को एक बड़े से तावीज में बाँधकर उसके शरीर में ही बाँध दी जाती थी, ताकि वक्त जरुरत में वह उसके पास ही रहे। परंतु, आज से कुछ वर्ष पूर्व के आधुनिक विज्ञान ने उसको अंध-विश्वास साबित कर दिया था। आज यह पूरी पद्धति फिर से वैज्ञानिक साबित हो गई है और अब लाखों रुपये वसूल करके उसको ‘स्टेम सेल’ बैंक में रखवाकर उसे वैज्ञानिक साबित कर दिया गया है। पहले कोयला, नमक आदि खुरदरे पदार्थों से दांत साफ करने को अवैज्ञानिक और आज कुछ वर्षों बाद फिर से वैज्ञानिक करार दिया जा रहा है। काँसे की थाली में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना खड़े होकर दूध पीना और बैठकर पानी पीना आदि जैसे कई उदाहरण हैं, जिन्हें समाज में से एक समय में निष्कासित करके उन्हें फिर से समाज में लाया जा रहा है। कुछ इसी तरह का अनुभव महिलाओं में माहवारी के दौरान ‘कपड़े के उपयोग’ को नकारकर तथाकथित ज्यादा सुरक्षित ‘सैनेटरी नैपकिन’ को प्रोत्साहित करने का है, जिसकी अपनी स्वयं की ढेरों समस्याएँ अब हमारे सामने हैं। कहने का अर्थ यह है, कि ‘आधुनिक विज्ञान’ अपने आप में अधूरा है। एक अधूरी चीज, जिसके मापदण्डों में नित नए परिवर्तन आ रहे हों, वह खुद दूसरी चीजों को मापने की कितनी कारगर कसौटी हो सकती है, यह सोचने वाली बात तो है ही।
इसीलिए, हमारे परम्परागत ज्ञान-विज्ञान को चिन्हित करना है, उनका दस्तावेजीकरण करना है, तो उन्हें ‘विज्ञान’ के साथ-साथ ‘कला’, ‘अध्यात्म’, ‘सामाजिकता’, ‘सामाजिक अर्थशास्त्र’, ‘प्रकृति प्रेम’, ‘पर्यावरण संरक्षण’ आदि जैसे कुछ और भी महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणों से देखना होगा। इन सभी की जाँची-परखी कसौटियों पर कसना होगा, अन्यथा हम अपनी सभी चीजों को एक एकांगी दृष्टि से मापकर उन्हें व्यर्थ में ही अंध-विश्वास या कुरीति, कुप्रथा मानकर दरकिनार करते चलेंगे और समाज एक एकांगी दृष्टिकोण पर आधारित होकर एकंगा हो जाएगा।
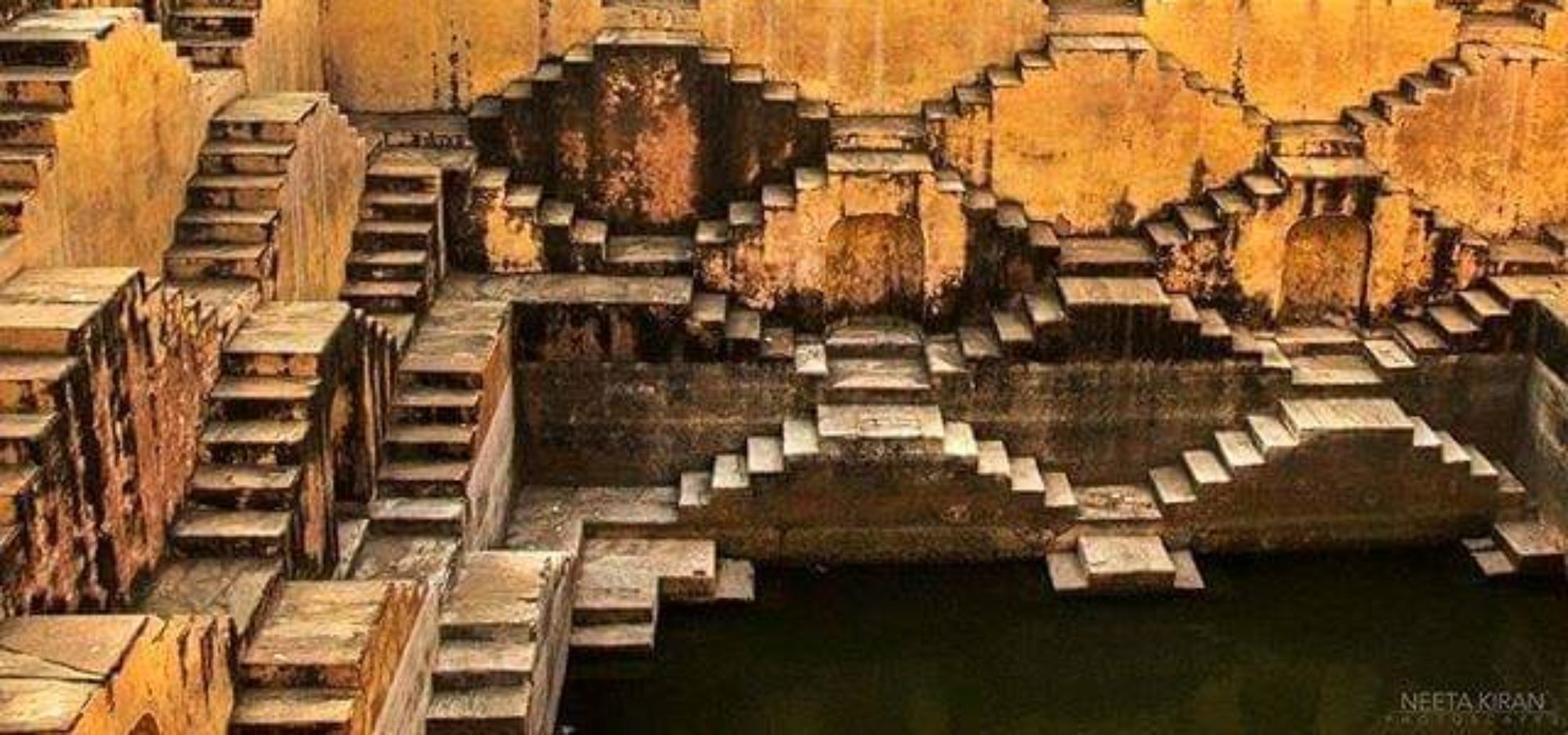

Leave a Reply