अभी कुछ दिन पहले ही नवगठित मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की प्रथम बैठक एक कार्यशाला के रूप में सम्पन्न हुई। बैठक और कार्यशाला का मुख्य विषय ‘पारम्परिक एवं देशज ज्ञान-विज्ञान का चिन्हीकरण और दस्तावेजीकरण’ था। श्री आशीष कुमार गुप्ता जी के विचार बैठक में प्रस्तुत लोगों को विशेष रूप से पसंद आए। बैठक के मुख्य अतिथि और कार्यशाला के मुख्य रिसोर्स पर्सन के रूप में पधारे IIM अहमदाबाद के श्री अनिल गुप्ता जी ने इन विचारों को लिपिबद्ध करके शीघ्र ही प्रस्तुत करने का वचन ही ले लिया। इस संदर्भ में ये विचार यहाँ भी प्रस्तुत हैं।
भारत में पारम्परिक एवं देशज ज्ञान-विज्ञान को चिन्हित करके उसके दस्तावेजीकरण का कार्य नया नहीं है। 80 के दशक में आईआईटी के छात्रों का एक बहुत बड़ा दल धरमपाल जी से प्रेरणा पाकर इस काम में लगा था। इसके अलावा भी बहुत से लोग, अन्य कई लोगों से प्रेरणा पाकर इस काम में लगातार लगे रहे हैं। इन सब प्रयासों में हमारी परम्पराओं, हमारे सभी रीति-रिवाजों को ‘ज्ञान’ के रूप में चिन्हित करने की मात्र और केवल एक मात्र कसौटी तथाकथित ‘आधुनिक विज्ञान’ ही रही है। जो भी परम्परा, रीति, रिवाज या प्रथा आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरी, उसे परम्परागत ‘ज्ञान’ मान लिया गया और जो इस कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई, उसे अंध-विश्वास मानकर, कुप्रथा मानकर, कुरीति मानकर नकार दिया गया। अभी भी इस दिशा के सभी कार्यों, सभी बैठकों, कार्यशालाओं में यह दृष्टिकोण निरन्तर रूप से दिखाई दे जाता है। हमें अपने इस एकांगी दृष्टिकोण से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी हमारा पूरा का पूरा समाज ‘विज्ञान’ के साथ-साथ ‘कला’, ‘अध्यात्म’, ‘सामाजिकता’, ‘सामाजिक अर्थशास्त्र’, ‘प्रकृति-प्रेम’, ‘पर्यावरण-संरक्षण’ जैसे कई मजबूत स्तम्भों पर बराबरी से खड़ा था। हमारी परम्पराओं, रीति-रिवाजों के पीछे के कारण केवल और केवल ‘वैज्ञानिक’ नहीं थे, बल्कि ये सारे और इनके जैसे कई और कारण भी थे। ‘विज्ञान’ तो था ही, पर विज्ञान के साथ-साथ ये सारे कारण भी थे। हमारी पूरी की पूरी जीवनशैली ‘वैज्ञानिक’ तो थी ही, पर उसके साथ-साथ वह उतनी ही ‘कलात्मक’ भी थी, उतनी ही ‘सामाजिक’ भी थी, उतनी ही ‘आध्यात्मिक’ भी थी, उतनी ही ‘पर्यावरण-सम्मत’ भी थी, उतनी ही ‘आर्थिक समानता’ वाली भी थी।
यही कारण है, कि आज से कुछ वर्ष पूर्व तक भी हमारे जीवन के हर कार्यकलाप के ढेरों गीत बना करते थे। यदि, हम आज से 25-30 वर्ष पहले के सिनेमा में फिल्माए गए गीत-संगीत को देखेंगे (क्योंकि दुर्भाग्य से दस्तावेज के रूप में वही हमारे सामने है), तो पाएंगे कि बैलगाड़ी पर, तांगों पर, घोड़ों पर ढेरों गीत बने हैं। वहीं इसके विपरीत, आवागमन के तथाकथित वैज्ञानिक साधनों पर – बसों पर, कारों पर, ट्रैक्टरों आदि पर आज हम कितने गीत गाते हैं। आधुनिक विज्ञान से रचे-बसे इन साधनों में गीत-संगीत उपजता ही नहीं है।
एक बार गुरुजी श्री रवींद्र शर्मा जी किसी आईआईटी में innovation की एक प्रदर्शनी देख रहे थे। वहाँ का सबसे ज्यादा प्रशंसा पाने वाला innovation एक कोई करघा था, जो के कपड़े बुनने के कार्य को बहुत ही सरल और efficient बना रहा था। गुरुजी ने सारा कुछ देखने के बाद उनसे जो पहला प्रश्न पूछा, वह यह था कि “इसमें से आवाज कैसी आती है।” यह प्रश्न, वहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए एकदम अटपटा और विस्मयकारी था। किसी भी यंत्र की आवाज और उसकी efficiency आदि में भला क्या रिश्ता हो सकता है। उपस्थित लोगों में से अधिकतर लोगों ने तो उस प्रश्न को जवाब देने लायक ही नहीं समझा। लगभग सभी ने गुरुजी और गुरुजी के उस प्रश्न को एक नौसिखिये का प्रश्न समझकर नजरअंदाज ही कर दिया। पर, एक युवक के मन में यह प्रश्न पचा नहीं। उसने गुरुजी से पूछ ही लिया, कि आखिर आपने यह एकदम असंबंधित सा प्रश्न क्यों पूछा। गुरुजी बोले, कि एक व्यक्ति लगभग 8 से 10 घंटे तक एक करघे पर काम करता है। उससे निकलने वाली आवाज का उसके शरीर के साथ रोजाना इतने घंटों का साथ रहता है। यदि वह आवाज कर्कश होगी, तो उसका हमारे शरीर पर, हमारी कार्यक्षमता पर एक तरह का प्रभाव पड़ेगा और वहीं अगर वह आवाज एक लय में, एक ताल में होगी, तो उसका हमारे शरीर पर दूसरे ढंग का प्रभाव पड़ेगा। किसी मशीन से आने वाली आवाज का हमारे शरीर पर बहुत असर पड़ता है। आज हम ‘कला’ आदि के इस पक्ष को पूरी तरह से नजरअन्दाज करके ‘विज्ञान’ की एकांगी दृष्टि पर ही आधारित हो गए हैं। इससे हमें बचना होगा।
इसी तरह, हमारे बहुत से रीति-रिवाजों में, व्यवस्थाओं में ‘सामाजिकता’ को बहुत बड़ा स्थान दिया गया था। गुरुजी श्री रवीन्द्र शर्मा जी पूछते हैं, कि जिस तरह हमारी सभी चीजों को, व्यवस्थाओं को नापने की एकमात्र कसौटी ‘विज्ञान’ हो गई है, क्या उसी तरह से ‘विज्ञान’ को नापने की भी कोई कसौटी है, या नहीं? शायद नहीं। यही कारण है, कि ‘विज्ञान’ समाज में निरंकुश हो गया है। वे ही आगे बताते हैं, कि कभी विज्ञान को नापने की हमारी सबसे प्रमुख कसौटी ‘सामाजिकता’ थी। कोई भी रीति-रिवाज कितना भी वैज्ञानिक क्यों न हो, यदि वह समाज में सामाजिकता को नहीं बढ़ाता है, व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहित करता है, तो वह समाज में लागू करने योग्य नहीं है। इसीलिए, समाज का यह मानना था, कि “हमारा समाज ‘वैज्ञानिक’ हो या न हो, हमारा विज्ञान, जरूर ‘सामाजिक’ होना चाहिए।” आज, इस छोटे से सिद्धांत के पटरी से उतर जाने से ‘विज्ञान’ कितना असामाजिक हो गया है, ये हम देख ही रहे हैं। इस संदर्भ में गुरुजी अपनी देखी, सुनी कई कहानियाँ, कई अनुभव भी सुनाते हैं।
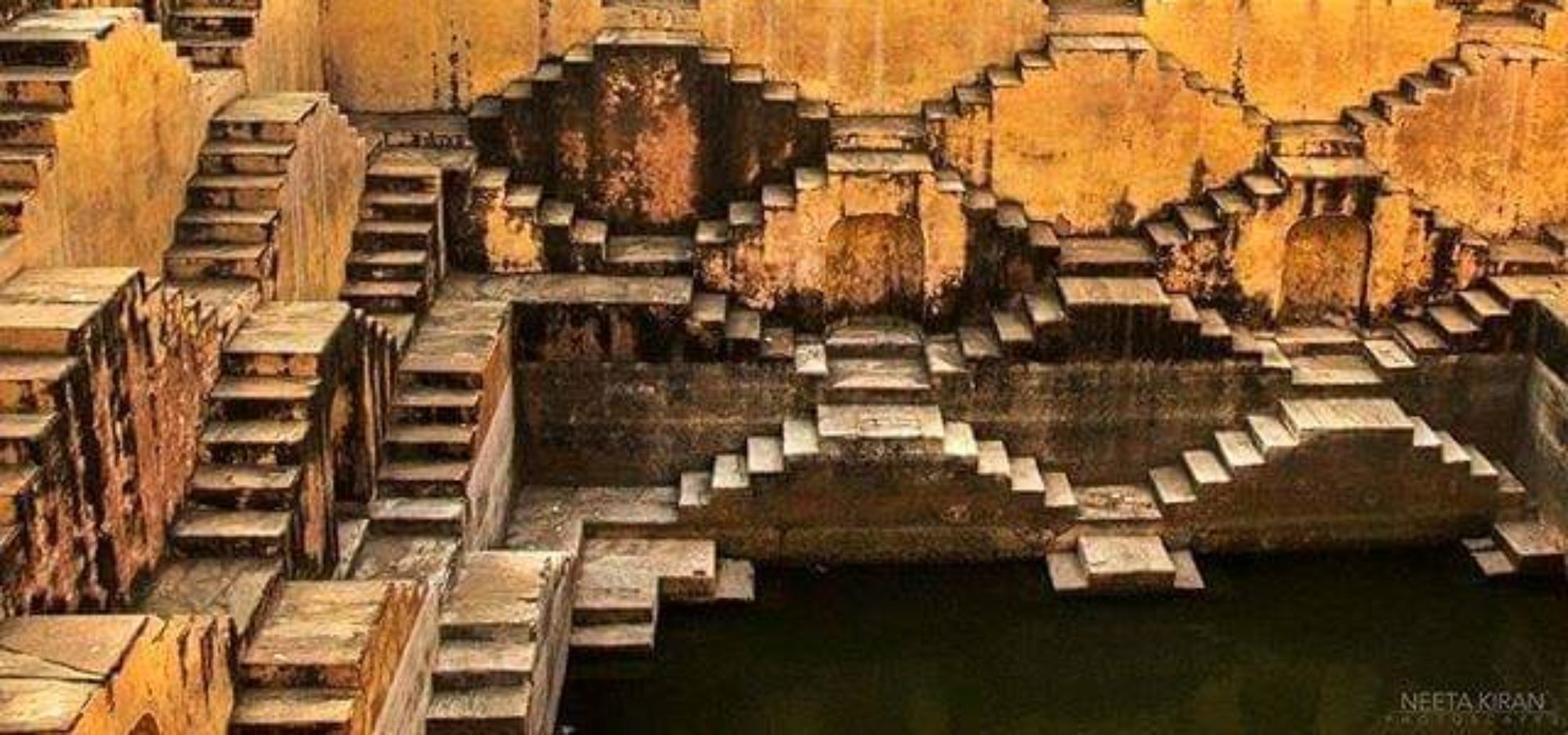

Leave a Reply