धर्मपाल की भाषा आरोप मढ़ने वाली भाषा नहीं है। वे जब भी ब्रिटिश शासन का उल्लेख करते हैं तो न के बराबर व्यक्तिगत होते हैं। उनकी भाषा एक सावधानीपूर्ण प्रयोग से युक्त है। यही बात उन्हें दूसरी धाराओं से जुदा करती है। इसके मूल उनके गांधीवादी चिंतन में हैं। गांधीजी सम्भवतः सबसे ताकतवर ढंग से औपनिवेशिक ज्ञान प्रणाली से लड़े और कभी अंग्रेज़ समुदाय को लेकर व्यक्तिगत नहीं हुए।
यह बात विचार में ले लेनी चाहिए कि ब्रिटिश ज्ञान मीमांसा के दो बड़े पक्ष हैं। पहला है उनका यहाँ शासन करने का व्यावहारिक पक्ष। उनका अधिकतर अध्ययन शासन में सहूलियत के लिए रहा। मस्लन कोई ब्रिटिश अफसर यहाँ की भाषा या शिक्षा प्रणाली का अध्ययन क्यों करे! इसलिए कि वह स्थानीय समाज को समझे और सरलता से प्रशासन चलाए। दूसरा कारण ज़्यादा महीन और पेचीदा है। वह ये कि बड़े से बड़ा ब्रिटिश विद्वान अंततः यूरोपीय दार्शनिक प्रणालियों और क्रिश्चियन धर्मशास्त्रीय ढाँचे में धंसा हुआ था। उसका कालबोध और संसार को देखने का ढंग वह था ही नहीं जो एक पौर्वात्य व्यक्ति का होता।
ब्रिटिश अधिकारी जब भी भारतीय शिक्षा प्रणाली पर टिप्पणियाँ करते हैं, तो उन्हें ध्यानपूर्वक देखने पर हम पाते हैं कि उनकी आलोचना ‘अजनबीपन’ से लिपटी हुई है। धर्मपाल के कार्य में और बर्नार्ड कॉन द्वारा उद्धृत ब्रिटिश अफसरों की आलोचना या प्रशंसा कैसी है! इस सिलसिले में धर्मपाल के शिक्षा संबंधी कार्य को बर्नार्ड कॉन के कार्य के साथ जोड़कर देखने से सम्भवतः कुछ बिंदु मिल पाएँ।
धर्मपाल खुद कोई बहुत ज़्यादा ‘वैल्यू जजमेंट’ नहीं देते। वे ब्रिटिश रिकॉर्ड्स को उद्धृत करते हुए सारणियों और रिपोर्ट्स की मदद से हमारी धारणाओं को धीमे धीमे तोड़ते जाते हैं। उदाहरण के लिए जब वे दक्षिण भारतीय शिक्षा प्रणाली के भीतर शूद्र छात्रों की उपस्थिति का ज़िक्र करते हैं, तो वे यह नहीं कहते कि ये सब वर्तमान जातीय विमर्श को सचेत रूप से सम्बोधित करने के लिए उद्धृत किया गया। लेकिन वो हो जाता है। एक बड़े महीन ढंग से। यही धर्मपाल के कार्य का सौंदर्य है।
भारत में शिल्प की शिक्षा जाति के ढाँचे के भीतर ही थी और यह वंशानुगत तरीके से हस्तान्तरित होती रहती थी। यह कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या फ़िर पॉलिटेक्निक में मौजूद ‘टेक्सचुअल’ ढंग की शिक्षा नहीं रही थी। लौहकार-स्वर्णकार-काष्ठकार से लेकर मूर्तिशिल्प तक के कार्य अधिकतर वंशानुगत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका टेक्स्ट यानी शास्त्र था ही नहीं। शास्त्र तो था – विश्वकर्मापुराण जिसका ज़िक्र एक जगह धर्मपाल भी करते हैं। लेकिन टेक्स्ट की भूमिका कितनी और कैसी थी ये अभी विचार का विषय है। क्योंकि ब्रिटिश पूर्व भारत में होने वाली पढ़ाई के दैनंदिन नोट्स या मिनट्स-संस्मरण हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। दरअसल ये नोट्स-मिनट्स का मामला भी औपनिवेशिक शासन के साथ ही ज़्यादा प्रचलित हुआ।
एक समस्या तो यह रही कि यूरोपीय विद्वान भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को समझने में बहुत कठिनाई अनुभव करते थे। उनमें से अधिकतर ये देखते थे कि भारतीय विद्यार्थी ये जो लम्बे लम्बे सूत्र या पद्य याद करते हैं इनके अर्थ अधिकांश नहीं समझते। फ़िर इस स्मरण की कसरत का अर्थ ही क्या है! कोई कोई ब्रिटिश विद्वान भारतीय पंडितों के साथ कार्य करते हुए उनके तौर तरीकों से परेशान हो जाता था। ये ध्यान रखने की बात है कि बनारस के खुले संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज या दक्षिण में फोर्ट सेंट जॉर्ज सरीखे संस्थानों में ब्रिटिश अध्यापक और भारतीय अध्यापक लगातार संवाद में थे। चूँकि वह एक संक्रमण काल था। भारतीय परम्परागत शालाएं या फ़िर अध्ययन केंद्र हाशिये पर जा रहे थे और उनकी जगह जो नए कॉलेज खुले वे धीरे-धीरे अध्ययन का केंद्र बनते गए। इन नए अध्ययन केंद्रों का पाठ्यक्रम खासकर भाषाओं का पाठ्यक्रम कौन तय कर रहा था! उनके विशेषज्ञ कौन थे! धर्मपाल इन प्रश्नों में बहुत नहीं गए। ये उनका कार्य था भी नहीं। लेकिन बाद में पैदा हुए विमर्श ने इन सब प्रश्नों से निपटने की एक हद तक कोशिश की है। भारतीय पंडित या मौलवी ब्रिटिश विद्वानों के लिए सूचना-प्रदायक मात्र थे। कौनसी सूचना किस ढंग से पुस्तक में शामिल हो ये निर्णय तो अंततः ब्रिटिश विद्वान को ही करना होता था। इस मामले में मुस्लिम विद्वानों की स्थिति हिन्दू विद्वानों से बेहतर नहीं थी। मस्लन मैथ्यू लमस्डेन ने फ़ारसी व्याकरण की पुस्तक के आरम्भ में लखनऊ के मौलवी अल्लाह दाऊद का आभार व्यक्त किया है कि उन्हें अधिकतर सूचनाएँ दाऊद साहिब से मिलीं। लेकिन इन सूचनाओं का ढाँचा तय करने का विशेषाधिकार तो लमस्डेन का ही रहा। इस मामले को धर्मपाल द्वारा उल्लेखित मालाबार में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियों के आंकड़ों के साथ जोड़कर देखें। किस तरह ब्रिटिश शिक्षा के प्रसार के साथ साथ मुस्लिम छात्राओं की संख्या में गिरावट आती गयी। ब्रिटिश ज्ञान प्रणाली के लिए हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही सापेक्षतः पिछड़े समाजों का प्रतिनिधित्व करते थे। ब्रिटिश पूर्व भारत में एक बात ध्यान देने लायक है और वह ये कि इस्लामी शासक स्वयं को साभ्यतिक स्तर पर श्रेष्ठ सिद्ध नहीं कर पाए। चाहे लोक दिखावे के लिए ही सही, उन्होंने खुद को हिन्दू शिक्षा के ढाँचे को नसीहत देने की स्थिति में कभी नहीं पाया। बहुत पहले आये अल बेरुनी की आलोचना भारतीय पंडितों के रूखे व्यवहार को लेकर रही, किन्तु उनके ज्ञान और दर्शन के प्रति तो नहीं रही।
ब्रिटिश विद्वानों के साथ एक नयी स्थिति बनी। वे पुनर्जागरण काल के दार्शनिक हेगेल-काँट-डेविड ह्यूम और न्यूटन-गैलीलियो सरीखे वैज्ञानिकों के तौर तरीकों से लिपटे हुए स्वयं की परम्परा को ग्रीक दर्शन तक ले जाते थे और उन्हें भारत की दार्शनिक प्रणालियाँ अजीब मालूम होतीं थीं। भारतीय शिक्षा अपनी दार्शनिक प्रणालियों की वाहक थी। उसके मंतव्य बहुत अलग क़िस्म के थे। धर्मपाल के कार्य से गुज़रते हुए जब हम भारतीय शालाओं के पाठ्यक्रम को देखते हैं, तो उसमें महाकाव्यों से लेकर व्यावहारिक विज्ञानों और फ़िर एकदम अमूर्त्त प्रतीत होने वाले दर्शन मौजूद थे। एकदम देखने पर यह बात थोड़ी कम समझ आती है, कि कोई पश्चिमी विद्वान इस पर कैसे आपत्ति करेगा। शिक्षा के अनौपचारिक दिखने वाले ढाँचे को ब्यूरोक्रेटिक ढंग के स्कूल-कॉलेजों से कमतर आखिर कैसे माना गया!!
इस सबका संकेत यही लगता है कि पश्चिम के पुनर्जागरण-उपरान्त चिंतन में और हमारे यहाँ के चिंतन में कुछ बुनियादी फ़र्क़ हैं जो शिक्षा को प्रभावित कर रहे थे। उनके यहाँ की शिक्षा औद्योगिक क्रान्ति के बाद बने समाज को लक्षित थी। यूरोप खुद भी एक गहरी उथल पुथल से गुज़र रहा था और वहाँ का औद्योगिक ढाँचा यूरोप की लोकपरम्पराओं को नष्ट करने में रत था। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में औपनिवेशिक शासन के बीज थे और इस अर्थव्यवस्था का मूल था मंडी और मुनाफे की तलाश। क्रिश्चियन धर्मशास्त्रियों के लिए षडदर्शन-भक्तिधारा-लोकआस्थाओं से युक्त भारत को समझाने के लिए क्या नया था! वे संवाद का मन बनाकर आये होते, तो क्रिश्चियन रहस्य धाराओं और भारतीय अध्यात्म में कोई संवाद सेतु बनता, जैसी संकल्पना रोमाँ रोलाँ ने कभी की थी।
ऐसा प्रतीत होता है कि उनका पूरा मन सिखा देने का था। उसी से शिक्षा का उनका मॉडल हमारे परम्परागत मॉडल से टकरा गया। फ़िर सब मानों ढहता ही गया। अन्यथा ये कैसे हुआ कि भारत में जातिभेद समस्या बन गया। फ़िर निरक्षरता समस्या बन गयी। फ़िर कन्याओं का अनुपात बिगड़ता गया। साम्प्रदायिक दंगे होने लगे। यदि किसी समाज को अच्छी शिक्षा मिलने लगी थी तो उसके परिणाम उलटे कैसे आये ! गांधीजी की हिन्द स्वराज उस औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा की आलोचना है और धर्मपाल का कार्य उस शासन से पहले के भारत की तुलनात्मक तस्वीर। धर्मपाल का कार्य इतना बड़ा है कि उसपर पृष्ठ दर पृष्ठ बात की जा सकती है। स्थानाभाव के चलते संकेत भर पर्याप्त होंगे।
(समाप्त)
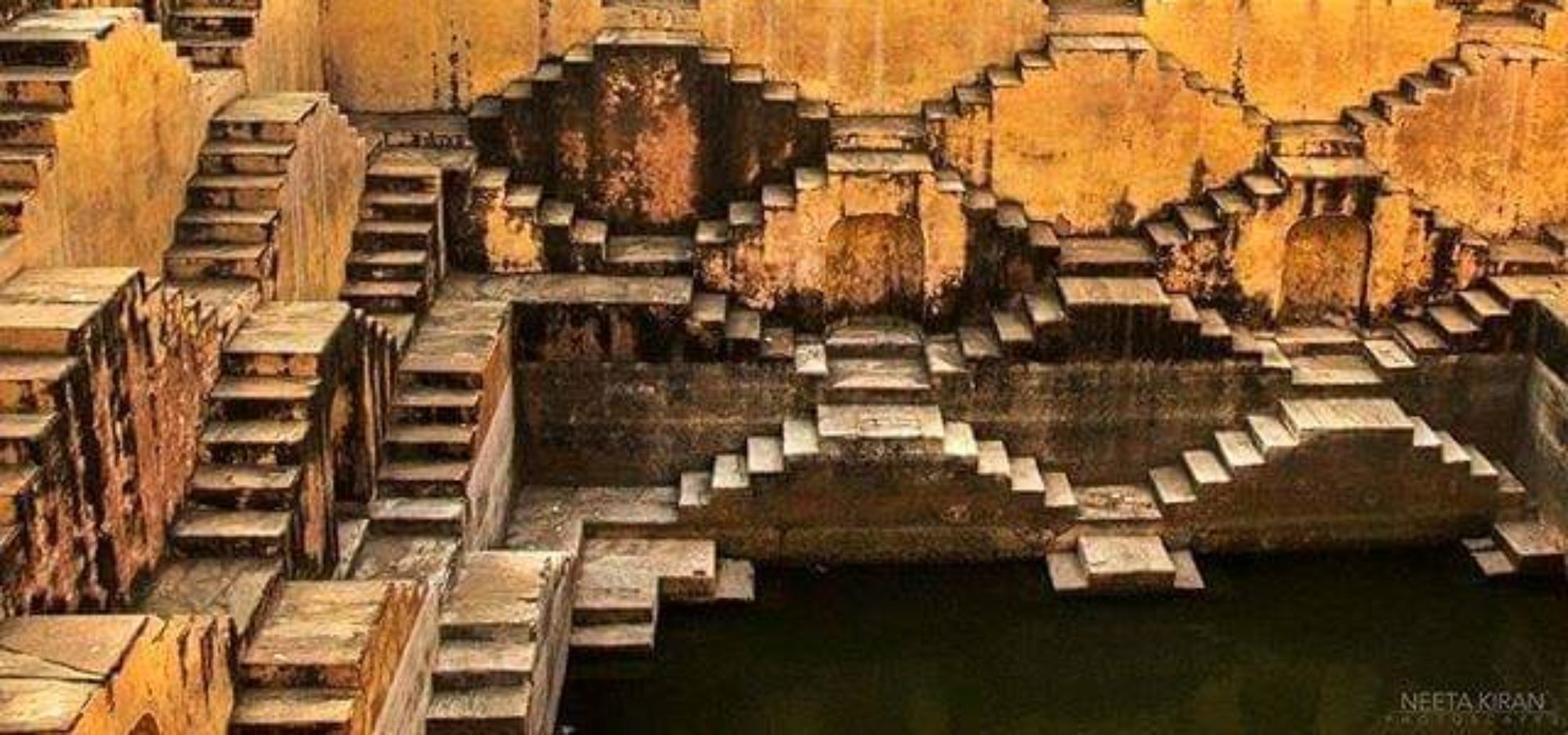


Leave a Reply