बहुत वर्ष पहले की बात है। अश्विन महीना था, नवरात्रि के दिन अष्टमी के रोज सुबह मैं घूमने निकला था। वर्षा के भीगे हुए दिनों के बाद शरद की भोर बड़ी सुहावनी लग रही थी। वातावरण में ताजगी थी। चौड़ी सड़क के दोनों ओर के वृक्ष मेरे परिचित थे। उनमें भी गोल चक्कर के पास के एक नीम के साथ तो मेरा विशिष्ट संबंध था। मेरा यह अनुभव रहा है, कि संतों की तरह वृक्षों का समागम भी गहन मानसिक शांति प्रदान करने वाला होता है।
इस अनुभव में आनंद और रोमांच का संचार करने वाले थे जीवन भगत। भगत प्रज्ञाचक्षु थे। मेरे परिचित नीम के नीचे उनका आसन था। किसीके भी पाँवों की आहट सुनाई देते ही भगवान तुम्हारा भला करे यह एक ही वाक्य उनके मुख से निकलता। बहुत से राही सुना अनसुना करके चले जाते। कोई एक नज़र उस ओर देख कर आगे बढ़ जाता। कोई सहानुभूति की दृष्टि डाल कर चल देता, तो किसी विरल अंतःकरण में समभाव उत्पन्न होने पर भगत की फैली हुई अंजलि में धेला पैसा पड़ता। रोज के आने जाने वाले कई लोगों को भगत उनकी आवाज से पहचान लेते थे। कुछ लोगों के पाँवों की आहट भी उनकी पहचानी हुई थी। उनका वे दूर से ही स्वागत करते।
मेरी नज़र में जीवन भगत सिर्फ अंधे भिक्षुक ही नहीं थे, किसी छोटी कहानी का उपादान बन सकने वाले करुणाप्रेरक पात्र भी नहीं थे। मुझे वो जीवन रहस्य का पार पाने की कोशिश करने वाले जिज्ञासु जीवनयात्री ही मालूम होते, इसके लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था। यह सिर्फ मेरी भावना थी, पर अंतःकरण की स्वयंस्फूर्त भावना सर्वदा प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखती।
आज सुबह भी उन्होंने मेरी आहट पहचान ली। समस्त मुखमंडल को निर्व्याज स्मित से संस्कारित करके भगत ने मेरा स्वागत किया। मैं भी पेड़ के तने से टिकाकर उनके सामने खड़ा रहा। आज मैं और दिनों से कुछ जल्दी ही घूमने निकल आया था। नीम के नीचे भगत के मिलने की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि ये अक्सर नौ बजे के आसपास आते थे। किसी अनजाने झरने की तरह वे न जाने कहाँ से आते थे और न मालूम कहाँ चले जाते थे। अतः कुछ आश्चर्य से मैंने पूछा, “क्यों भगत, आज कुछ जल्दी!”
“हाँ बापू, आज नवरात्रि की अष्टमी है। पावागढ़ जाने वाले यात्रासंघ इसी रास्ते से निकलेंगे। इसलिए जल्दी आ गया हूँ।“ भगत के चेहरे पर स्मित छा गया।
“भगत, आप मुझे बापू न कहा करें। आपकी उम्र और ज्ञान को देखते हुए तो मुझे आपको बापू कहना चाहिए।“ मैंने नम्रता से कहा। “ज्ञान और समझदारी से क्या होता है और जीवन जीने की जानकारी न हो, तो उम्र भी किस काम की?” बापू भगत की आवाज़ में अनुभवजन्य वेदना की झंकार थी। “फिर भी, भगत, आप मुझे भाई ही कहा करें।“ मैंने विनती की।
“तुम्हें उससे खुशी होती हो, तो भाई कहूंगा।“ अत्यंत स्वाभाविकता से भगत ने मेरी बात मान ली। मुझे इससे आनंद हुआ। इस आनंद से अंतर के द्वार खुल गये। अतः मैंने कुछ आत्मीयता से पूछा, “भगत, घर पर रोटी-पानी कौन बनाता है? घरवाली है?”
इस सवाल ने भगत के मुख का स्मित पोंछ डाला। मुझे इससे रंज भी हुआ और संकोच भी। मानो मेरे चेहरे के भावों को पढ़ लिया हो, इस तरह भगत बोले, “भैया, पंद्रह बरस हुए, वह तो मुझे छोड़कर भगवान के दरबार में चली गयी। जिंदा थी तब तक हाथ पकड़ कर मुझे भी मजदूरी करने ले जाती थी। दोनों साथ काम कर के पेट भर लेते थे, पर उसके जाने के बाद सब गड़बड़ा गया। बेसहारा अंधे को कोई मजदूरी के लिए भी नहीं रखता। इसलिए भगवान के नाम पर भरोसा रख कर पंद्रह वर्ष से इसी नीम के नीचे बैठता हूँ। कोई राजीखुशी से कुछ दे सकता है, तो उन्हीं के नाम पर ले लेता हूँ। दसेक साल से तो तुम भी देख ही रहे हो। भाई जाने वाली तो सती थी उसकी याद कर के दिन पूरे कर रहा हूँ।“
इतना कहते-कहते भगत की आँखों से आँसू टपकने लगे। उन्होंने उन्हें पोंछा भी नहीं। उस अकिंचन सदाचारी का मुँह आँसुओं से भीग कर शील के प्रकाश से दमकने लगा। हम दोनों ही मौन रहे। इतने में अंबा माता के संघ की झांझ-नगाड़ों की आवाज ने हमारा ध्यान खींचा।
“भाई, संघ पास आ रहा है।“ भगत ने अब आँसू पोंछ डालें।
संघ का जुलूस गुजरने लगा। सबसे आगे ढोली था। शहनाई उसका साथ दे रही थी। उनके पीछे माता का रथ था। मूर्ति के गले में फूलों का हार था और हाथों में फूलों के गजरे ललाट पर कुंकुम। कुछ लोग जंजीरे पकड़ कर रथ को खींच रहे थे और रथ के पीछे था भक्तों का समुदाय। सब लोग उच्च स्वर से माताजी के भजन स्तवन गा रहे थे, नगाड़े का ताल रहस्यमयता का वातावरण उत्पन्न कर रहा था। स्त्रियाँ माताजी के जवारे हाथों में लिए नवरात्रि के गीत गाती हुई जा रही थी।
ठीक हमारे सामने आते ही रथ चलाने वाले रथी के शरीर में देवी का संचार हुआ। वह हुंकार भरता हुआ सिर धूनाने लगा। उसके लंबे बाल उलझ कर चारों और बिखर रहे थे। आँखें लाल हो रही थी। हाथ की जंजीर से वह अपनी ही पीठ पर कोड़े लगाने लगा। ढोल की आवाज़ बढ़ी। शहनाई के सुर अधिक तीव्र हुए। डमरू डमडमा उठे। रथी और भी जोर से पीठ पर जंजीर के प्रहार करने लगा। इतने में ‘जय हो माता भवनी दया, अंबामाता, दया कहती हुई कुछ स्त्रियां आगे आयी। माता के रथ के सामने आँचल पसार कर क्षमा के लिए गिड़गिड़ाने लगी। रथी ने प्रहार करना बंद किया। स्त्रियाँ आगे बढ़ गयी। इतने में भगत ने कहा, “भाई, मुझे रथ के पास ले चलो।“
मैं उन्हें हाथ पकड़ कर रथ के पास ले गया। भगत ने साष्टांग प्रणिपात किया। रथ के मार्ग की रज सिर पर चढ़ाई; फिर जेब में से सवा रूपया निकाल कर रथी को दिया और कहा, “भैया, कल दुर्गानवमी के दिन मेरी मणि के नाम से माताजी को प्रसाद चढ़ा देना, तुम्हारा पुण्य होगा भैया। मेरा इतना काम याद से कर देना।“ मुझसे बोले, “चलो भाई।“ मैं उन्हें हाथ पकड़ कर नीम तले ले आया। पावगढ़ का संघ आगे बढ़ गया। मैं अवाक् हो गया।
भगत ने कहा, “भाई, हर साल नवरात्रि की अष्टमी को मैं उस सती के नाम से सवा रूपये का प्रसाद संघ के साथ पावागढ़ भेज देता हूँ। खुद तो जा नहीं सकता। भैया, वह तो सती थी, सो चली गयी।“ भगत के मुख पर स्मृति की रेखाएँ उभर आयी, उनमें से स्मित फूटा और उनका पूरा मुखमंडल आनंद से प्रफुल्लित हो उठा।
उन्हें उस सुख में छोड़ कर मैं वापस लौटा, पर हृदय पर मानों कोई कोड़े बरसा रहा था। मैं अपने आपको अंतर्निष्ठा का परम उपासक समझता था, परंतु आज मालूम हुआ कि वह निष्ठा विकलांग थी। अपाहिज थी। आज भगत को देखते ही मैं सोचने लगा था, कि आज वह इसलिए जल्दी आये हैं, कि पावागढ़ जाने वाले संघ के यात्रियों से रोज की अपेक्षा दो चार पैसे अधिक मिल जायेंगे, परंतु उनके जल्दी जाने का कारण तो था प्रिय पत्नी की स्मृति में संघ के द्वारा माताजी को सवा रुपये का प्रसाद भेजने की अंतरेच्छा। मैंने अपनी आँखों से देखा और हृदय से अनुभव किया कि उसके फलीभूत होने पर भगत की स्नेहभावना किस कदर धन्य हो उठी थी। मैं अपने हीन विचार के कारण लज्जित हो उठा।
विचार आया, कि मनुष्य को अपनी सन्निष्ठा का भी कैसा भव्य अहंकार हो सकता है और उसके प्रवाह में बह कर वह दूसरे के हेतुओं को किस हद तक गलत समझ सकता है।
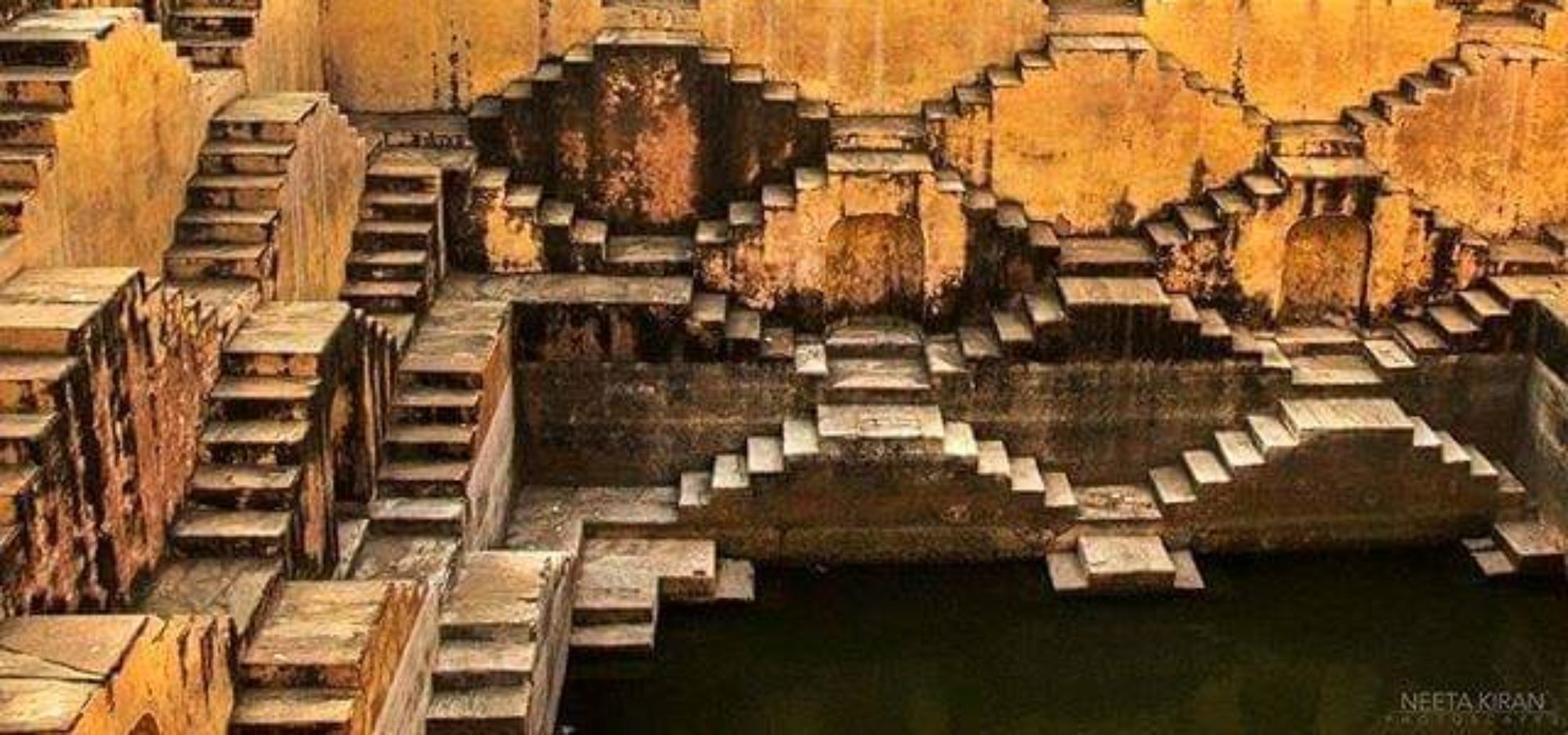

Leave a Reply