अब हमारे सामने प्रश्न ये है, कि भारतीय चित्त की इस मूल भूमि को किसने सबसे सटीक पहचाना! स्वाभाविक उत्तर होगा, कि गांधीजी ने। इसीलिए वे विदेशी कपड़ों की होली जलवाकर जब विदेश गए, तो उन मज़दूरों से मिले जो उन कपड़ों को बनाते थे। गांधीजी के लिए प्रक्रिया केंद्र में थी – व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं।
इस सारी प्रक्रिया को धर्मपाल अपनी तरह से पकड़ रहे थे और कोई हैरानी नहीं है, कि गांधीजी बार बार धर्मपाल के चिंतन में अलग अलग मौकों पर प्रकट होते रहते हैं, हालाँकि ये एक विषयांतर होगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है, कि क्या गांधीजी के हत्यारे के मन में भी कोई द्वंद्व उपस्थित नहीं हुआ होगा! क्या उसने बाद में कभी इस बात पर पश्चाताप व्यक्त किया, कि निहत्थे व्यक्ति पर हथियार उठाना भारतीय युद्ध के नियमों के ही विरुद्ध है। उसकी स्वयं की मनोवैज्ञानिक भूमि क्या थी। फिलहाल इतना ही संकेत पर्याप्त होगा, कि हिंसक व्यक्ति का बचपन बहुत उलझनों से भरा होता है, जो बाद में जाकर ग्रंथियों के तौर पर उभरता है।
धर्मपाल यदि होते तो उनसे इस बाबत पूछा जा सकता था। वे शायद इतना ही कहते, कि – अधिक गहराई से संतुलित होकर अध्ययन मनन करो।
‘धर्मपाल कुछ यादें’ में संग्रहित एक अन्य आलेख ‘द रेनेसाँ मैन’ [जिसका भावानुवाद ‘पुनर्जागरण का पुरोधा पुरुष’ होगा] में सुश्री अनुराधा जोशी जी ने कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदुओं की ओर संकेत किया है, जो धर्मपाल के अध्येताओं के लिए मनोवैज्ञानिक स्तर पर विचारणीय है। धर्मपाल जी भारतीय साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियों में प्रेमचंद की बनिस्बत शरतचंद्र की ओर अधिक उन्मुख हुए। उनके अनुसार प्रेमचंद के लेखन में भारतीय समाज की आतंरिक शक्तियों का पर्याप्त चित्रण न होकर दरिद्रता – विपन्नता की ओर अधिक ध्यान रहता था, जो मात्र करुण-क्रन्दन [धर्मपाल जी के शब्दों में ‘रोना पीटना’] मात्र बनकर रह जाता।
निश्चित ही यह एक गंभीर बिंदु है, हालाँकि मेरे विचार से ऐसा नहीं है, कि शरतचंद्र में भी ‘करुण-तत्त्व’ एकदम अनुपस्थित हो। देवदास नामक कृति इसका बड़ा उदाहरण है। स्वयं को नष्ट कर देने पर उतारू एक प्रेमी की यह करुण-कथा भारतीय सिनेमा में दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान सरीखे अभिनेताओं ने बारम्बार निभायी और ख्याति अर्जित की। दरिद्रता और करुणा समाज का सत्य है। शक्ति और गौरव भी समाज का दूसरा सत्य है। मेरे मत से किसी व्यक्ति को एक पक्ष अच्छा लगता है तथा किसी को दूसरा। भारत का सत्य इन दोनों सत्यों का जोड़ है।
भारत को प्रेमचंद्र का कठोर निर्मम सच भी चाहिए तथा बंकिमचंद्र – शरतचंद्र – जयशंकर प्रसाद का आत्मगौरव भी। दूसरे शब्दों में कहें, तो महाभारत तथा रामायण दोनों से मिलकर ही हमारी दृष्टि पूर्ण होती है। एक भाइयों के बीच कठोर निर्मम युद्ध तथा दूसरा भाइयों के बीच प्रेम का अतुलनीय उदाहरण। हम इनमें से एक को चुन सकते हैं, लेकिन वह चुनाव एकांगी होगा। परमात्मा की सृष्टि में दिन भी होता है और रात भी। शायद प्रेमचंद रात के चितेरे हैं और शरत दिन के।
अहोरात्र तो लेकिन दोनों से मिलकर बनेगा न! ख़ैर, आगे अनुराधा जी ने स्त्रीमुक्ति आंदोलन का उदाहरण लेते हुए धर्मपाल के कार्य को लेकर एक गुत्थी की ओर संकेत किया तथा धर्मपाल से हुए उनके संवाद का उल्लेख भी। पूरी बारीकी के लिए उस संस्मरण को मूल अंग्रेज़ी ही में पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन फ़िर भी संक्षेप में वह भाव के स्तर पर कुछ यूँ था। शोषण की कथाएँ आमतौर पर मुक्ति की कामना से शुरू होती हैं, लेकिन अंततः ‘विक्टिम सिंड्रोम’ [स्वयं को सदा पीड़ित समझने का रोग] में तब्दील हो जाती हैं। स्त्रीवादी चिंतक महिलाएँ आमतौर पर पुरुषों के आचरण को लेकर शिकायत करने तथा पुरुषों को ज़िम्मेदार ठहराने मात्र से ही संतुष्ट हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार कहीं ऐसा तो नहीं कि हम केवल ‘पश्चिम’ को ही दोषी ठहराते जाएँ !
“After all those years, I felt the same way about Dharampalji’s writings. In the seventies, the feminists had blamed and complained about the man : this time the blame and complaints were the same with a small difference – instead of men the target was the west”. (‘The renaissance man’ पृष्ठ – 84, धर्मपाल कुछ यादें )
इसके उपरान्त केवल ‘पश्चिम’ को दोषी मानने से आने वाली मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों का ज़िक्र हुआ। पूरे पैराग्राफ़ यहाँ उद्धृत करना स्थानाभाव के चलते सम्भव नहीं, परतु ये सुझाव है, कि मूल पुस्तक को अवश्य देखा जाये चूंकि ये पूरा ही अध्याय महत्त्वपूर्ण है।
जब ये बिंदु धर्मपाल जी को कहे गए, तो उन्होंने इस सारी आलोचना को मुस्कुराकर स्वीकार किया। उन्होंने कहा, कि ‘मैं तो बहुत रद्दी लिखता हूँ’!
“He listened attentively, withstood my criticism with a smile and completely disarmed me by saying that of course he understood my response because he knew he wrote badly.”
धर्मपाल जी के व्यक्तित्व का बहुत ध्यान देने योग्य पक्ष है, कि कैसे आलोचना को खुलकर स्वीकार किया जाए तथा संवाद के मार्ग खुले रखे जाएँ। आज के समय में जबकि हल्की सी आलोचना हमें उत्तेजित कर देती है – तब धर्मपाल जी की उस सरल मुस्कुराहट की याद सम्भवतः मार्ग प्रशस्त करे।
मेरे विचार से धर्मपाल जी के चिंतन में ‘पश्चिम’ निजी स्तर पर नहीं आया है। उनके यहाँ पश्चिम की नहीं, अपितु औपनिवेशिक प्रक्रिया की आलोचना हुई है, लेकिन उसी औपनिवेशिक प्रक्रिया का जन्म ‘पश्चिम’ में हुआ, इसलिए हम सभी धर्मपाल के कार्य का अर्थ पश्चिम की आलोचना लगाते हैं। उस अर्थ का धर्मपाल जी ने भी कभी सीधा प्रतिवाद नहीं किया।
मेरे विचार से उनकी पुस्तकों में सम्पूर्ण पश्चिम है भी नहीं। ठीक से देखें, तो वहाँ केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के साथ भारत के संबंधों का ज़िक्र है। वहाँ जर्मन ज्ञान प्रणाली अथवा फ्रेंच दर्शन या फ़िर इटैलियन परम्परा आदि की कोई विधिवत आलोचना नहीं है। अतः वह एक ख़ास औपनिवेशिक संबंधों की आलोचना है, लेकिन जब वे औपनिवेशिक संबंधों की आलोचना करने चले तो स्वभावतः ‘पश्चिम’ की संरचना का सवाल तो आ ही गया होगा, कि फ्रेंच-जर्मन-डच-स्पैनिश-इटालियन परम्पराओं में भेद होने के बावजूद क्या कुछ समान है और वह समानता भारत के साथ कैसे उलझती है। इसलिए भाषा के स्तर पर कभी ‘पश्चिम’ आ जाता है तो कभी ‘औपनिवेशिक प्रणाली’! तकनीकी लिहाज़ से ‘औपनिवेशिक प्रणाली’ अधिक सटीक है और भाव के स्तर पर ‘पश्चिम’ भी।
[क्रमशः]
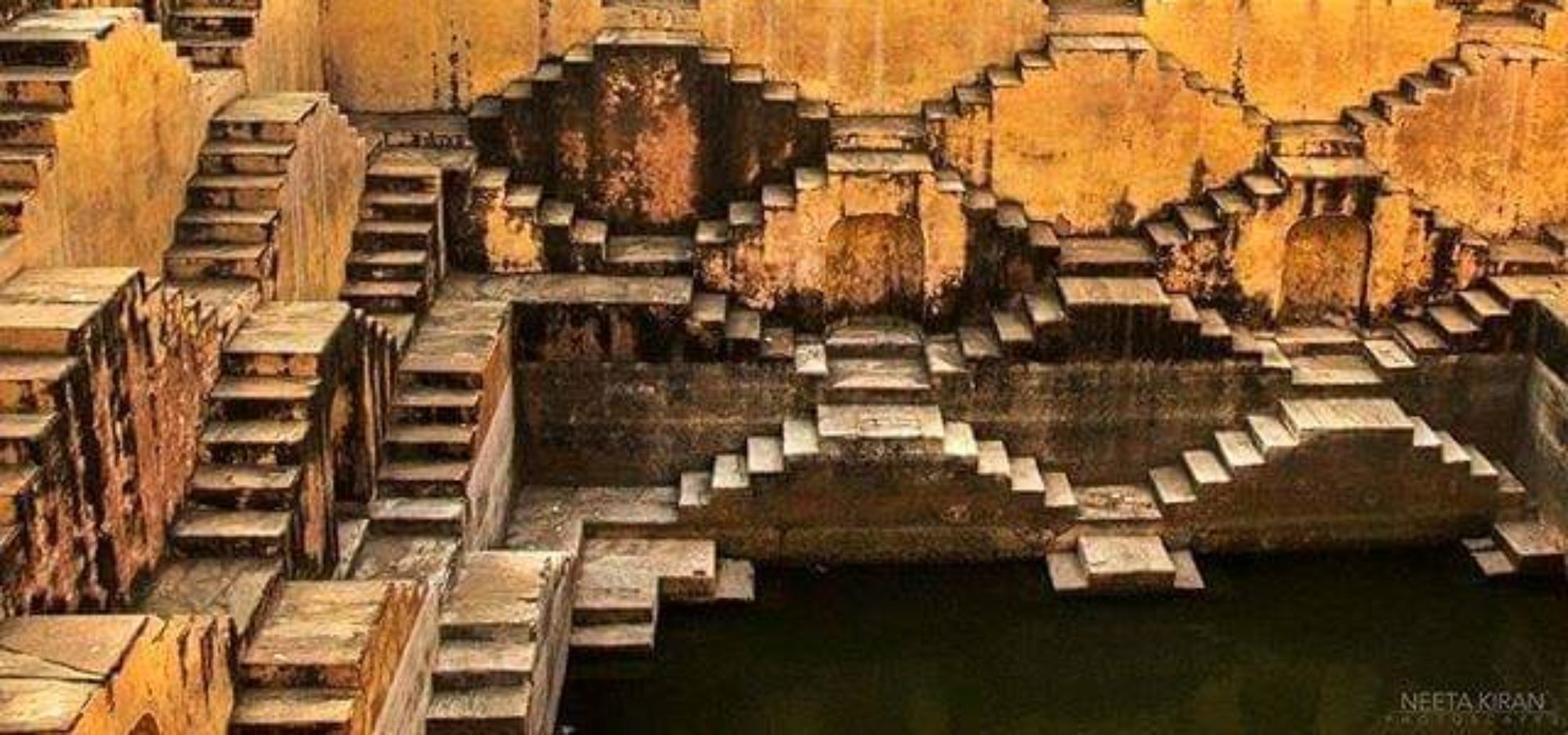





Leave a Reply