इस पूरे कोरोना प्रकरण के दो प्रमुख उप-प्रकरण सामने आ रहे हैं । एक तो ‘कोरोना वायरस’ प्रकरण और दूसरा ‘लॉक-डाउन’ प्रकरण । ‘कोरोना वायरस’ उप-प्रकरण से जो सीख मिलेगी, सो मिलेगी, पर यह ‘लॉक-डाउन’ उप-प्रकरण समाज व्यवस्थाओं के बारे में ढेरों सीख देते जा रहा है । लॉक-डाउन के बाद चारों ओर ‘हाथ कँगन को आरसी क्या’ वाली स्थिति हो गई है । न जाने कितने दशकों से पर्यावरणविद जो कहते आ रहे हैं, कुछ-एक अर्थशास्त्री जो कह रहे हैं, जीवन की शैली को समझने वाले ढेरों दार्शनिक कह रहे हैं, वह सब हम यथार्थ में अपनी आँखों से होता हुआ देख पा रहे हैं ।
मात्र 30-40 दिनों के लॉक-डाउन ने हमें दिखा दिया है कि हमारे विकास की दिशा कितनी एकांगी और गड़बड़ है । चाहे वह पर्यावरण का मामला हो, पञ्च महाभूतों के रख-रखाव का मामला हो, प्रकृति में पेड़-पौधों को, अन्य जीव-जन्तुओं को भयमुक्त जीवन जीने देने का मामला हो, गरीबों का मामला हो, अमीरी-गरीबी में बढ़ते फासले का मामला हो, (जरुरत के बदले) इच्छाओं का मामला हो, (सुख के बदले) भौतिक सुविधाओं का मामला हो, (धीमी, सुकून वाली जिन्दगी के बदले) तेज दौड़ती-भागती जिन्दगी का मामला हो, हमारे विकास की गाड़ी एकदम एकांगी ही चली है ।
मेरी जो समझ अभी तक बनी है, उसके अनुसार हमारे इस एकांगी विकास के मूल में बड़े-बड़े, दैत्याकार उद्योग धन्धों और विशालकाय कॉर्पोरेट/कम्पनियों वाली व्यवस्था है । यह पूरी व्यवस्था कैसे काम करती है, यह जानना बहुत रोचक है । जैसा कि हम लॉक-डाउन के कारण देख पा रहे हैं कि हमारा बाज़ार ‘बिना जरुरत’ की ऐसी सैकड़ों-हजारों चीजों से भरा पड़ा है, जिनके बिना भी हम बहुत आसानी से पिछले एक-डेढ़ महीने से जी पा रहे हैं । इस कॉर्पोरेट वाली व्यवस्था में पहला काम तो ‘बिना जरुरत’ का सामान/सेवा बनाने की सोचना है । फिर ‘बिना जरुरत’ का सामान बनाने / सेवा प्रदान करने के लिए बड़े-बड़े उद्योग लगाये जाते हैं, कम्पनियाँ बनाई जाती हैं। । इन विशालकाय दैत्यों को खड़ा करने के लिए सैकड़ों-हजारों लोगों को विस्थापित करके, न केवल उनकी आजीविका को नष्ट किया जाता है, बल्कि उनको उनकी अपनी पूरी संस्कृति से ही बेदख़ल करके उनसे उनकी जमीन छीन ली जाती है । उन ‘बिना जरुरत’ के सामानों के निर्माण के लिए सैकड़ों-हजारों किलोमीटर दूर से उसका कच्चा-माल, उपकरण, तकनीक लाना । इन उद्योगों/कम्पनियों को चलाने के लिए लोगों को (अच्छे पैसों वाली नौकरी, आदि का लालच देकर) उनके गाँवों, कस्बों, उनकी संस्कृति से दूर करके प्रवासी मजदूर बनाया जाता है (जिनमें तथाकथित कंप्यूटर, एकाउंटिंग, प्रबंधन, आदि कामों से जुड़े तगड़ी तनख्वाह पाने वाले पढ़े-लिखे मजदूर भी शामिल हैं) । आज इन विशालकाय उद्योगों/कारखानों/कम्पनियों के कारण हमारा पूरा का पूरा समाज ‘संचार जाति’ वाला बन गया है । फिर, ‘बिना जरूरत’ के इस तैयार माल/सेवा को नाहक ही सैकड़ों, हजारों किलोमीटर दूर-दूर ले जाकर जबरदस्ती (विज्ञापन, सेल्स, सेल प्रमोशन आदि के माध्यम से) लोगों को बेचा जाता है । और, जिनके पास इनको खरीदने की औकात न हो, संसाधन न हों, उनको बैंकों आदि से ऋण/लोन दिलवाकर उनसे सामान खरीदवाया जाता है आदि-आदि ।
बड़े-बड़े उद्योगों के बाद, पर्यावरण की खराबी का, प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण रोड-रेल-हवाई ‘ट्रांसपोर्टेशन’ की व्यवस्था है । हमने शायद ही कभी सोचा है कि बड़े-बड़े कारखानों के बदले छोटे-छोटे कारखानों/ उद्योगों/ कम्पनियों वाली व्यवस्था हो, तो उनके कच्चे और तैयार दोनों तरह के मालों के इतने व्यापक परिवहन की आवश्यकता ही नहीं होगी । बड़े-बड़े उद्योगों/कम्पनियों के द्वारा (उनमें काम करने के लिए, और उनके लिए जरूरी सहयोगी व्यवस्थाओं में काम करने के लिए) इतनी वृहत संख्या में लोगों के विस्थापन की आवश्यकता ही न हो, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी लगभग न के बराबर आवश्यक होगा । हमारे शहर, जो आज पर्यावरण, प्रदूषण, क्वालिटी-टाइम की उपलब्धता, रहन-सहन स्तर, स्वास्थ्य आदि ढेरों पैमानों में बद से बदतर होते जा रहे हैं, जनसंख्या के दबाव में अधमरे हुए जा रहे हैं, उनकी स्थापना और उनके फैलाव के मूल में भी ये बड़े उद्योग-धन्धे और कम्पनियाँ ही हैं । गुरूजी श्री रवीन्द्र शर्मा जी के शब्दों में हमारा पूरा समाज ‘संचार जाति’ वाला समाज हो गया है । अब तो खैर, इन फैलते हुए शहरों की अपनी खुद की जनसंख्या और उसके लिए जरूरी सहयोगी सेवाएँ ही उनके फैलने का कारण बन रही हैं । पर इनके मूल में बड़े उद्योगों और कम्पनियों वाली व्यवस्था ही है । एक सीमा से आगे जाकर ‘इकॉनोमी ऑफ़ स्केल’ की संकल्पना एक पलटवार करती है, आज हमारी इस दुर्दशा से यह एक बार पुनः सत्यापित हो रहा है ।
संचार जाति वाला समाज
जब तक यह बड़े उद्योगों/कम्पनियों वाली व्यवस्था है, तब तक भला क्या हो सकता है?
नौकरी वाली इस व्यवस्था में अपने अनुसार कुछ भी कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असम्भव है। वैसे भी हमारा जो कुछ अभी तक बचा हुआ है — संस्कार, पूजा-पाठ, त्यौहार, दान-दक्षिणा आदि — ये सब केवल परम्परागत व्यवसायी, कारीगर और किसान परिवारों में ही बचा है। नौकरीशुदा लोग तो कब के इन सब से अलग हो गए हैं, या होते जा रहे हैं। या फिर कुछ थोड़ा-बहुत कर भी रहे हैं, तो इन सबको परम्परा, शौक, स्टेटस या किसी अनजाने से डर के कारण ढो रहे हैं कि यदि ये सब नहीं किया तो न जाने कौन-सा अनिष्ट हो जाएगा। बड़ी कम्पनियों द्वारा पोषित अलग तरह की नौकरशाही ने हमारे समाज को एक संचार जाति वाले समाज में तब्दील कर दिया है। आज कोई भी व्यक्ति अपने गाँव और अपने शहर में रहकर जी नहीं पा रहा है। हरेक को काम और कैरियर की तलाश में अपना गाँव और शहर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। दसवीं-बारहवीं की पढ़ाई के- लिए या उसके बाद घरों से निकली सन्तान रोजी-रोटी और आजीविका के लिए शायद ही अपने घर वापस आ रही है। बहुत ही कम सन्तानें अपने बाप-दादों के बनाए घरों में रह रही हैं। हर कोई अपना स्वयं का घर बना रहा है। आज हर कोई अपनी जिन्दगी अपने से आरम्भ कर रहा है और अपने पर ही खत्म कर रहा है। सदियों से पीढ़ियों से संचित और पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रदान किए जाने वाले ज्ञान की, परम्पराओं के निर्वहन की इस समाज को कोई आवश्यकता नहीं है।
जब समाज संचार जाति वाला हो जाता है, तो इसकी जरूरतें बहुत कम हो जाती हैं। बच्चों की दसवीं-बारहवीं तक की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा स्कूल मिल जाए, बीमार पड़ने पर नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधाएँ, खाने के लिए दो-चार रेस्टोरेण्ट और दैनिक जरूरतों के लिए छोटा-सा बाजार मिल जाए, तो बहुत है। न तो इसको साहित्य की जरूरत होती है, न संगीत की, न कला की, न समाज की, न पूजा-पाठ की, न व्रतों की, न त्योहारों की और न ही अन्य किसी सामाजिक कार्यक्रमों आदि की। संचार जाति वाले समाज की न तो कोई सभ्यता होती है, न ही कोई संस्कृति और न ही कोई परम्परा। अध्यात्म, कला, सामाजिक कार्यक्रम, पूजा-पाठ, संस्कार, त्योहार, दान-दक्षिणा तथा आपसी मेल-मिलाप के लिए न तो उसके पास समय होता है और न उसकी कोई जरूरत महसूस होती है।
अपनी संस्कृति, परम्पराओं से कटे ऐसे समाज में लोगों को 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम कराना आसान होता है। छोटे शहरों, कस्बों का वहीं रहकर नौकरी करने वाला आदमी, साल में 8-10 दिन की छुट्टी तो किसी न किसी की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए ले ही लेता है। नाते-रिश्ते, पास-पड़ोस, मित्र, मित्र के परिवार आदि में किसी न किसी का, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। शादियाँ चूँकि शाम-रात को होने लगी हैं, इसीलिए उसकी छुट्टी बच जाती हैं, फिर भी 5-7 दिन की छुट्टी तो नजदीकी लोगों की शादी के लिए भी कोई भी आदमी लेता है। लेकिन बड़े शहरों में रहने वालों को इस तरह की छुट्टी की जरूरत ही नहीं होती है। उनको सामाजिकता, सामाजिक जीवन से लेना-देना नहीं होता है। वह तो चौबीसों घंटे खट-खटकर केवल काम करना जानते हैं। नहीं तो कभी हमारे दिन के 24 घंटों का बहुत ही बढ़िया विभाजन हुआ करता था। परमात्मा के दिए 24 घंटों में 8 घंटे तो सोओ, खाओ, पिओ, नित्य क्रिया-कर्म करो। 8 घंटे आजीविका के लिए दो और बाकी के 8 घंटे अपनी सामाजिक और आध्यात्मिक जिन्दगी जिओ। यदि, सामाजिक और आध्यात्मिक जिन्दगी ही नहीं जी सकते हैं, तो फिर काम करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। बड़े-बड़े उद्योगों, कम्पनियों वाली व्यवस्था ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है।
- स्व. श्री रवीन्द्र शर्मा (गुरूजी)
सौभाग्य से आज ‘लॉक-डाउन’ के कारण हम हमारे जीवन में घुस आई इन बिना विशेष जरूरत की चीजों को देख पा रहे हैं, जो पहले रोजाना दिखते हुए भी अदृश्य थीं । इनका भलीभांति आकलन कर पा रहे हैं कि भला इनकी जरूरत कितनी थी – क्या किसानों, कारीगरों द्वारा प्रतिपादित छोटे उद्योगों वाली व्यवस्था में हम नहीं जी पाते? गौरतलब हो कि वर्तमान लॉक-डाउन में ‘जरूरत’ की सारी आपूर्ति इन्हीं लोगों से हो रही है । ‘बिना जरुरत’ का सामान बनाने वाले उद्योग, कम्पनियाँ लगभग पूरी तरह से बन्द पड़े हैं, और उनके बिना भी हमारा सब-कुछ आसानी से चल रहा है ।
इतना सब कुछ सीधे-सीधे अपनी आँखों से देखने के बाद भी हम अपने आपको, अपनी जीवन-शैली को नहीं बदल पाये, तब तो भगवान ही हमारा मालिक है । आज जरूरत है कि हम पूँजीपतियों, वर्तमान अर्थशास्त्रियों के बिछाये हुए मायाजाल को समझें । ‘इकॉनोमी ऑफ़ स्केल’ की सीमाओं को समझें । इस अवसर का फायदा उठाकर स्वयं कुछ आकलन करें, अपना मोहभंग करें । अन्य सभी के सहयोग से बड़े कारखाने, बड़ी-बड़ी कम्पनियों के बनाये भ्रम-जाल को तोडें और किसानों, छोटे, घरेलू, कुटीर, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों वाली व्यवस्था को अपने-अपने स्तर पर प्रोत्साहित करते चलें । सभी कुछ चीजों के लिए सरकार पर निर्भर रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है । आज के समय में तो और भी नहीं क्योंकि आज की सरकारें भी तो बड़े-बड़े उद्योगपति ही चला रहे हैं ।
– आशीष गुप्ता
५ मई, २०२०
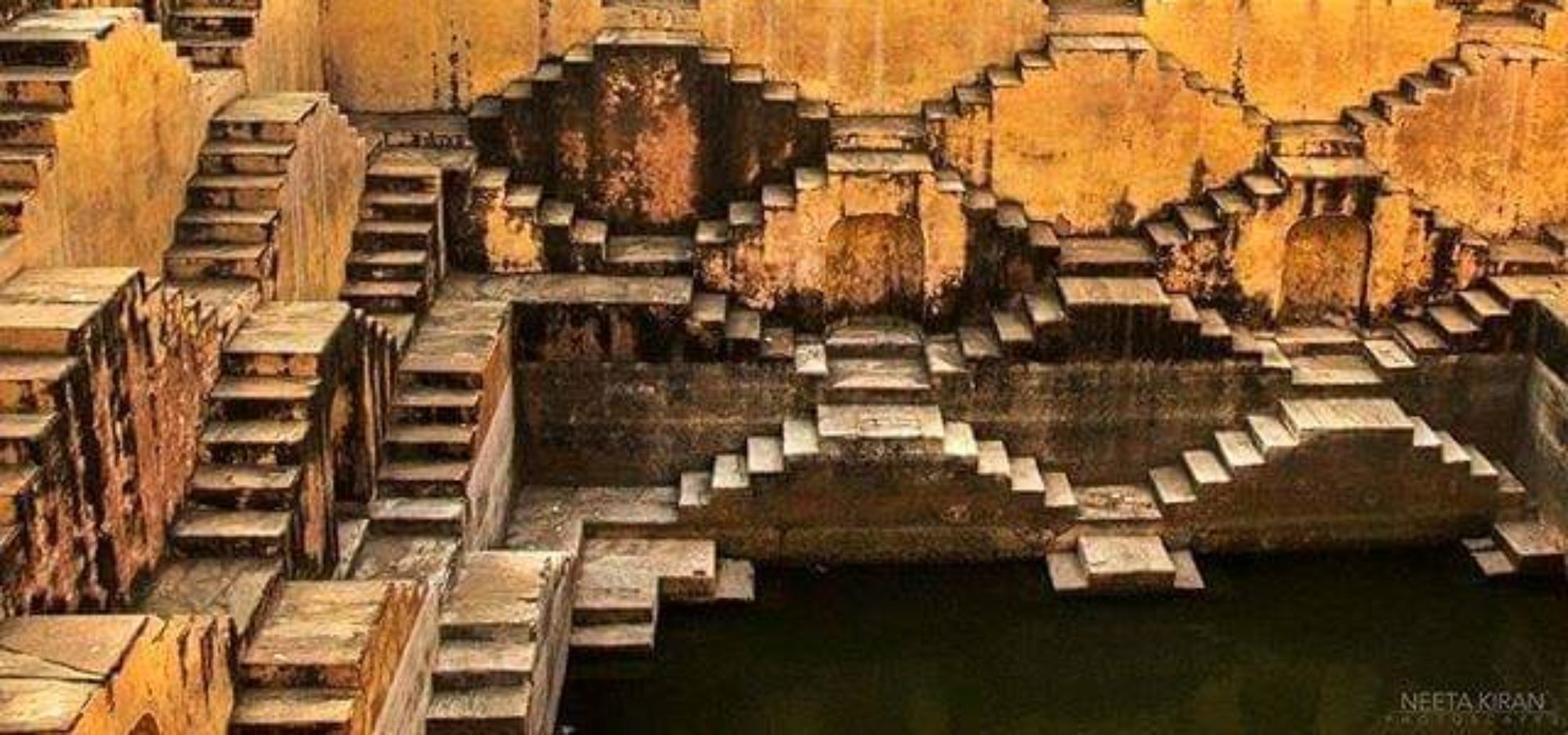

Leave a Reply