(गुरुजी श्री रवीन्द्र शर्मा जी के साथ की बातचीत के आधार पर)
सामाजिक अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में हमारे समाज में वर्तमान आधुनिक समाज की तरह ‘धन की अर्थव्यवस्था’ न होकर ‘सहयोग की अर्थव्यवस्था’ रही है। जिस तरह आजकल समाज में ‘पैसों’ के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, उसी तरह किसी समय हमारे समाज में ‘आपसी सहयोग’ के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता था।
आजकल तो हर सारी चीज पैसों के ऊपर निर्भर करती है। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही धन पर आधारित होकर रह गई है। शादी-विवाह, जन्म-मृत्यु संस्कार आदि सभी सामाजिक कार्यक्रमों में पैसों के दम पर भोजन (बनाने, परोसने, उठाने, समेटने, बर्तन धोने आदि), आवास (होटल, लॉज आदि), कार्यक्रम स्थलों (होटल, सामुदायिक स्थल, मेरिज गार्डन आदि), साज-सजावट आदि में ‘पैसा फेंक तमाशा देख’ की तर्ज पर सारी व्यवस्थाएँ होती हैं, उसी तरह कभी समाज में ये सारी व्यवस्थाएँ पैसों के दम पर नहीं बल्कि ‘आपसी सहयोग’ के दम पर होती थीं। रिश्तेदारों, पड़ोसियों, मित्रों आदि की सहयोगात्मक व्यवस्था के कारण, इन जैसे बहुत से कामों के बारे में सोचना तक नहीं पड़ता था, बस निश्चय करने की जरूरत होती थी। सभी लोग, निर्धारित कार्यक्रमों से बहुत पहले स्वयं घरों में आकर, खड़े रहकर ये सारे काम करते, करवाते थे।
कुछ समाजों में एक ही घर में सभी का भोजन-पानी बनता था, तो कुछ ऐसे भी समाज थे, जहाँ शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों में हर घर से रोटियाँ, चावल आदि बनकर शादी वाले घर आ जाता था। सभी वहीं एक साथ बैठकर भोजन करते थे।
इन महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों और जिम्मेदारियों पर ही नहीं बल्कि ‘गृह निर्माण’ जैसे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण काम भी ‘आपसी सहयोग’ से बहुत ही सहजता से निपट जाते थे और ‘गृह निर्माण’ जैसे कभी कभार होने वाले कुछ महत्वपूर्ण और सामाजिक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन के अन्य कार्यक्रम जैसे ‘कृषि’ आदि भी बिना किसी मज़दूरी के ‘आपसी सहयोग’ से ही होते थे। गाँव के सभी लोग, जिसका घर बनना होता था, वहाँ पहले से ही निश्चित दिन पर पहुंचकर, मिलकर उस व्यक्ति का घर बनवा देते थे। घर बनने के बाद भी हर साल होने वाली कबेलू वाले छतों की मरम्मत भी गाँव के लोग आपस में मिल-बांटकर कर लेते हैं। इसी तरह खेती का सारा काम भी सभी लोग आपस में मिल-जुलकर करते थे। जिसके घर काम लगता था, उसकी जिम्मेदारी मात्र यह होती थी, कि उस दिन का भोजन उसके घर बनता था। भोजन भी सभी लोग आपस में मिलकर ही बनाते थे।
बिना मज़दूरों वाली व्यवस्था:
गुरुजी बताते हैं, कि हमारे ग्रामीण इलाकों में तो आज से 40-50 साल पहले तक भी ‘मज़दूरी’ नाम की कोई चीज नहीं थी। हमारी अर्थव्यवस्था में ‘आपसी सहयोग’ के विस्तार को इसी बात से समझा जा सकता है, कि हमारा पूरा का पूरा समाज बिना मज़दूरों के, केवल ‘आपसी सहयोग’ के दम पर ही बहुत सहजता से चला करता था। और न केवल चला करता था बल्कि ‘सोने की चिड़िया’ तक बन पाया था।
बिना दुकानों वाली व्यवस्था:
‘सहयोग वाली अर्थव्यवस्था’ ही मुख्य कारण था, कि हमारे गांवों में आज से 40-50 साल पहले तक भी कोई दुकान नहीं लगने दी गई थी। गुरूजी बताते हैं, कि ‘मज़दूरों’ की तरह ही हमारे समाज में एक जगह बैठकर लगने वाली ‘दुकानें’ भी नहीं थीं। हर कारीगर का घर ही उसकी दुकान हुआ करता था। ‘दुकान’, ‘दुकान’ न होकर ‘घर’ होने के कारण उससे ‘व्यापार’ न होकर, ‘सहयोग’ ही हुआ करता था।
इन दुकानों / घरों / कारखानों आदि से ‘मोल / खरीदी-बिक्री’ किसी एक वस्तु / उत्पाद का न होकर, साल भर की जरूरत का हुआ करता था। इसीलिए, उन वस्तुओं का अपना एक ‘दाम’ ही नहीं होता था। घर की जरूरतों वाली इन चीजों का अपना कोई ‘मोल’ नहीं होता था, क्योंकि हर कारीगर से पूरे परिवार की, पूरे साल भर की जरूरत के हिसाब से लेन-देन होता था।
इस पद्धति का सबसे सुखद पहलू यह होता है, कि हर बार-बार छोटी-छोटी चीज की खरीदी-बिक्री के समय होने वाले मोल-भाव को बड़ी सहजता से एक किनारे कर दिया गया था। जितनी ज्यादा बार मोल-भाव, उतनी ज्यादा बार दोनों पक्षों की अपेक्षाएँ, उतनी ही ज्यादा बार मन-मुटाव और एक-दूसरे से दुराव होने की सम्भावना। ‘न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी’ के सिद्धान्त पर इसकी सम्भावना को एकदम न्यूनतम कर दिया गया था, जहाँ साल में एक बार पूरे वर्ष भर की जरुरत के हिसाब से लेन-देन निश्चित कर लिया जाता था।
इसके अतिरिक्त, संस्कारों, व्रतों आदि में इस्तेमाल होने वाली ‘बिना-जरूरत’ की वस्तुओं का तो वैसे भी कोई ‘दाम’ या ‘कीमत’ नहीं होती थी। संस्कारों, व्रतों, में लगने वाली इन चीजों के बदले में कारीगरों का ‘मान’ करना होता था। इन अवसरों पर लगने वाली चीजों की कोई निश्चित ‘कीमत’ या ‘दाम’ नहीं हुआ करती थी। महालक्ष्मी की पूजा/व्रत में लगने वाले मिट्टी के हाथी के लिए कुम्हारों को किसी घर से केवल कुछ प्रसाद और पूजा में चढ़ाई गई कुछ चीजों का एक हिस्सा, तो किसी घर से इनके अतिरिक्त कुछ रूपये, तो किसी अन्य घर से इन सबके अतिरिक्त 15-20 किलो अनाज तक भी मिल जाता है। पूजा में लगने वाले ’हाथी’ की कोई कीमत नहीं होने के कारण, सभी घर अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने कुम्हार का ‘मान’ करते हैं। इस पद्धति में मान करने वाला अपनी हैसियत के अनुरूप और सामने वाले की जरूरत के अनुसार ही मान किया करता था, जो कि और कुछ नहीं बल्कि ‘आपसी सहयोग’ का ही एक तरीका था।
बिना व्यापार वाली व्यवस्था:
जरूरत और बिना-जरूरत, सारे ही तरह के लेन-देन ‘सहयोग’ की भावना से ही प्रेरित हुआ करते थे, न कि ‘खरीदने-बेचने’ या ‘व्यापार’ की भावना से। यही कारण है कि हमारे कारीगर ‘बेचने’ के लिए नहीं, बल्कि ‘देने’ के लिए चीजें बनाते थे। और न केवल बनाते थे, बल्कि आम बोलचाल में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते थे। ग्रामीण अंचलों में आम बोलचाल में तो खैर आज भी कारीगर ‘देने’ शब्द का ही प्रयोग करते हैं, कि फलां चीज, फलाने के घर ‘देना’ है; फलाने का ‘ऑर्डर है’, या फलाने को ‘बेचना है’ नहीं। शब्दों के इस तरह के प्रयोगों से भी हम समाज की व्यवस्थाओं और किसी कार्य को करने के पीछे की भावनाओं, पद्धतियों को समझ सकते हैं।
‘व्यय–प्रधान’ अर्थव्यवस्था:
आजकल की तरह, भारतीय समाज में अर्थव्यवस्था कभी भी ‘आय-प्रधान’ नहीं रही है। भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था हमेशा से ‘व्यय-प्रधान’ अर्थव्यवस्था ही रही है। यहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की, लोगों की आय आदि बढ़ाने की बात करने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। गाँव में ‘आय आधारित’ अर्थव्यवस्था बनाने की जरूरत इसीलिए नहीं पड़ती है, क्योंकि गाँव में सभी के ‘आहार की सुरक्षा’ सुनिश्चित होने के कारण किसी को भी आय की चिंता ही नहीं होती है। वहीं यदि गाँव की अर्थव्यवस्था ‘व्यय आधारित’ नहीं होगी, तो शायद सभी लोगों के ‘आहार की सुरक्षा’ ही सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, क्योंकि यदि लोग खर्च नहीं करेंगे, व्यय नहीं करेंगे, अन्य कारीगरों का सामान नहीं खरीदेंगे, तो लोगों के ‘आहार की सुरक्षा’ ही सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। और शायद यही (हमारी अर्थव्यवस्था का क्रमश: ‘आय प्रधान’ होते जाना) एक कारण है कि वर्तमान समय में इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी हमारा समाज ‘खाद्य सुरक्षा’ जैसे सरल से लक्ष्य को भी अभी तक प्राप्त नहीं कर सका है।
इसके विपरीत, ‘व्यय प्रधान’ अर्थव्यवस्था में सारा जोर इसी बात पर रहा है, कि लोग कब-कब, कैसे-कैसे और कितना-कितना खर्च करेंगे। सारा जोर इसी बात पर रहा है, कि लोग क्या-क्या, कब-कब, और कैसे-कैसे खर्च करें। इसीलिए व्रतों, त्यौहारों, पूजाओं, संस्कारों आदि को मनाने के बहुत ही विस्तृत वर्णन, विस्तृत विधान हमारी बहुत सी किताबों, ग्रंथों आदि में मिलते हैं। इस चीज को बहुत ही गहराई से सोचा और समझा गया, कि खर्च करने की पद्धतियों पर ही सारा ध्यान केन्द्रित न करके केवल लोगों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा तो लोग अपनी आय बढ़ाकर फिजूल खर्च ही करेंगे, जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है। उसके विपरीत यदि लोगों के खर्च करने के तरीकों को ही पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया जाएगा, तो लोग उसके लिए जरूरी आय आदि साधनों को स्वतः ही व्यवस्थित कर लेंगे।
इस पूरे व्यवस्था-तंत्र का दूसरा पहलू यह है कि लोगों के खर्च करने के तरीकों, एक-दूसरे को देने के तरीकों को ही पूरी तरह व्यवस्थित कर देने पर, (सभी आठ तरह के धनों सहित) धन का समाज में विधिवत संचलन/circulation स्वतः ही सुनिश्चित हो जाता है। खर्च करने के इतने सारे और विधिवत रास्ते होने के कारण, स्वतः ही धन एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचता रहता है। लोगों की आय आदि बढ़ाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचने के क्रम में यह स्वतः ही लोगों के पास पहुंचता रहता है।
अतः इस तरह की अर्थव्यवस्था में एक साथ दोनों ही लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। एक तो लोगों के खर्च करने के तौर-तरीकों में पूरा नियंत्रण होता है, जिससे समाज में वांछित मानस, वांछित गुणों का विकास सुनिश्चित होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, जैसे लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त होते हैं। दूसरा, समाज में पर्याप्त रूप से धन के संचलन/circulation से लोगों की संपन्नता बढ़े ना बढ़े, समाज में समृद्धि का समुचित विकास होता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था में एक समृद्ध समाज का निर्माण एकदम सहज हो जाता है और यह समृद्वि केवल आर्थिक समृद्वि न होकर के मानस में भी समृद्वि लाती है। इस व्यवस्था में देने वाले और लेने वाले दोनों का ही मानस समृद्ध होता है।
(क्रमश:)
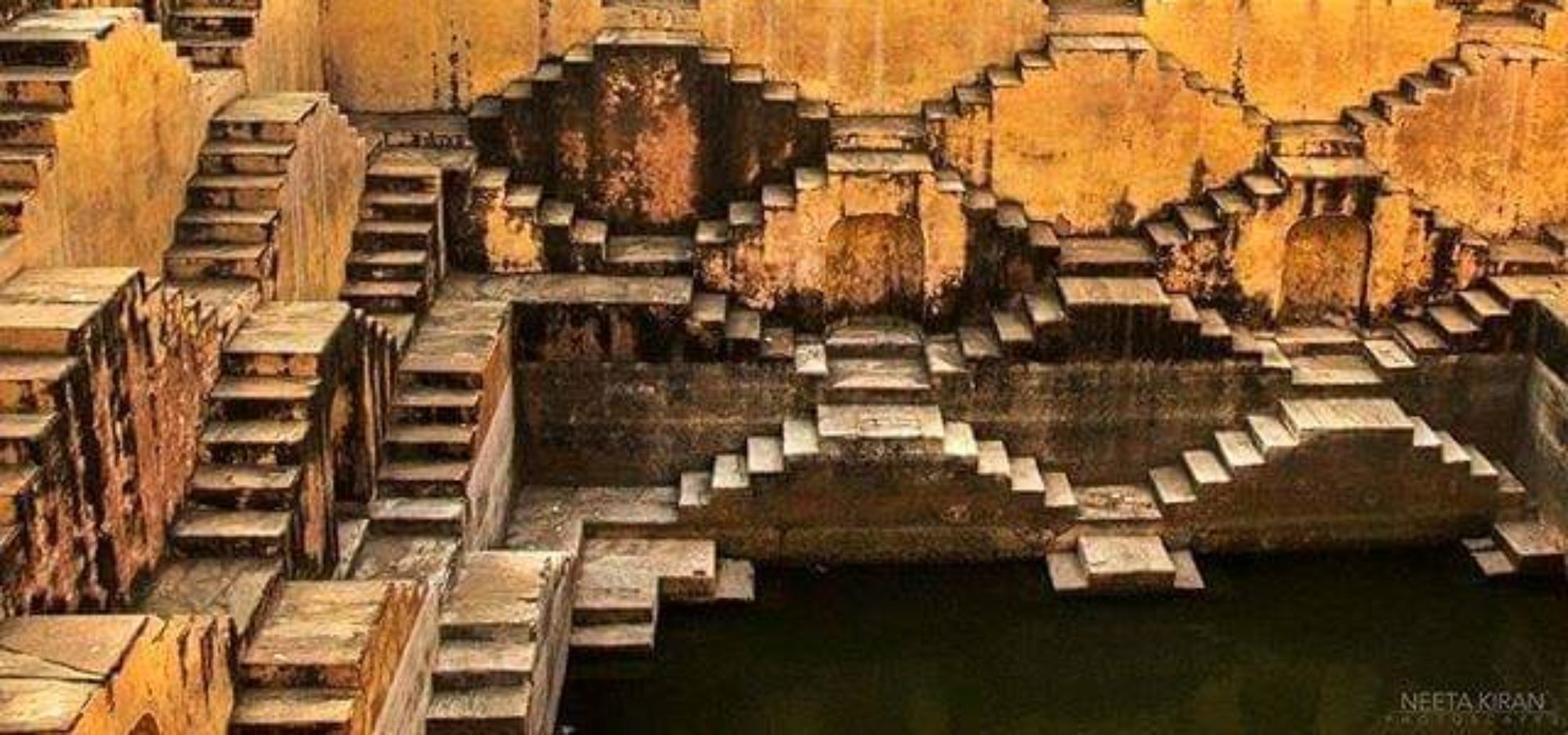

Leave a Reply